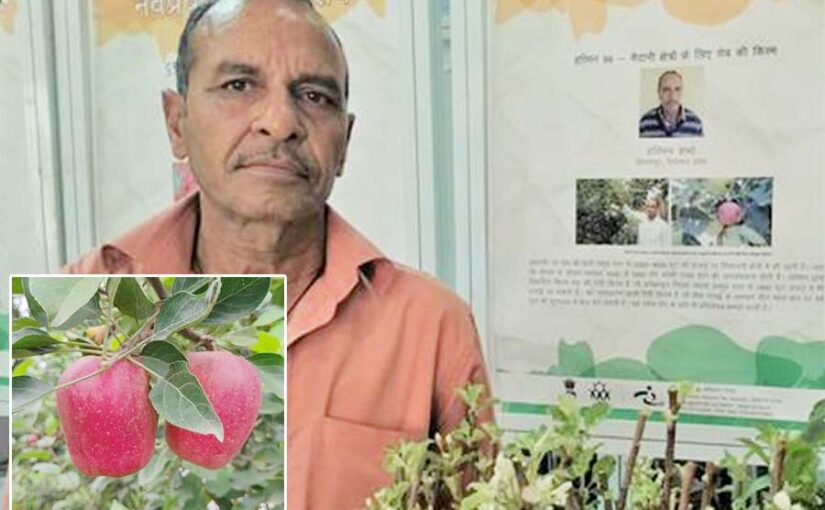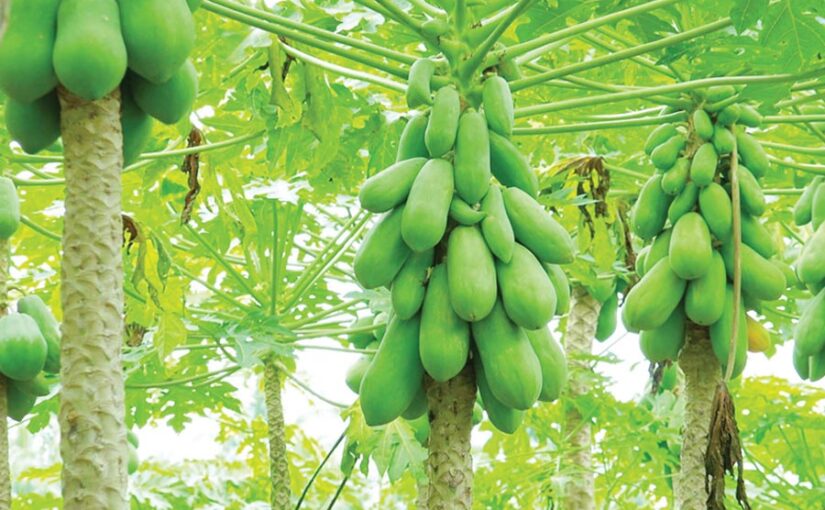आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और दिल को सुकून मिलता है. हमारे दिमाग में एक ऐसे फल की तसवीर उभरती है जिसे सोच कर ही खुशी से झूमने लगता है. आम ऐसी फसल है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है.
भारत में आम फलों का राजा है. इस की पैदावार तकरीबन पूरे भारत में होती है, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश आम के लिए जाना जाता है. यहां पर मलीहाबाद के आमों की मिठास विदेशों में भी लोगों को अपना मुरीद बना चुकी है.
पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, जांबिया, माले, ब्राजील, पेरू, केन्या, जमायका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका वगैरह देशों में भी आम उगाया जाता है.
भारत में आम के बाग सब से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन इस की सब से ज्यादा पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है. आम की बागबानी के लिए गरम आबोहवा बेहतर है.
आम के लिए 24 से 26 डिगरी सैल्सियस तापमान वाला इलाका सब से अच्छा माना गया है. यह नम व सूखी दोनों तरह की जलवायु में उगता है. लेकिन जिन इलाकों में जून से सितंबर माह तक अच्छी बारिश होती है और बाकी महीने सूखे रहते हैं, वहां आम की पैदावार ज्यादा होती है.
आम के पेड़ों को रोगों से बचाना बहुत जरूरी है. समयसमय पर आम में लगने वाली खास बीमारियों पर नजर रख कर ही रोगों से बचाया जा सकता है.
काली फफूंद रोग
आम के पुराने और घने गहरे बगीचों में आम के फूलों और मुलायम पत्तियों से रस चूसने वाले कीट जैसे भुनगा, फुदका, मधुआ और कढ़ी कीट का प्रकोप चैत्र माह से ही शुरू हो जाता है. ये कीट छोटीछोटी नई मुलायम पत्तियों और फूलों से रस चूसते रहते हैं. इस वजह से आम की पत्तियों और फूलों के ऊपर एक चिपचिपाहट सी बनने लगती है और फल झड़ने लगते हैं.
यह रोग भुनगा कीट की वजह से होता है. फफूंद के जरीए भी यह रोग तेजी से फैलती है. कुछ समय बाद आम के बगीचों में पेड़ों की पत्तियों पर काले रंग की एक परत बन जाती है, जो सीधा पत्तियों से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है.
उपचार
काली फफूंदी के नियंत्रण के लिए नीम की पत्तियों को उबालें. इस के बाद 10-12 लिटर उबले हुए पानी को 100 लिटर पानी में मिला कर पेड़ों पर 2-3 बार अच्छी तरह से स्प्रेयर पंप की मदद से छिड़काव करना चाहिए.
आम का भुनगा, फुदका और कढ़ी कीट पर 300 से 400 मिलीलिटर नीम के तेल को 100 लिटर पानी में घोल कर फूल खिलने से पहले या फिर मटर के दाने के बराबर फल बनने के बाद 2-3 छिड़काव करने से इन कीटों पर काबू पाया जा सकता है.
इस के अलावा ब्यूबेरिया बेसियाना की 200 ग्राम मात्रा को 100 लिटर पानी में घोल कर 2-3 बार छिड़काव करने या 15-20 दिन पुरानी सड़ी हुई छाछ या मट्ठा 10 लिटर व 8 से 10 दिन पुराने 10 लिटर गौमूत्र को 100 लिटर पानी में मिला कर पूरे पौधे पर 2-3 छिड़काव करने से कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है.
चूर्णिल आसिता रोग
आम का यह रोग फफूंद की वजह से फैलता है. इस रोग का हमला होने आम की पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बे बन जाते हैं. कभीकभी फूलों की टहनियों और छोटेछोटे फलों पर भी ये धब्बे हवा के रुख के साथ फैल जाते हैं. इस वजह से फल पकने से पहले ही पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं.
इस रोग की रोकथाम के लिए 100 लिटर पानी में मिलाएं 10 दिन पुरानी सड़ी हुई छाछ या मट्ठा 10 लिटर या 10 लिटर गौमूत्र 10-12 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने से रोग इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है.
सूखा रोग
आम के पेड़ों में लगने वाला सूखा रोग यानी तनाछेदक कीट हरियाली का दुश्मन है. इस रोग के प्रकोप से आम का हराभरा पेड़ कुछ ही महीनों में सूख कर ढांचे में तबदील हो जाता है.
तनाछेदक कीट पौधे के तने में छेद कर आसानी से अंदर घुस जाता है. पेड़ के तने को सावधानी से देखने पर किसानों को कीड़ों के होने की प्रारंभिक दशा में छाल पर चूर्ण जैसा पदार्थ देखने को मिलता है. तना गीला हो जाता है. कीट के बड़े हो जाने पर तने में सुराख साफसाफ दिखाई देने लगता है.
उपचार न होने की दशा में कीट तने को खोखला कर देते हैं. इस से पेड़ सूखने लगता है. इस में पत्तियां ऊपर से सूखना शुरू होती हैं, जो नीचे की ओर बढ़ती जाती हैं.
ऐसे करें रोकथाम
तनाबेधक या तनाछेदक कीट साल में सिर्फ 2 महीने मई व जून माह में बाहर रहता है. नियंत्रण के लिए क्विनालफास व साइपरमैथलीन दवा का स्प्रे करें.
रोकथाम के लिए बाद में तने को छील कर सुराख में साइकिल की तीली डाल कर बड़े कीटों को मारा जा सकता है.
अंडे बच्चों को नष्ट करने के लिए मोनोक्रोटोफास के घोल को रुई में भिगो कर सुराख में डाल दें व ऊपर से गाय के गोबर में मिट्टी मिला कर लेप लगा दें.
देशी उपचार में 2 किलोग्राम तंबाकू व ढाई सौ ग्राम फ्यूरोडान प्रति पेड़ की जड़ में डालने से भी रोकथाम हो सकती है.
बौर का रोग
आम के बौरों, फलों या पत्तियों पर सफेद चूर्ण की तरह का पदार्थ दिखाई देता है. ऐसा लगता है कि पेड़ों पर राख छिड़क दी गई है. प्रकोप होने से उन की बढ़वार रुक जाती है और फूल गिरने लगते हैं.
बौर के समय फुहार और ठंडी रातें इस रोग के बढ़ने में मददगार होती हैं. कवक से नए फल बिलकुल ढक जाते हैं और धीरेधीरे उस की बाहरी सतह पर दरारें पड़ने लगती हैं. दरार वाला वह भाग कड़ा हो जाता है. नए फल मटर के दाने के बराबर होने के पहले ही गिर जाते हैं.
नई पत्तियों की पिछली सतह पर यह रोग काफी फैलता है और स्लेटी रंग के धब्बे बनने लगते हैं, जिस पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है और रोगग्रस्त पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं. ऐसी पत्तियां पूरे साल पौधों पर लगी रहती हैं और अगले साल भी रोगों को फैलाने में सहायक होती हैं.
उपचार से करें बचाव
इस रोग से बचाव के लिए फूल के मौसम में कुल 3 छिड़काव करने चाहिए. पहला छिड़काव 0.2 फीसदी विलयशील गंधक (वेटेबल सल्फर) (सल्फेट या दूसरा विलयशील गंधक फफूंदनाशक 2 ग्राम प्रति लिटर), दूसरा छिड़काव 0.1 फीसदी ट्राइडीमार्फ या 0.04 फीसदी फ्लूजिजाल (1 मिलीलिटर कैलिक्सीन या 0.4 मिलीलिटर पंच प्रति लिटर) और तीसरा छिड़काव 0.1 फीसदी डाइनोकैप या बावस्टीन (1 मिलीलिटर 5 प्रति केराथेन या 1 ग्राम ट्राइडीमेफान प्रति लिटर) से करना चाहिए.
पहला छिड़काव बौर निकलने के दौरान करना चाहिए. दूसरा और तीसरा छिड़काव 10-15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए.

पत्तियों पर एंथ्रेक्नोज रोग
तुड़ाई के बाद आम का यह सब से खास रोग है. यह एक फफूंद कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोराइडिस से होती है. इस का प्रकोप हर आम उगाने वाली जगहों पर होता है. फलों पर इन के लक्षण शुरू में छोटेछोटे भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जो बाद में बढ़ कर पूरे फल को ढक लेते हैं. ये धब्बे 3-4 दिन में ही पूरे फल को ढक लेते हैं और पूरा फल काला हो कर सड़ जाता है.
रोकथाम
कार्बंडाजिम या टापसिन-एम (0.1 फीसदी यानी 1 ग्राम प्रति लिटर) का 3 छिड़काव तुड़ाई से पहले करें फिर 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए. छिड़काव इस तरह करना चाहिए कि अंतिम छिड़काव तुड़ाई से 15 दिन पहले हो जाए.
फलों को 0.05 फीसदी कार्बंडाजिम (0.5 ग्राम प्रति लिटर) के कुनकुने पानी में 15 मिनट तक डुबो कर रखने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है.
शाखा रोग
इस रोग से शाखाएं और टहनियां सूखने लगती हैं. उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि शाखा आग से झुलस गई है. रोग की शुरुआत में शाखाओं के अगले भाग की छाल काली पड़ जाती है, जो धीरेधीरे बढ़ती है और फिर पूरी शाखा ही सूख जाती है. साथ ही, गोंद का रिसाव भी होने लगता है.
रोकथाम
रोगग्रस्त शाखाओं की कटाई रोग से ग्रसित हिस्से के करीब 7.5-10 सैंटीमीटर नीचे से करनी चाहिए. इस के बाद 3 ग्राम फफूंदनाशक दवा प्रति लिटर पानी में मिला कर छिड़काव करना चाहिए और कटे हुए भाग पर इसी फफूंदनाशक दवा का लेप लगाना चाहिए. छोटे पेड़ों में भी रोगग्रस्त शाखाओं की छंटाई के बाद कौपर औक्सीक्लोराइड का लेप लगाना फायदेमंद है.
रेड रस्ट रोग
पत्तियों पर गोलाकार, मटमैले रंग के मखमली धब्बे दिखाई देते हैं, जिन का आकार बाद में बड़ा और रंग बादामी हो जाता है.
धब्बे की सतह भी उभरी हुई होती है. इस के ऊपर काई के बीजाणु बनते हैं जो बाद में तांबे के रंग के हो जाते हैं. आखिर में बीजाणुओं के झड़ने की वजह से पत्तियों पर गोलाकार सफेद निशान रह जाते हैं.
इस रोग के कारण पत्तियां और टहनियां छोटी रह जाती हैं और बाद में सूखने लगती हैं.
दिसंबरजनवरी माह में रोग से ग्रसित पत्तियां अधिक झड़ती हैं और पौधे दूर से ही मुरझाए हुए से दिखाई देते हैं.
रोकथाम
इस रोग की रोकथाम के लिए 0.3 फीसदी कौपर औक्सीक्लोराइड (3 ग्राम प्रति लिटर का 2-3 ग्राम प्रति लिटर) का छिड़काव करना असरदार पाया गया है.
ये सारे रोग आम के फलों में तुड़ाई से पहले लगते हैं, लेकिन इन सारे रोगों से निबटने के बाद भी आम के उत्पादकों को तुड़ाई के बाद भी कई तरह के रोगों से अपने फलों को बचाने की चुनौती रहती है. अगर जरा सी लापरवाही की गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है.

तुड़ाई के बाद रोग
फलों में तुड़ाई के बाद भी उत्पादन का तकरीबन 25-40 फीसदी कई वजहों से खराब हो जाता है. यह नुकसान गलत समय पर फलों की तुड़ाई, गलत तुड़ाई के तरीके और गलत ढंग से भंडारण करने की वजह से होता है. लेकिन जो नुकसान होता है, वह मुख्य रूप से फलों की तुड़ाई के बाद लगने वाले रोग हैं.
आम की तुड़ाई के बाद होने वाले रोगों में मुख्य फफूंद है. तुड़ाई के बाद फलों में संक्रमण, आम की ढुलाई, भंडारण और लाने और ले जाने के दौरान होता है.
आम में बीमारियों का प्रकोप 2 तरह से होता है. एक तो फलों के लगते समय ही उन को संक्रमित कर देते हैं, दूसरे तुड़ाई के बाद फलों के रखरखाव के दौरान होता है.
आम की तुड़ाई के बाद भी बहुत सी बीमारियां लगती हैं, लेकिन इन में एंथ्रेक्नोज, ढेपी विगलन और काला सड़न बीमारी से अधिक नुकसान का डर रहता है.
गहरे भूरे रंग का डंठल
तुड़ाई के बाद आम की यह खास बीमारी है. यह लेसियोडिपलोडिया थियोब्रोमी नामक फफूंद से होती है. इस में तकरीबन 15-20 फीसदी तक का नुकसान होता है. यह बीमारी आम की चौसा किस्म में अधिक पाई जाती है. फलों में यह बीमारी ढेपी की तरह से शुरू होती है तभी इसे ढेपी विगलन रोग कहते हैं.
शुरू में जहां पर डंठल लगा होता है, वह भाग गहरे भूरे रंग का हो जाता है और धीरेधीरे बढ़ कर यह पूरे फल को ढक लेता है. 3-4 दिन बाद पूरा फल सड़ कर काले रंग का हो जाता है.
रोकथाम
फल को 1 से 2 सैंटीमीटर के डंठल सहित तोड़ना चाहिए. इस के बाद फल को मिट्टी के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए.
तुड़ाई से पहले 2 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर कार्बंडाजिम या टापसिन एम (0.1 फीसदी यानी 1 ग्राम प्रति लिटर) का करना चाहिए. फलों को 0.05 फीसदी कार्बंडाजिम (0.5 ग्राम प्रति लिटर) के कुनकुने पानी में 5 मिनट डुबो कर रखने से इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है.
काला सड़न रोग
यह रोग एस्परजीलस नाइजर नामक फफूंद से होता है. यह रोग फलों में चोट या कटे स्थान से शुरू होता है.
शुरू में इस के लक्षण पीले रंग के गोल धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं. 3-4 दिन में धब्बे आकार में बढ़ जाते हैं और इन के ऊपर काले रंग के फफूंद के जीवाणु दिखाई देने लगते हैं.
रोकथाम
फलों को सावधानी से तोड़ना चाहिए, ताकि फलों पर खरोंच न लगे या फल न कटे.
फलों को 0.5 फीसदी कार्बंडाजिम (0.5 ग्राम प्रति लिटर) के कुनकुने पानी में 5 मिनट तक डुबो कर रखने से इस रोग पर काबू किया जा सकता है.
अगर आप को आम की अच्छी उपज लेनी है तो शुरू से ही पौधों की देखभाल करें. आम के पौधों को जितना फल लगने के बाद देखभाल की जरूरत होती है, उस से कहीं ज्यादा फल आने के पहले होती है.
आमतौर पर किसान यहीं गलती करते हैं. इस वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है. बौर आने के पहले रोगों से आम को बचाएं, साथ ही, बौर आने के बाद भी कई तरह के छिड़काव से रोगों से बचाना अहम हो जाता है. जब फल बड़े हो कर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएं तब भी उन्हें सड़नेगलने से बचाना उतना ही जरूरी है, जितना शुरुआत में बचाया गया था.