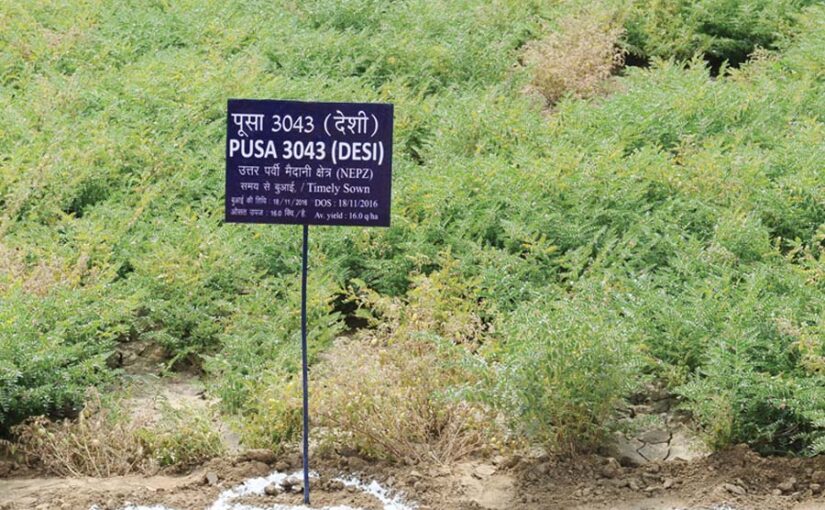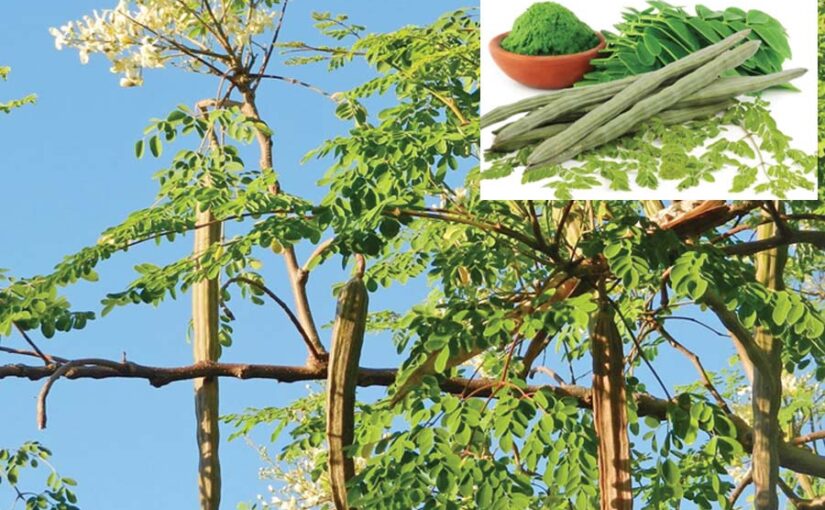सामाजिक संस्थाएं, गैरसरकारी संस्थान, उन्नत कृषि तकनीक, बजाज फाउंडेशन,विश्व युवक केंद्र,कृषि उत्पादक संगठन, ट्रेनिंग,आजीविका, खेती,दिल्ली प्रेस, फार्म एन फूड,
देशभर में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक सरकारी, गैरसरकारी संस्थान किसानों को अनेक उन्नत कृषि तकनीकों से रूबरू कराते हैं, समयसमय पर अनेक ट्रेनिंग देते हैं, जिस से कृषि क्षेत्र उन्नति कर सके और इस से जुड़े किसानों की आय में भी इजाफा हो.
ऐसी ही कड़ी में राजस्थान के सीकर में विश्व युवक केंद्र और बजाज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से 11 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित ध्येय कार्यक्रम के तहत देश की सामाजिक संस्थाओं और कृषि उत्पादक संगठनों के करीब 100 प्रतिनिधियों को कृषि, जल, शिक्षा और आजीविका पर विषय पर प्रशिक्षित किया गया.
इस अवसर पर बजाज समूह के संस्थापक जमनालाल बजाज की जन्मस्थली सीकर और उस के आसपास के क्षेत्रों में जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट द्वारा 1963 से अब तक किए गए सतत प्रयासों से कृषि, जल, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया.
आयोजकों ने साझा किया ट्रेनिंग का उद्देश्य

ट्रेनिंग के पहले दिन बजाज फाउंडेशन में सीएसआर के प्रेसिडेंट हरिभाई मोरी ने जल संसाधनों के विकास पर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने सभी संस्थाओं से आह्वान किया कि अगर सभी सामाजिक संगठन एकजुट हो कर कृषि और जल पर काम करें, तो देश को विकास की नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है.
उन्होंने बताया कि बजाज फाउंडेशन द्वारा सीकर में कृषि, जल पुनर्भरण, शिक्षा और आजीविका पर सघन और सफल रूप से काम किया जा रहा है, जिस के सफल अनुभवों से रूबरू कराने के लिए देश अभी तक 500 के करीब ऐसे सामाजिक सगठनों और किसान उत्पादक संस्थाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो खेती के जरीए आजीविका को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं.

विश्व युवक केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. इस दौरान बजाज फाउंडेशन और विश्व युवक केंद्र के कार्यों पर एक डौक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की गई.
उन्होंने बताया कि सीकर में गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा गांव में सपने को साकार करने के लिए सामाजिक संस्थाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं. ऐसे में सीकर में अपनाए जा रहे इस मौडल को समझाना भी एक उद्देश्य रहा है.
उन्होंने यह भी बताया कि सीकर में लोगों ने बारिश के पानी को अपने घर की छत के जरीए संचयन करने का काम किया है. वर्षा जल संचयन की इस संरचना के लाभों को समझने के लिए यह ट्रेनिंग इन प्रतिभागियों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है.

विश्व युवक केंद्र में कार्यक्रम अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि देश में आने वाले समय में जल संकट एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ सकता है. ऐसे में जल की कमी वाले सीकर में ट्रेनिंग आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग यहां के जल संचयन, खेती और सिंचाई में जल प्रबंधन सहित आजीविका के उपायों को सीखें और अपने क्षेत्रों में लागू करें.

विश्व युवक केंद्र में ही कार्यक्रम अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि कृषि, जल पुनर्भरण, शिक्षा और आजीविका जैसे विषय पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किए जाने की जरूरत है. ऐसे में सफल अनुभवों को एकदूसरे से साझा किए जाने के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम साबित हो सकता है. उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आह्वान किया कि सभी लोग समयसमय पर सोशल मीडिया के जरीए सफलता की कहानियों को साझा करते रहें, जिस से बदलाव की कहानियों से सीख ले कर दूसरे क्षेत्रों में भी लोग इसे अपना पाएं.
पद्मश्री जगदीश पारीक ने कृषि के नवाचारों को किया साझा
पद्मश्री और गोभीमैन औफ इंडिया के नाम से विख्यात जगदीश पारीक ने कम पानी में खेती और बागबानी का अनुभव साझा किया और अपने नवाचारों पर जानकारी दी. कार्यक्रम में एफपीओ और कृषि उद्यमिता, प्राकृतिक खेती और मूल्य संवर्धन मौडल, आत्मनिर्भर परिवार, लघु पैमाने पर कृषि उद्यमिता, वर्षा जल पुनर्भरण संरचना पर प्रकाश डाला गया.
सीकर जिले के अजीतगढ़ निवासी किसान जगदीश प्रसाद पारीक ने बताया कि वे खेती में नएनए प्रयोग करते हैं. वे सब्जियों की नई किस्म तैयार करने से ले कर किसानों को और्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करते हैं.
खेती के नाम कई रिकौर्ड
पद्मश्री जगदीश पारीक ने बताया कि वह अपने खेत में 25 किलो ढाई सौ ग्राम वजनी गोभी का फूल, 86 किलो कद्दू, 6 फीट लंबी घीया, 7 फीट लंबी तोरिया, 1 मीटर लंबा और 2 इंच का बैगन, 5 किलो गोल बैगन, ढाई सौ ग्राम मोटा प्याज, साढ़े 3 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्ची तक उगा चुके हैं.
उन्होंने बताया कि सब से अधिक किस्में फूलगोभी की हैं. यही वजह है कि लोग इन्हें ‘गोभी मैन’ कह कर भी बुलाते हैं.

54 साल से कर रहे जैविक खेती
जगदीश पारीक ने बताया कि वह साल 1970 से और्गेनिक खेती कर रहे हैं. पिता के निधन के बाद पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया. उन्होंने गोभी से इस की शुरुआत की और इस की किस्मों को ले कर कई नए प्रयोग किए. उन्हें प्रदेश में जैविक और शून्य लागत की खेती के प्रणेता के रूप में पहचान मिली है. इसी वजह से साल 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था.
रेतीले इलाके में सफल खेती
जगदीश पारीक का खेत ड्राई जोन का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि बरसात के पानी से आने वाले बहाव को वह अपने खेत में डायवर्ट करते हैं, जिस से उन का कुआं रिचार्ज हो जाता है और सालभर वह उसी पानी का इस्तेमाल खेती के लिए करते हैं. एक बरसात के सीजन में वह 3 बार पानी की राह रोक कर अपने खेत में मोड़ देते हैं. जिसे जमीन सोख लेती है और उसी पानी से उन के खेत पर बना कुआं जीवंत हो जाता है.
खेती के अनुभवों को करते हैं साझा
जगदीश पारीक की खेती में प्रयोगधर्मिता से न सिर्फ किसान, बल्कि कृषि अधिकारी तक प्रभावित हैं. यही वजह है कि कृषि से जुड़े सैमिनार हों या वर्कशाप देशभर से जगदीश पारीक को बुलाया जाता है और उन के अनुभवों से सीखा जाता है.
फील्ड विजिट कर प्रतिभागी कृषि, जल और आजीविका के अनुभव से हुए रूबरू
विश्व युवक केंद्र और बजाज फाउंडेशन द्वारा सीकर में आयोजित पांचदिवसीय प्रशिक्षण और फील्ड विजिट कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रतिभागियों ने लक्ष्मणगढ़ ब्लौक खिनवासर गांव के प्रगतिशील किसान अमरचंद काजला के प्राकृतिक खेती, मीठे नीबू के भूखंड और बायोगैस प्लांट का दौरा किया.
इस दौरान अमरचंद काजला ने अपने प्राकृतिक खेती के मौडल पर प्रतिभागियों को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वह जिस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, वहां का क्लाइमेट खेती के लिए बहुत जटिल है, फिर भी उन्होंने प्राकृतिक खेती के जरीए खेती में सफलता के नए आयाम गढ़ते हुए सफलता प्राप्त की है.
उन्होंने बताया कि उन के कृषि उत्पादों को बेचने के लिए वह एप का सहारा लेते हैं, जिस से उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है. उन्होंने अपने गोबर गैस प्लांट की कार्यप्रणाली को दिखाते हुए उस के फायदे भी गिनाए.
बजाज फाउंडेशन में सीएसआर के प्रेसिडेंट हरिभाई मोरी ने अमरचंद काजला के गौ आधारित खेती के मौडल की प्रशंसा करते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू करने पर जोर दिया. वीवाईके के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर सिंह ने सीकर में अपनाए जा रहे जल उपयोग प्रणाली, जैविक, प्राकृतिक और गौ आधारित खेती को आज की आवश्यकता बताते हुए मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया.
उन्होंने सीकर के आजीविका मौडल और भूमि जल पुनर्भरण मौडल की सराहना की और उसे अन्य राज्यों में भी लागू किए जाने की वकालत की.
इस के बाद दौरे पर आई टीम ने इस बलारा गांव में कृषि प्रसंस्करण इकाई तेल मिल और मसाला मिल का दौरा कर मूल्य संवर्धन और आजीविका से जुड़ी सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त की.
ध्येय प्रोग्राम के तहत दौरे पर आई यह टीम सिंहोदरा गांव के पवन कुमार शर्मा के फार्म पर प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण के तहत 3 लेयर खेती, बाजरा प्रसंस्करण इकाई, खेत टांका और वृक्षारोपण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की.
टीम ने ड्रिप के जरीए किन्नू और मीठे नीबू के बाग का अध्ययन करने के लिए रामचंद्र सेन के फार्म का दौरा किया. छत पर वर्षा जल संचयन संरचना के लाभों को समझने के लिए ओमप्रकाश मेहेरिया के फार्म का भी दौरा किया. इस दौरान टीम ने भूमि समतलीकरण गतिविधि के लाभों को समझने के लिए राजेश स्वामी से जानकारियां प्राप्त की.
राजस्थान के सूखे खेतों में फूलों की लहलहाती खेती ने किया हैरान
राजस्थान की जमीन रेतीली होने और कम बारिश के चलते देश के अन्य हिस्सों की तुलना में खेती किया जाना कठिन काम है, लेकिन सीकर जिले के तमाम किसानों ने बजाज फाउंडेशन के सहयोग के बारिश के पानी को संरक्षित करते हुए ड्रिप इरिगेशन के जरीए तमाम ऐसी फसलों को उगाने में सफलता पाई है, जिसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है. सीकर की इसी खेती की विधि को सीखने के लिए टीम जब तसरबाड़ी गांव पहुची, तो यहां के किसान भंवर लाल के एकीकृत खेती के मौडल करीब 40 एकड़ क्षेत्र में गेदे और गुलदाऊदी फूल की सफल खेती को देख कर अचंभित हो गई.

इस मौके पर किसान भंवर लाल ने बताया कि वह करीब 40 एकड़ क्षेत्र में पानी का बेहतर प्रबंधन करते हुए फूलों की खेती कर करीब 70 लाख रुपए की आमदनी हर साल कर लेते हैं. उन्होंने बताया कि वह बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं, जिसे ड्रिप के जरीए फसल की सिंचाई करते हैं. उन्होने अपने फार्म, तालाब, पौलीहाउस, बगीचे का भ्रमण भी कराया और खेती के सफल मौडल की जानकारी दी.
प्रतिभागियों ने सराहा
विश्व युवक केंद्र और बजाज फाउंडेशन द्वारा कृषि, जल पुनर्भरण, शिक्षा और आजीविका विषय पर आयोजित ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम में देश के करीब 12 राज्यों से 100 से भी अधिक प्रतिभागी शामिल हुए. प्रतिभागियों ने राजस्थान के सीकर में कम पानी में किए जा रहे सफल खेती और आजीविका के मौडल को सराहा और अपनेअपने क्षेत्रों में लागू किए जाने पर बल दिया.
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से नैशनल अवार्डी किसान राममूर्ति मिश्र ने कहा कि उन्हें सीकर में अपनाए जा रहे एक लिटर पानी में पौधारोपण के सफल प्रयोग ने काफी प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में हरियाली बढ़ाई जा सकती है, तो देश के सिंचित और वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे और भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है.

ट्रेनिंग में आए रूरल अवेयरनेस फौर कम्युनिटी इवोलूशन के अध्यक्ष नितेश शर्मा ने सीकर में किसानों द्वारा जल संसाधन विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को सराहा. उन्होंने कहा कि सीकर में किसानों द्वारा संचालित एफपीओ कृषि उद्यमिता की मिसाल है. इस से देश के अन्य किसानों को सीखने में मदद मिलेगी.


विश्वनाथ चौधरी ने विजिट के दौरान प्राकृतिक खेती और मूल्य संवर्धन के मौडल और उस से आत्मनिर्भर बने किसान परिवारों के अनुभवों को साझा किया. प्रतिभागी नीलम मिश्रा ने एसएचजी फेडरेशन के जरीए सीकर में हुए महिला सशक्तीकरण को सराहा.









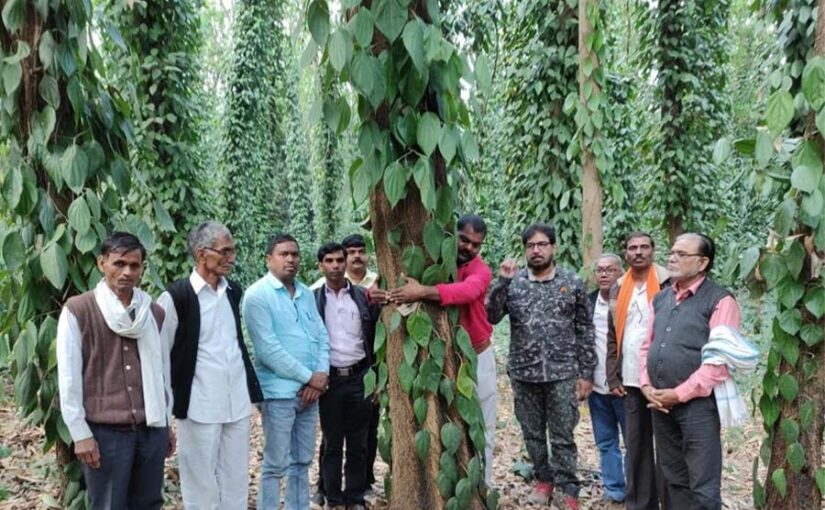

 महिला किसानों ने बढ़ाया हौसला
महिला किसानों ने बढ़ाया हौसला कार्यकारी प्रकाशक ने किया स्वागत
कार्यकारी प्रकाशक ने किया स्वागत दिल्ली प्रैस के इतिहास पर प्रकाश
दिल्ली प्रैस के इतिहास पर प्रकाश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बढ़ाया हौसला
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बढ़ाया हौसला जूरी टीम ने किया चयन
जूरी टीम ने किया चयन सहप्रायोजक के रूप में इन का भी रहा सहयोग
सहप्रायोजक के रूप में इन का भी रहा सहयोग