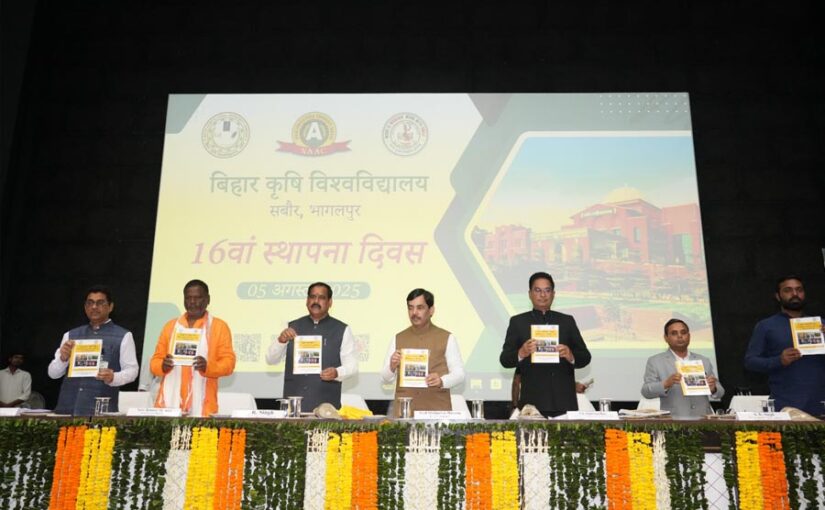Seafood : मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग ने पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित अंबेडकर भवन में समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यातक सम्मेलन 2025 का आयोजन किया.
इस बैठक में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (एमओएफएएचएंडडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) मंत्री राजीव रंजन सिंह, एमओएफएएचएंडडी और एमओपीआर राज्य मंत्री प्रोफैसर एसपी सिंह बघेल और राज्य मंत्री एमओएफएएचएंडडी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जौर्ज कुरियन भी उपस्थित थे.
इस बैठक में वाणिज्य विभाग, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, निर्यात निरीक्षण परिषद, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारियों, उद्योग भागीदारों और किसानों ने भाग लिया. इस में भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथसाथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात के मत्स्यपालन विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया.
इस बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारतीय समुद्री खाद्य (Seafood) की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए इस में मूल्य संवर्धन के महत्त्व पर जोर दिया. उन्होंने मत्स्यपालन क्षेत्र में चल रही सरकारी गतिविधियों पर का जिक्र किया, जिस में सभी भागीदारों के लिए बेहतर बाजार संपर्क हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का विकास, उच्च स्तर के सागरीय और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यपालन को मजबूत करना और बुनियादी ढांचे को उन्नत करना शामिल है. इस का उद्देश्य मत्स्यपालन क्षेत्र को और अधिक मजबूत करना है.
उन्होंने आगे उद्योग के सामने आने वाली टैरिफ चुनौतियों से निपटने में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और राज्य सरकारों के साथ समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से राज्यवार प्रजाति विशिष्ट निर्यातों के सटीक मानचित्रण और नए निर्यात अवसरों की पहचान के लिए सभी हितधारक के साथ सलाह आयोजित करने का आग्रह किया. उन्होंने वहां मौजूद सभी भागीदारों को भारतीय समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात को और मजबूत बनाने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया.
प्रोफैसर एसपी सिंह बघेल ने देश के बड़े मत्स्य संसाधनों का जिक्र किया और सभी भागीदारों से भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उन का लाभ उठाने का आग्रह किया. उन्होंने वैश्विक बाजार जोखिमों को कम करने के लिए नए बाजारों की पहचान करने व उन का उपयोग करने के महत्त्व पर जोर दिया और सभी भागीदारों से समुद्री खाद्य (Seafood) मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और उस का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिल कर काम करने का आह्वान किया.
राज्य मंत्री मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय जौर्ज कुरियन ने “वोकल फौर लोकल” दृष्टिकोण को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि घरेलू बाजारों को मजबूत करने से विशेष रूप से वैश्विक टैरिफ चुनौतियों के मद्देनजर मछुआरों एवं किसानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे.
एमओएफएएचएंडडी सचिव (मत्स्यपालन) डा. अभिलक्ष लिखी ने इस बात पर जोर दिया कि धनराशि के हिसाब से भारत के समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात का केवल 10 फीसदी ही वर्तमान में मूल्यवर्धित उत्पाद हैं, उन्होंने बढ़े हुए घरेलू उत्पादन या आयात और पुनर्निर्यात रणनीतियों के माध्यम से वैश्विक मानदंडों के अनुरूप इस हिस्से को 30-60 फीसदी तक बढ़ाने की जोर दिया.
उन्होंने एक ही प्रजाति, व्हाइटलेग श्रिम्प पर भारी निर्भरता पर चिंता जताई, जिस का निर्यात मूल्य 62 फीसदी है, लेकिन मात्रा केवल 38 फीसदी है. डा. अभिलक्ष लिखी ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की तुरंत आवश्यकता पर जोर दिया और आश्वासन दिया कि टैरिफ और गैरटैरिफ बाधाओं से संबंधित मुद्दों को वाणिज्य विभाग, विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर के हल किया जाएगा.
उन्होंने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए उन की पहचान और वित्तपोषण के लिए लक्षित इनपुट का भी आह्वान किया, जिस से समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात मूल्य श्रृंखला में मूल्यवर्धन को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा.
इस बैठक में भागीदारों ने समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात को बढ़ावा देने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताया, जिन में चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा कड़े प्रोत्साहनों की पेशकश के बावजूद अधिक मूल्य संवर्धन की आवश्यकता, अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में टैरिफ बाधाएं और यूरोपीय संघ जैसे उच्चमूल्य वाले क्षेत्रों तक पहुंचने में प्रमाणन और अनुपालन संबंधी बाधाएं शामिल हैं.
डा. अभिलक्ष लिखी ने निजी परीक्षण, थर्डपार्टी मंजूरी और कृषि प्रमाणन जैसी गैरटैरिफ बाधाओं के साथसाथ रेनबो ट्राउट जैसे विशिष्ट उत्पादों के लिए कोल्ड चेन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे में कमियों की ओर भी इशारा किया. इन सुझावों में बड़े निर्यातकों को योजना के लाभ प्रदान करना, मूल्य संवर्धन के लिए प्रोत्साहन देना, सरकार समर्थित प्रमाणन सहायता को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, वैश्विक खरीदारों के साथ बी2बी संपर्क को आसान बनाना और बैंकों व एनबीएफसी के माध्यम से वित्त तक पहुंच में सुधार करना शामिल था.
समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात के विस्तार के लिए पहचाने गए वैकल्पिक बाजारों में ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, रूस और चीन शामिल थे, जिन में दक्षिण कोरिया की क्षमता और मध्य पूर्व की बढ़ती मांग पर विशेष जोर दिया गया.
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात के भविष्य से संबंधित विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर मीडिया प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की. उन्होंने हाल के अमरीकी टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात की और निर्यातकों के हितों की रक्षा और वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उपायों का भी जिक्र किया.
उन्होंने बीते सालों में मत्स्यपालन क्षेत्र की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और उत्पादन में हुई खास बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे के विकास और बाजार विविधीकरण के बारे में बताया. इस के अलावा, उन्होंने भारत में समुद्री खाद्य (Seafood) मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रमुख योजनाओं और गतिविधियों पर भी जानकारी साझा की.