बांस एक बहुपयोगी घास है, जो हमारे जीवन में अहम जगह रखता है. इस को ‘गरीब आदमी का काष्ठ’, ‘लोगों का साथी’ और ‘हरा सोना’ आदि नामों से जाना जाता है. बांस के कोमल प्ररोह सब्जी व अचार बनाने और इस के लंबे तंतु रेऔन पल्प बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, जिस से कपड़ा बनता है.
आवास (झोंपड़ी) व हलके फर्नीचर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बांस प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार यह आदमी की 3 प्रमुख जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करता है.
भारत बांस संसाधन से संपन्न है, क्योंकि यह देश के अधिकतर क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. देश में इस समय बांस की लगभग 125 देशी व विदेशी प्रजातियां उपलब्ध हैं. पूरे देश के 89.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बांस वाला वन क्षेत्र है, जो पूरे वन क्षेत्रफल का तकरीबन 12.8 फीसदी है.
आमतौर पर गांव में लोग अपने घर के आसपास ही काफी अधिक मात्रा में बांस उगाते हैं, ताकि उस से वे अपने रोजाना की जरूरतें पूरी कर सकें.
जलवायु और मिट्टी
बहुत ठंडे क्षेत्रों को छोड़ कर लगभग हर प्रकार के क्षेत्रों में बांस का रोपण किया जा सकता है. इस के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है. बांस जलोढ़, पथरीली व लाल मिट्टी में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है.
प्रमुख प्रजातियां
वर्तमान में देश में बांस के 23 वंश (जेनरा) और 125 जातियां (स्पीसीज) पाई जाती हैं. क्षेत्र व जलवायु के हिसाब से बांस की अलगअलग प्रजातियां उपयुक्त होती हैं. उत्तरपूर्वी भारत (पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि) में रोपण के लिए उपयुक्त जातियां (स्पीसीज ) हैं.
* बैंबूसा बाल्कोवा
* बैंबूसा टुल्डा
* डैंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस
प्रारंभ की 2 जातियों में बांस की कटाई ज्यादा आसान रहती है.
प्रवर्धन तकनीकी
पौधशाला में तैयार पौधे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इस तरह के पौधे स्वस्थ व तेज वृद्धि करने वाले होते हैं. बांस का प्रवर्धन पौधशाला में सीधे बीज की बोआई, प्रकंद रोपण, प्रशाखा (औफसैट), रोपण व नाल (कलम) रोपण द्वारा किया जाता है. प्रमुख विधियों की संक्षिप्त तकनीकी इस तरह है :
* बीज द्वारा सीधी बोआई : यह सब से सरल विधि है. इस में बांस के ताजा बीज को पौधशाला की क्यारियों में बोआई करते हैं. जब पौधे 8 से 10 सैंटीमीटर के हो जाते हैं, तब इन पौधो को पौलीथिन की थैलियों में दोबारा रोपित किया जाता है.
पर, अधिकतर बांस की जातियों (स्पीसीज) में पुष्पन व बीजीकरण सामूहिक (ग्रिगेरियस) रूप में औसतन 40 से 50 साल के बाद होता है, जिस के कारण बांस का बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है और बीजजनित पौधे धीमी वृद्धि करते हैं. इस वजह से आमतौर पर बांस का प्रवर्धन बीज से नहीं किया जाता है.
* प्रकंद रोपण : इस विधि में जीवित प्रकंद का 1-2 आंखों वाला तकरीबन 30 सैंटीमीटर लंबा भाग 45 घन सैंटीमीटर आकार के गड्ढे में रोपित किया जाता है.
गड्ढे में गोबर की खाद व मिट्टी का मिश्रण रोपण से पहले भर लिया जाता है.
* प्रशाखा (औफसैट) रोपण : यह एक प्रचलित विधि है. इस में प्रशाखा को रोपित किया जाता है. इस विधि में इस बात का ध्यान रखना जरूरी रहता है कि प्रशाखा में प्रकंद भाग के साथ एकवर्षीय कोमल नाल (कंड) का भी लगभग 70 से 80 सैंटीमीटर लंबा भाग जुड़ा हो.
प्रशाखा को तैयार करने के लिए सब से पहले बांस की कोठी से एकवर्षीय नाल को 70-80 सैंटीमीटर लंबाई पर तिर्यक रूप से काट कर इस को प्रकंद व जड़ सहित खोद लेते हैं. खोदते समय यह ध्यान रखें कि प्रकंद में कम से कम एक आंख जरूर हो.
इस तरह से तैयार प्रशाखा (औफसैट) को वर्षा ऋतु की शुरुआत में पर्याप्त आकार व गहराई के गड्ढे में इस प्रकार रोपित करते हैं कि 2-3 अंतर्गांठें (इंटरनोड) मिट्टी में दब जाएं व आंख को कोई क्षति न पहुंचे.
* बांसुरी विधि या नाल रोपण : अन्य विधियों जैसे प्रकंद, बीज आदि की तुलना में बांसुरी विधि बांस प्रर्वधन की एक उत्तम विधि है, जिस के द्वारा नर्सरी में कम समय में गुणवत्ता वाले व तेज वृद्धि करने वाले बांस के पौधे तैयार किए जा सकते हैं.
शुआट्स, इलाहाबाद द्वारा विकसित इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए अप्रैल माह में 18-24 माह पुराने, खोखले व पके बांस (गांठ पर कलीयुक्त) का चयन कर इस के 2-2 गांठ वाले टुकड़े काट लें और 2 गांठों के बीच 1 वर्ग इंच का छेद बना लें.
इस के बाद इन टुकड़ों को क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी के 2.5 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी के घोल में डुबो कर नर्सरी बैड में 8-10 सैंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी में दबा दें. छेद को किसी साफ प्लास्टिक शीट से ढक दें, ताकि छेद में मिट्टी न जा सके.
तने के छेद के अंदर 100 पीपीएम नैप्थलिन एसिटिक एसिड (एनएए) घोल डालें और शुरू के 2-3 माह तक हर हफ्ते प्लास्टिक शीट हटा कर निरीक्षण करते रहें व बांस के टुकड़ों के अंदर पानी कम होने पर जरूरत के मुताबिक पानी डालते रहें.
इस विधि द्वारा रोपित कलम/नाल से 10-12 दिनों में नए कल्ले व 45-60 दिनों में जड़ें आ जाती हैं. 6 से 9 माह के बाद इन कलमों को जमीन से जड़ सहित खोद कर आरी से गांठों को काट लें. इन गांठों को बड़ी पौलीथिन की थैली में दोबारा रोपित कर दें. 1-2 माह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है.
रोपण तकनीकी
रोपण की दूरी : बांस को खेत में 2 प्रकार से लगाया जा सकता है. पहले तरीके में मेंड़ पर 7-8 मीटर की दूरी पर और दूसरे तरीके में पंक्ति से पंक्ति एवं लाइन से लाइन 9-10 मीटर की दूरी पर पूरे खेत में सघन रोपण किया जा सकता है. प्रारंभ के कुछ वर्षों में बांस की कतारों के बीच उपयुक्त फसलें उगाई जा सकती हैं. डैंड्रोकेलेमस प्रजाति के रोपण के लिए रोपण की दूरी कम की जा सकती है.
रोपण की विधि : मार्चअप्रैल माह में उपरोक्त रोपण की दूरी पर 45 घन सैंटीमीटर आकार का गड्ढा खोद लें व खुदी हुई मिट्टी को गड्ढे के पास ऋतुक्षरण के लिए छोड़ दें, जिस से कड़ी धूप की वजह से गड्ढा कीट व रोगाणुओं से मुक्त हो सकें.
वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के 10 से 15 दिन पहले उक्त गड्ढों में गड्ढे की ऊपरी सतह की मिट्टी के साथ सड़ी गोबर की खाद (4:1 के अनुपात में), 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 50 ग्राम म्यूरेट औफ पोटाश और 25 ग्राम क्लोरोपाइरीफास धूल मिला कर भर दें. गड्ढों में भरी मिट्टी भूमितल से कुछ ऊंची होनी चाहिए. वर्षा ऋतु (जुलाईअगस्त माह) के समय उक्त गड्ढों में विभिन्न विधियों से तैयार पौधों, प्रकंद, कलम आदि का रोपण करना चाहिए.
बांस की फसल का प्रबंधन
खाद और उर्वरक : पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए रोपण के लगभग 45-50 दिन बाद व 7-8 माह के बाद प्रति पौध 50 ग्राम यूरिया रोपित पौधे के चारों तरफ मिला दें.
बाद के वर्षों में बांस के लिए किसी विशेष खाद और उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती है. फिर भी अच्छी वृद्धि के लिए प्रति वर्ष अगस्तसितंबर माह में 50 ग्राम यूरिया व 50 ग्राम डीएपी और सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति पुंज देनी चाहिए. हर एक पुंज को पुवाल या पत्ती के पलवार (मल्च) से ढकने पर नए बांस के कल्ले आने में आसानी रहती है.
पुंज की टैंडिंग व शाखा कर्तन क्रिया : मरे हुए पौधों व पुंज में बीमारी एवं कीड़ों द्वारा प्रभावित कलम को काट कर निकाल देें व पुंज से सभी प्रकार की झाडि़यों व लताओं को भी समयसमय पर निकालते रहें. जब (खासकर जुलाईसितंबर माह में) नई कोंपलें निकल रही हों, तब उस समय पुंज में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करनी चाहिए. इस समय साफसफाई आदि कामों के प्रभाव से नई कोंपलें प्रभावित हो सकती हैं.
बांस के रोपण के 15-16 महीने बाद नीचे की शाखाओं को काटा जा सकता है, पर 4-5 वर्ष पुराने बांस पुंज में यह क्रिया करनी ज्यादा लाभप्रद रहती है. शाखा कर्तन क्रिया हमेशा अक्तूबर से फरवरी माह के बीच करनी चाहिए. इस क्रिया के फलस्वरूप बांस निकालना आसान हो जाता है व पशुओं के लिए बांस की पत्तियों के रूप में चारा प्राप्त हो जाता है.
कीट व रोग प्रबंधन : बांस की पौधशाला में मुख्यत: डंपिंग औफ (आर्द्रगलन रोग) लगता है, जो एक फफूंदजनित रोग है. इस के नियंत्रण के लिए व्यापारिक ग्रेड की फार्मालीन को (15-20 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी के साथ) क्यारी की मिट्टी में डालना (ड्रैंचिंग) चाहिए.
इस के अतिरिक्त कार्बंडाजिम (2 ग्राम प्रति लिटर पानी) से भी क्यारियों का उपचार किया जा सकता है. रोपण से पहले भी पौधों को उक्त फफूंदनाशी से उपचारित करना बेहतर रहता है. प्रकंदों के रोपण के समय भी प्रकंद को कार्बंडाजिम के घोल में 3 से 5 मिनट डुबोने पर फफूंदजनित रोगों से बचाव में सहायता मिलती है.
बांस में झाड़ू रोग, राइजोम राट, बेसल कलम राट आदि बीमारियां लगती हैं, जिन्हें उचित फफूंदनाशी जैसे कार्बंडाजिम (3 ग्राम प्रति लिटर पानी), डाइथेन एम. 45 (3 ग्राम प्रति लिटर पानी), मैनकोजेब (2 ग्राम प्रति लिटर पानी) द्वारा रोग लगने की शुरुआती अवस्था में उपचार करने से रोका जा सकता है. यदि कोई बांस का पुंज फफूंद से पूरी तरह संक्रमित है, तो इस को पूरी तरह जला देना ज्यादा उचित रहता है.
बांस को 50 से अधिक प्रकार के कीट हानि पहुंचाते हैं, जिन में से सफेद ग्रब, दीमक, कटवर्म और तना छेदक कीट प्रमुख हैं. पौधशाला व रोपण में सफेद ग्रब व कटवर्म से बचाव के लिए फ्यूरोडौन 3 जी दवा (500 ग्राम प्रति 10 वर्गमीटर क्यारी या 100-150 ग्राम प्रति पुंज) का प्रयोग करना चाहिए.
दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास (2 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी) घोल का छिड़काव करें. लीफ रोलर कीट बांस की पत्तियों को मोड़ कर बीड़ी की तरह बना देता है, जिस के नियंत्रण के लिए कारटौप हाईड्रोक्लोराइड (1 ग्राम प्रति लिटर पानी) के घोल का छिड़काव करें.
नए कल्लों एवं बांस प्ररोह को तना छेदक भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिस के नियंत्रण के लिए हरे बांस एवं कल्लों की सब से नीचे की अंतर्गांठ (इंटरनोड) के ऊपरी भाग पर बारीक छेद कर लें, फिर उस छेद में डाईक्लोरोवाश कीटनाशी (2 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी) का घोल किसी इंजैक्शन या पिचकारी की सहायता से डाल दें, जिस से तना छेदक कीट नष्ट हो जाएगा.
 कटाई, उपज और आमदनी
कटाई, उपज और आमदनी
बांस की कटाई रोपण के 4-5 वर्षों के बाद प्रारंभ की जा सकती है. कटाई हमेशा सर्दी (नवंबरफरवरी माह) में ही करना उचित रहता है. 4-5 वर्षों के बाद प्रति बांस पुंज लगभग 6-10 बांस हर साल प्राप्त किया जा सकता है.
इस प्रकार 10×10 मीटर पर रोपित बांस के 1 हेक्टेयर रोपण (रोप वन) से लगभग 600 से 1,000 बांस हर साल प्राप्त किया जा सकता है. यदि एक बांस का औसत मूल्य 100 रुपए रखा जाए, तो 1 हेक्टेयर खेत से लगभग 60,000-1,00,000 रुपए कुल आय हर साल प्राप्त की जा सकती है.
बांस के रोपण और प्रारंभ के 2-3 वर्षों तक ही लागत लगती है, जो 22,000 से 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है. इस प्रकार 4-5 वर्षों के बाद बिना किसी विशेष लागत के बांस के 1 हेक्टेयर रोपण से औसतन 60,000 से 1,00,000 रुपए हर साल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है.
बांस को कागज मिल और शहर की बांस मंडियों में बेचा जा सकता है. शहरों व गांवों में घर बनाने के दौरान बांस की अच्छी मांग रहती है.








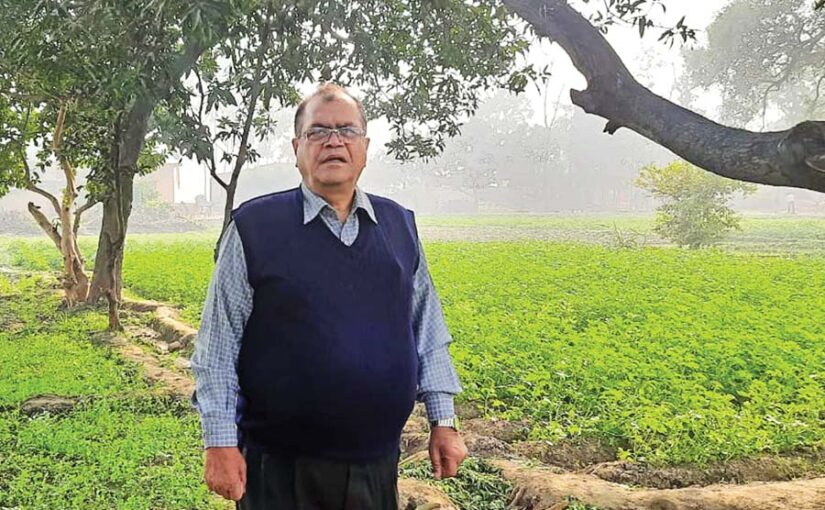


 उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय हमेशा इस तरह की पहल का समर्थन करता रहेगा. इसी तरह प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल का सक्रिय रूप से समर्थन कर के वन हेल्थ मिशन के लिए समर्थन भी जारी रहेगा. साथ ही, उन्होंने मनुष्यों, पशुधन और वन्यजीवों को शामिल करते हुए एकीकृत निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित किया.
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय हमेशा इस तरह की पहल का समर्थन करता रहेगा. इसी तरह प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल का सक्रिय रूप से समर्थन कर के वन हेल्थ मिशन के लिए समर्थन भी जारी रहेगा. साथ ही, उन्होंने मनुष्यों, पशुधन और वन्यजीवों को शामिल करते हुए एकीकृत निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित किया. कार्यशाला में वन्यजीवों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय रेफरल केंद्र के लिए विचारविमर्श किए गए फोकस क्षेत्रों पर जानकारी प्रदान की गई, जिस में शामिल हैं –
कार्यशाला में वन्यजीवों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय रेफरल केंद्र के लिए विचारविमर्श किए गए फोकस क्षेत्रों पर जानकारी प्रदान की गई, जिस में शामिल हैं –

 इस अवसर पर, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत स्पाइनलेस कैक्टस की खेती और इस के आर्थिक उपयोग को प्रोत्साहन देने में सहयोग पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएआरडीए) और राजस्थान राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
इस अवसर पर, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत स्पाइनलेस कैक्टस की खेती और इस के आर्थिक उपयोग को प्रोत्साहन देने में सहयोग पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएआरडीए) और राजस्थान राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. 15 राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 प्रतिनिधि, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), एमओए-एफडबल्यू, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ-सीसी), डीओआरडी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित उद्योग प्रतिनिधि और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), आईजीएफआरए, आईसीएआरडीए जैसे अन्य प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठन व संस्थान, सीएजेडआरआई, एनआरएए ने कार्यशाला में भाग लिया. कार्यशाला में भूमि संसाधन विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) और वाटरशेड प्रभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
15 राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 प्रतिनिधि, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), एमओए-एफडबल्यू, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ-सीसी), डीओआरडी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित उद्योग प्रतिनिधि और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), आईजीएफआरए, आईसीएआरडीए जैसे अन्य प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठन व संस्थान, सीएजेडआरआई, एनआरएए ने कार्यशाला में भाग लिया. कार्यशाला में भूमि संसाधन विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) और वाटरशेड प्रभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
 कटाई, उपज और आमदनी
कटाई, उपज और आमदनी
 सरसों में झुलसा रोग का प्रकोप ज्यादा हो सकता है. इस रोग में पत्तियों और फलियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिन में गोल छल्ले केवल पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिस से पूरी पत्ती झुलस जाती है.
सरसों में झुलसा रोग का प्रकोप ज्यादा हो सकता है. इस रोग में पत्तियों और फलियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिन में गोल छल्ले केवल पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिस से पूरी पत्ती झुलस जाती है.

