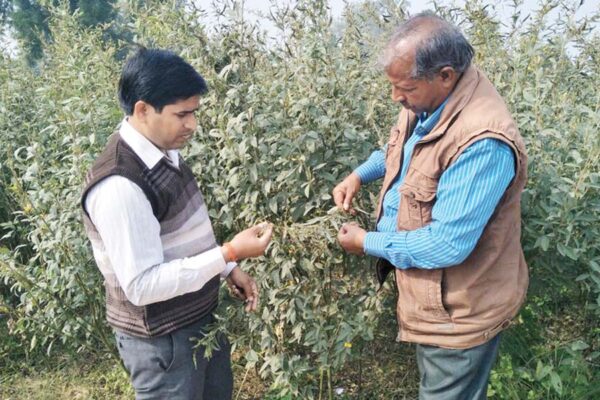बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर एक दिन नए प्रयोग और योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इस के लिए पिछले दिनों राज्य लैवल से ले कर जिला और ब्लौक लैवल पर गोष्ठियां, प्रदर्शनियां और ट्रेनिंग कार्यक्रमों का बेहद सफल आयोजन किया गया.
इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के कृषि महकमे के उद्यान निदेशालय द्वारा पटना के गांधी मैदान में बीते 3 जनवरी से 5 जनवरी, 2025 तक तीनदिवसीय बागबानी महोत्सव का आयोजन किया गया. इस बागबानी महोत्सव में बिहार के सभी जिलों से तकरीबन 1500 किसान 14 हजार से ज्यादा प्रविष्टियों के साथ शामिल हुए.
बागबानी महोत्सव में प्रदर्शनी में तकरीबन 60 स्टाल लगाए गए, जहां से खेतीबागबानी में रुचि रखने वाले लोगों ने अपने पसंद के फल, फूल, सब्जी के बीज/बिचड़ा, पौधा, गमला, मधु, मखाना, मशरूम आदि की खरीदारी भी की.
बागबानी महोत्सव का उद्घाटन राज्य के कृषि और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया. इस मौके पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी में उन्होंने राज्य के भूमिहीन किसानों को ले कर बड़ी घोषणा की.
बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कृषि विभाग बिहार में जल्दी ही शहद के उत्पादन और प्रोत्साहन के लिए नीति बनाएगा, जिसे सरकार राज्यभर में बढ़ावा देगी खासकर भूमिहीन किसानों को शहद उत्पादन से जोड़ने की पहल को ले कर नीति बनाई जाएगी.
भूमिहीन किसान मधुमक्खीपालन कर खुद को सशक्त बनाएंगे. सूरजमुखी, सहजन, सरसों, लीची जैसे फल, फूलों के शहद का उत्पादन करने की नीति बनेगी.
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है. रंगबिरंगे फल, फूल, सब्जी और अन्य बागबानी उत्पादों से सुसज्जित बागबानी महोत्सव, 2025 किसानों के उत्साह का गवाह है.
प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में किसानों की भूमिका
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में बागबानी खासकर फल, फूल, सब्जी, मसाला आदि की भूमिका अहम साबित हो रही है. साल 2005 के समय राज्य में प्रति व्यक्ति आय 7,500 रुपए के करीब थी, वहीं आज इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपए हो गई है.
उन्होंने आगे कहा कि बीते 20 वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में लगभग 8 गुना से अधिक प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जिस में किसानों की बढ़ी आय का बड़ा योगदान रहा है. अगर हम सभी राज्य को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो बागबानी के माध्यम से किसानों को समृद्ध कर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं.
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि महोत्सव में सिर्फ बागबानी उत्पादों का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि फल, फूल, सब्जी के बीज, बिचड़ा, पौधा, बागबानी उपकरण, मधु, मखाना, मशरूम, चाय आदि की बिक्री की भी व्यवस्था की गई है. बिहार में कुल 13.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागबानी फसलों की खेती की जाती है, जिस से तकरीबन 286.45 लाख मीट्रिक टन फल, फूल, सब्जी आदि का उत्पादन होता है, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाने का लक्ष्य है.
बागबानी क्षेत्र को बढ़ाने पर दिया जोर
कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कृषि रोडमैप के लक्ष्य से आगे बढ़ कर भी सोचने की जरूरत है. सालाना लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में भी हम सोच सकते हैं. हमें साल 2025 में बागबानी का लक्ष्य बढ़ा कर 18 लाख हेक्टेयर एवं 2026 में इसे बढ़ा कर 20 लाख हेक्टेयर पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए.
बागबानी के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है. आज हमारे किसान पारंपरिक बागबानी फसलों के साथसाथ उच्च बाजार मूल्य वाले एक्जोटिक फल, ड्रैगन फ्रूट्स, स्ट्राबेरी आदि की खेती कर रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि इन उत्पादों का उचित भंडारण हो, प्रसंस्करण यानी प्रोसैसिंग एवं मूल्य संवर्द्धन हो, बाजार की सुलभ उपलब्धता हो, इस दिशा में तीव्र गति से काम किया जा रहा है. इस कड़ी में राज्य सरकार के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि मार्केटिंग निदेशालय का गठन किया गया है, जिस का उद्देश्य किसानों को उन की उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना, किसानों को बाजार की व्यवस्था उपलब्ध कराना, किसानों के उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन कराना, भंडारण की सुविधा, बेहतर पैकेजिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है.
विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य बाजारोन्मुख बागबानी उत्पादों के गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए किसानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाना है, वहीं बागबानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी उपकरण से रूबरू कराना और किसानों को उन के उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त हो, इस के लिए निर्यात प्रोत्साहन के लिए किसानों और व्यापारियों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है.
इस अवसर पर अभिषेक कुमार, निदेशक उद्यान, आलोक रंजन घोष, एमडी, बिहार राज्य बीज निगम, अमिताभ सिंह, आप्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, संतोष कुमार उत्तम, निदेशक पीपीएम, वीरेंद्र प्रसाद यादव, विशेष सचिव, कृषि विभाग, पद्मश्री से सम्मानित किसान चाची राजकुमारी देवी, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव समेत कई अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

मन मोह लेने वाला रहा बागबानी महोत्सव, भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रविष्टियां
पटना के गांधी मैदान में लगाए गए बागबानी महोत्सव में सब्जी, फल, फूल और सजावटी पौधों को ले कर किसानों और शहरी क्षेत्र के लोगों से प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिस में उन के प्रविष्टियों की कोडिंग की गई थी. निर्णायक मंडल द्वारा निष्पक्ष रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों के साथ इंसाफ किया जा सके.
16 वर्गों में आयोजित की गई प्रतियोगिताएं
बागबानी महोत्सव में भाग लेने लिए किसानों और बागबानी प्रेमियों के लिए 16 वर्गों में प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं, जिस में सब्जी, मशरूम, फल, शहद, पान, कटे फूल डंठल सहित, औषधीय एवं सुगंधित पौधा, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, फल संरक्षण (घर की बनी), शोभाकार पत्तीदार पौधा, बोनसाई, जाड़े के मौसमी फूलों के पौधे, कैक्टस एवं सकुलेंट पौधा, विभिन्न तरह के पाम, कलात्मक पुष्प सज्जा एवं नक्काशी शामिल रहा. इन वर्गों को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया था.
इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक वर्ग से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में नकद इनाम भी दिया गया. इस के अंतर्गत महोत्सव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 4,000 रुपए व तृतीय पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपए प्रदान किए गए.
रंगबिरंगे फूलों और सजावटी पौधों ने मोहा मन, ली जम कर सैल्फी
बिहार सरकार द्वारा पटना के गांधी मैदान में लगाए गए बागबानी महोत्सव में चारों तरफ रंगबिरंगे फूलों की खुशबू बिखरी रही और इन पौधों ने लोगों को सैल्फी लेने को मजबूर कर दिया.
प्रदर्शनी में ये पौधे विभिन्न प्रतियोगियों द्वारा प्रतियोगिता में इनाम पाने के लिए प्रदर्शित किए गए थे. इस के तहत कैक्टस, पाम, गुलाब, गेंदा, सकुलेंट, पान, क्रोटन, गुलदाउदी, जरबेरा, एलोवेरा, विभिन्न पेड़ों के बोनसाई के हजारों की संख्या में पौधे शामिल रहे, जबकि एक विशिष्ट पुरस्कार के लिए 10,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया.
रंगीन और विदेशी सब्जियों को देख हैरान हुए लोग
गांधी मैदान में लगाए तीनदिवसीय बागबानी महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान फल, फूल और सब्जियों के पौधे ले कर प्रतियोगिता में शामिल होने आए थे, जिन्हें प्रदर्शन के लिए आम दर्शकों के लिए रखा गया था. इन प्रतियोगिताओं में आदमकद और जंबो साइज की सब्जियां और फलफूल देखने को मिले.
इस में 20 से 40 किलोग्राम का कद्दू, 5 से 10 किलोग्राम की फूलगोभी, डेढ़ किलोग्राम तक की गांठगोभी, जंबो साइज के सूरन, लौकी, बैगन, टमाटर, बंदगोभी, सेम, गाजर, आलू, मटर, अदरक, हलदी, ड्रैगन फ्रूट के अलावा जैविक तरीके से उगाए गए फलफूल और सब्जी को देख कर लोग हैरान हो कर फोटो और वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं पाए.
प्रदर्शनी में विदेशी सब्जियों में पाकचोई, जुकुनी सहित कई सब्जियां भी प्रतियोगिता के लिए रखी गई थीं, जिस का परिचय जानने के लिए लोग उत्सुक रहे.
चोरमा गांव के बाशिंदे सुरेश गिरी इस महोत्व में हरी मिर्च के पौधे ले कर आए थे. उन के एक पौधे में 60 मिर्चें लगी हुई थीं. वे बताते हैं कि उन्होंने जैविक तरीके से 2 कट्ठे में मिर्च की खेती की. एक कट्ठा में मिर्च गाने में 10,000 रुपए खर्च होते हैं और कमाई तकरीबन 60,000 रुपए होती है.
 प्रदर्शनी के स्टालों पर खूब बिकी बागबानी से जुड़ी चीजें
प्रदर्शनी के स्टालों पर खूब बिकी बागबानी से जुड़ी चीजें
बागबानी महोत्सव में बागबानी से जुड़े उपकरणों, खाद, उर्वरक, बीज, पौधे, गमले इत्यादि से जुड़े लगभग 60 स्टाल लगाए गए थे. जिस में निजी कंपनियों से ले कर सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय, आईसीएआर से जुड़े संस्थान और महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोग शामिल रहे.
इन स्टालों पर लोगों ने बागबानी से जुड़े ब्रांडेड कंपनियों के छोटेछोटे मैनुअल उत्पाद और उपकरण तो खरीदे ही, साथ में उन्नत किस्मों के बीज और पौधों की भी जम कर खरीदारी की.
इस महोत्सव में राष्ट्रीय बीज निगम के स्टाल पर मोटे अनाज, फल, फूल और सब्जियों के प्रमाणित बीजों की खूब बिक्री हुई, जिस में मंडुआ, सांवा, मटर, धनिया, कैलेंडुला, बैगन, मूली, लाल साग और प्याज के बीज आदि शामिल रहे.
इसी तरह 3 रुपए प्रति पौध की दर से टमाटर, बैगन, पत्तागोभी, लाल फूलगोभी का पौधा भी खूब बिका. एक स्टाल पर बिना बीज वाला खीरा 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिका, जो खाने में बिलकुल भी तीखा नहीं होता. इसी तरह आम, अमरूद, चीकू और आंवला के पौधों की बिक्री भी जम कर हुई.
 बिहारी व्यंजनों का स्वाद
बिहारी व्यंजनों का स्वाद
बागबानी महोत्सव न केवल किसानों और बागबानी में रुचि रखने वाले लोगों के लिए खास रहा, बल्कि यह महोत्सव खानेपीने वाले लोगों को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा.
महोत्सव में बिहार के स्थानीय पारंपरिक व्यंजनों का भी स्टाल लगाया गया था, जहां लिट्टीचोखा, मशरूम के व्यंजन, मंगोड़े इत्यादि का भी लोगों ने जम कर स्वाद लिया.
छत पर फार्मिंग बैड योजना एवं गमले पर मिल रहा अनुदान
बिहार सरकार द्वारा चुनिंदा जनपदों में छत पर खेती किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए छत पर बागबानी योजना के तहत सहायता अनुदान मुहैया कराया जा रहा है, जिस का उद्देश्य शहरों में रहने वाले लोगों में जैविक उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देने सहित छत पर खेती के जरीए शहरी प्रदूषण में कमी लाना और सब्जियों, फलों के ऊपर लोगों की बाजार पर निर्भरता को कम करना भी है.
यह योजना उन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है, जिन के पास अपनी खुद की खेती के लिए जमीन नहीं है. वे लोग अगर खेती और बागबानी में रुचि रखते हैं, तो अपने घर की छत पर शौक को अमलीजामा पहना कर अपने इस शौक को पूरा कर सकते हैं.
बागबानी महोत्सव में इस योजना के प्रचारप्रसार के लिए लाइव डैमो प्रदर्शन किया गया था, जहां इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियों सहित योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों का मौके पर ही पंजीकरण किया गया.
योजना से जुड़ी खास बातें
योजना से जुड़े उपकरण, बीज पौधे व अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराने वाली एक कंपनी से जुड़े विकास कुमार ने महोत्सव में उक्त योजना का डैमो प्रदर्शन लगा रखा था. इस दौरान उन्होंने बातचीत में बताया कि अभी केवल बिहार के पटना सदर, दानापुर, फुलवारी एवं खगौल और भागलपुर, गया एवं मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र में इस योजना का लाभ लिया जा सकता है. जिस के पास अपना घर हो अथवा अपार्टमेंट में फ्लैट हो, जिस की छत पर 300 वर्ग फुट की जगह हो, वे फार्मिंग बैड योजना का लाभ ले सकते हैं.
उन्होंने आगे बताया कि स्वयं के मकान की स्थिति में छत पर 300 वर्ग फुट खाली स्थल, जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो और अपार्टमेंट की स्थिति में अपार्टमेंट की पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होना जरूरी है.
विकास कुमार ने बताया कि फार्मिंग बैड योजना के अंतर्गत प्रति इकाई (300 वर्ग फुट) का इकाई लागत 48574 रुपए एवं अनुदान 75 फीसदी और शेष 12143.50 रुपए लाभार्थी द्वारा दिया जाना है. इसी तरह गमले की योजना के अंतर्गत प्रति इकाई लागत 8975 रुपए एवं अनुदान 75 फीसदी और शेष 2243.75 रुपए लाभार्थी द्वारा देय होगा.
उन्होंने यह भी बताया कि आवेदन करने के बाद फार्मिंग बैड योजना के अंतर्गत प्राप्त रसीद पर लाभार्थी को अपने अंश की राशि 12143.50 रुपए प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) और गमले की योजना के अंतर्गत प्राप्त रसीद पर लाभुक को अपने अंश की राशि 2243.75 रुपए प्रति इकाई जमा करने के लिए बैंक खाता संख्या एवं विस्तृत विवरणी प्राप्त होगी.
संबंधित जिले के संबंधित खाता संख्या में लाभुक अंश की राशि जमा होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी द्वारा छत पर लगे बागबानी इकाई का रखरखाव स्वयं के स्तर से करना अनिवार्य होगा.
उन्होंने बताया कि फार्मिंग बैड योजना के अंतर्गत स्वयं के मकान की स्थिति में 2 इकाई और अपार्टमेंट एवं शैक्षणिक/अन्य संस्थान के लिए अधिकतम 5 इकाई का लाभ दिया जाएगा. गमले की योजना का लाभ संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा और गमले की योजना का लाभ किसी आवेदक द्वारा अधिकतम 5 यूनिट तक लिया जा सकेगा.
विकास कुमार ने बताया कि इस योजना की गाइडलाइन के अनुसार चयन के लिए जिले के लक्ष्य के अंतर्गत 78.60 फीसदी सामान्य जाति, 20 फीसदी अनुसूचित जाति और 1.40 फीसदी अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिस में कुल भागीदारी में 30 फीसदी महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है.
गमला योजना में शामिल हैं ये चीजें
गमला योजना के तहत 30 गमले में अलगअलग तरह के पौधे लगा कर दिए जाएंगे. इस में तुलसी, अश्वगंधा, एलोवेरा, स्टीविया, पुदीना, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, गुलाब, चांदनी, एरिका पाम, अपराजिता, करीपत्ता, बोगनविलिया, अमरूद, आम, नीबू, चीकू, केला, रबर आदि के पौधे रहेंगे. इन में 10 इंच के 5, 12 इंच के 5, 14 इंच के 10 और 16 इंच के 10 गमले दिए जाएंगे. इस योजना की लागत 8,974 रुपए की है, लेकिन 75 फीसदी अनुदान के बाद आवेदक को केवल 2,244 रुपए ही देने होंगे.
12,000 रुपए में छत पर बागबानी का सपना होगा सच
फार्मिंग बैड योजना के तहत लाभार्थी के घर की छत पर कई तरह के फार्मिंग बैड और बैग लगाए जाएंगे. इन में 10 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा 3 फार्मिंग बैड, 2 फुट लंबा और एक फुट चौड़ा एक फार्मिंग बैग, 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा 6 बैग लगाए जाएंगे. इस में ड्रिप सिस्टम और मोटर लगा कर दिया जाएगा. ड्रिप सिस्टम में लगे स्विच को चालू करते ही पौधों की सिंचाई हो जाएगी. साथ ही, 30 किलोग्राम कोकोपिट और 50 किलोग्राम वमीं कंपोस्ट दिया जाएगा.
फार्मिंग बैड योजना के तहत लोगों को मौसमी सब्जी और फल के पौधे लगा कर इस योजना के तहत 9 माह तक प्रबंधन का काम एजेंसी ही करेगी. इस दौरान एजेंसी के लोग 18 बार निरीक्षण करने आएंगे. पौधों का विकास, उन की जरूरत के हिसाब से वे काम करेंगे.
एजेंसी पूरी करेगी जरूरतें
सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लोगों को आसानी से मुहैया हो पाए, इस के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि आवेदन के लिए कहीं चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े. इस के लिए सबकुछ एजेंसी पहुंचाने का काम कर रही है. इस योजना के लिए आवेदक को निदेशालय की वैबसाइट https:// horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा. इस वैबसाइट पर ही औनलाइन आवेदन करना होगा. इस के बाद आवेदन किए जाने के 10 दिन के अंदर ही आप के घर की छत पर बागबानी कर दी जाएगी.









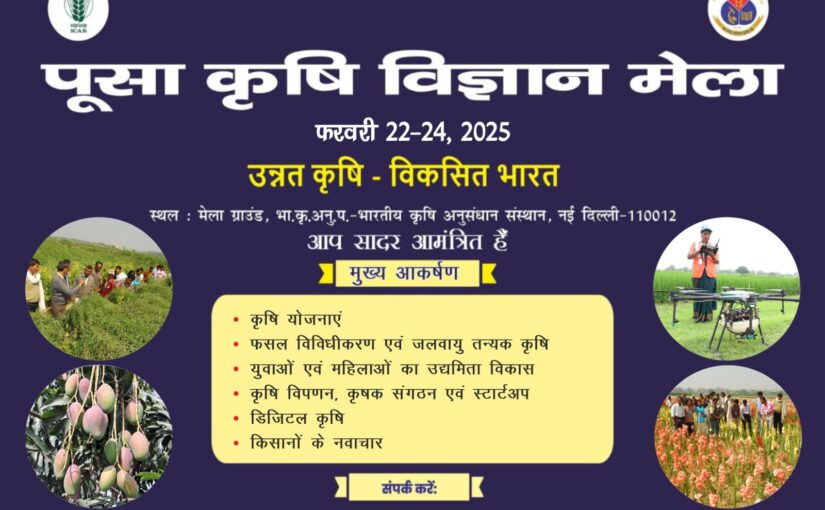







 प्रदर्शनी के स्टालों पर खूब बिकी बागबानी से जुड़ी चीजें
प्रदर्शनी के स्टालों पर खूब बिकी बागबानी से जुड़ी चीजें बिहारी व्यंजनों का स्वाद
बिहारी व्यंजनों का स्वाद