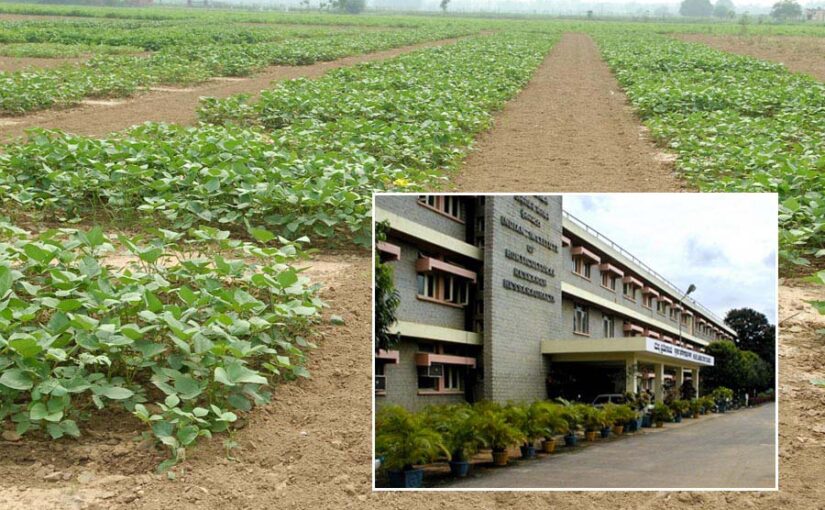हिसार : पिछले दिनों चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ‘रिसर्च मैनेजमेंट’ विषय पर 21दिवसीय रिफ्रैशर कोर्स संपन्न हुआ. विश्वविद्यालय के मानव संसाधन प्रबंधन निदेशालय द्वारा आयोजित किए गए इस रिफ्रैशर कोर्स में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय व लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों ने भाग लिया. कार्यक्रम में कुलपति प्रो. बीआर कंबोज मुख्यातिथि के तौर पर उपस्थित रहे.
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने रिफ्रैशर कोर्स के समापन अवसर पर वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नए अनुसंधानों को बढ़ावा देना जरूरी है. कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए तापमान रोधी नईनई किस्में व नई तकनीक विकसित करने के लिए और अधिक बेहतर ढंग से काम करना होगा.
उन्होंने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में असमय तापमान की बढ़ोतरी से निबटने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को शोध कार्यों एवं अनुसंधानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना बना कर काम करना होगा. इस के साथसाथ नए उत्पादों को विकसित करने वाले अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से छोटे किसानों को नवीनतम तकनीकों के माध्यम से कम लागत में अधिक पैदावार की ओर अग्रसर कर के उन की माली हालात को मजबूत करना है.
उन्होंने वैज्ञानिकों से कृषि क्षेत्र में आने वाली मुख्य चुनौतियों पर अधिक से अधिक शोध करने एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने की हिदायत दी. साथ ही, शोध कार्यों, नई कृषि तकनीकों, नवाचारों के साथसाथ कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने पर ज्यादा से ज्यादा काम करें.
रिफ्रेशर कोर्स में सभी वैज्ञानिकों ने अपना एकएक रिसर्च प्रोजैक्ट प्रस्तुत किया. कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने वैज्ञानिकों को 15 दिन के अंदर इस रिसर्च प्रोजैक्ट को संबंधित एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए. उन्होंने कार्यक्रम के समापन अवसर पर कोर्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र बांटे.
मानव संसाधन प्रबंधन निदेशक डा. अतुल ढींगड़ा ने अतिथियों व प्रतिभागियों का स्वागत किया. उन्होंने रिफ्रेशर कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उपरोक्त निदेशालय की संयुक्त निदेशक एवं कोर्स समन्वयक डा. रेणु मुंजाल ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान किए गए विभिन्न विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जबकि प्रशिक्षण सहसमन्वयक डा. जितेंद्र भाटिया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया.
मंच का संचालन डा. जयंती टोकस ने किया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, निदेशक, अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे.