जिस तरह से जीवजंतुओं व प्राणियों में अच्छी सेहत के लिए अनेक पोषक तत्त्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से खेत की मिट्टी से अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्हें भी पोषक तत्त्वों की जरूरत होती है. अगर खेत की मिट्टी में समुचित मात्रा में पोषक तत्त्व मौजूद हैं तो हमें खेती से अच्छी उपज मिलेगी.
खेत की मिट्टी परीक्षण के लिए समयसमय पर मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए. मिट्टी की जांच से हमें उस में मौजूद लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता की जानकारी मिलती है.
पौधों में समुचित विकास के लिए उन्हें 16 पोषक तत्त्वों की जरूरत होती है, जिस में खासकर हाइड्रोजन, औक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि होते हैं.
सामान्य तौर पर मिट्टी में ये सभी तत्त्व मौजूद होते हैं, लेकिन लगातार अनेक तरह की फसल लेने से इन में अनेक पोषक तत्त्वों में कमी आ जाती है. इस के अलावा खेत में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थ व खेत में ही फसल अवशेषों का जला देना आदि भी खेत की मिट्टी खराब करते हैं और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्त्वों में असमानता आ जाती है, जिस के चलते हमें उचित पैदावार भी नहीं मिल पाती है.
इसी कमी की भरपाई के लिए खेत का मिट्टी परीक्षण कराना अच्छा रहता है. मिट्टी जांच के बाद जो संस्तुति या नतीजे मिलते हैं, उसी के अनुसार खेत में उर्वरक व खादबीज आदि डाले जाते हैं.
मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आसान है और सभी की पहुंच में भी. जरूरत है, केवल जागरूकता की.
जानकारी के लिए बता दें कि भारत में मिट्टी जांच की शुरुआत साल 1956 में हुई थी और शुरुआत के समय 24 मिट्टी जांच केंद्र खोले गए थे.
लेकिन तब और अब में बहुत बदलाव आ चुका है. उन दिनों पारंपरिक खेती का दौर था, कृषि रसायनों का इस्तेमाल भी नहीं होता था. लेकिन अब खेती में कृषि रसायनों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आज के समय में ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच समयसमय पर कराते रहें और उसी के अनुसार खेती को करें.
आज तो चंद कदमों की दूरी पर मिट्टी जांच की सुविधाएं भी हैं. किसान के काम भी आसान हो रहे हैं, इसलिए सही समय पर सही तरीके से मिट्टी की जांच करानी चाहिए.
मिट्टी नमूना लेने की सही विधि
सब से पहले खेत का मुआयना कर के उसे ढलान, रंग, फसलोत्पादन और आकार के अनुसार उचित भागों में बांट लें. इस के बाद प्रत्येक भाग में टेढ़ेमेढ़े चलते हुए 15-20 निशान लगा लें. इस के बाद खेत में अलगअलग जगहों से मिट्टी लें.
औजारों का चयन
ऊपरी सतह से नमूना लेने के लिए खुरपी या ट्यूब, आगर, अधिक गहराई से या गीली मिट्टी से लेने के लिए पोस्ट होल आगर और सख्त मिट्टी से नमूना लेने के लिए बरमे (स्क्रू आगर) का प्रयोग करें. गड्ढे खोदने के लिए कस्सी, फावड़ा या बेलचा का प्रयोग करें अथवा लंबी छड़ वाले आगर का प्रयोग करें.
नमूने की गहराई
अन्न, दलहन, तिलहन, गन्ना, कपास, चारे, सब्जियों और मौसमी फलों आदि के लिए ऊपरी सतह (0-15 सैंटीमीटर) से 15-20 निशानों से नमूना लें. बाग या अन्य वृक्षों के लिए 0-30, 30-60 और 60-90 सैंटीमीटर तक के अलगअलग नमूने लें. सतह से नमूने लेने के लिए खुरपी की सहायता से ‘वी’ के आकार का गड्ढा 15 सैंटीमीटर की गहराई तक बनाएं और एक किनारे से लगभग 2 सैंटीमीटर मोटी परत लें.
नमूना तैयार करना
एक खेत या एक बाग से लिए गए सभी नमूनों को एक बिलकुल साफ सतह पर या कपड़े या पौलीथिन शीट पर रख कर खूब अच्छी तरह मिला लें. पूरी मात्रा को एकसमान मोटाई में फैला लें और हाथ से 4 बराबर भागों में बांट लें. आमनेसामने वाले 2 भाग हटा दें और शेष 2 को फिर मिला कर 4 भागों में बांट दें. यह क्रिया तब तक दोहराते रहें, जब तक लगभग आधा किलोग्राम मात्रा न बच जाए.
नाम, पता आदि लिखना
अंत में बची हुई लगभग आधा किलोग्राम मिट्टी को कपड़े, कागज या पौलीथिन की साफ (नई) थैली में रख कर उस पर किसान का नाम, पता नमूना संख्या लिख दें. अलग से एक कागज पर यही विवरण लिख कर थैली के अंदर भी रख दें. मिट्टी गीली हो, तो छाया में सुखा कर थैली में रख दें और 2-3 दिन में ही प्रयोगशाला में भेज दें.
नमूनों पर पहचान चिह्न, नमूने की गहराई, फसल प्रणाली, प्रयोग की गई खादों व उर्वरकों की मात्रा और समय, सिंचाई की सुविधा, जलनिकास आदि की जानकारी के अतिरिक्त वांछित फसल का नाम भी लिखें.
सावधानियां
खेत में अलगअलग जगहों से नमूने लें. प्रयोग में लाए जाने वाले औजार, थैलियां आदि बिलकुल साफ होनी चाहिए. मिट्टी नमूनों को खाद, उर्वरक, दवाओं आदि के संपर्क में न आने दें. नमूना लेते समय सतह पर पड़ा हुआ कूड़ा, खरपतवार, गोबर आदि पहले ही हटा दें. पेड़ों के नीचे और खाद के गड्ढों के आसपास नमूने न लें.
मिट्टी परीक्षण का समय
फसल बोने या रोपाई करने के एक माह पूर्व खाद व उर्वरकों के प्रयोग से पहले ही मिट्टी परीक्षण कराएं. आवश्यकता हो तो खड़ी फसल में से भी कतारों के बीच से नमूने ले कर परीक्षण के लिए भेज सकते हैं, ताकि खड़ी फसल में पोषण सुधार किया जा सके.
साधारण फसलों के लिए 1 या 2 वर्ष में एक बार मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए. फसल कमजोर होने पर बीच में तुरंत समाधान के लिए परीक्षण कराया जा सकता है. खेती आरंभ करने से पूर्व पूरे फार्म की मिट्टी का परीक्षण करा लेना बहुत आवश्यक है.
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं
इस समय देश के लगभग प्रत्येक जिले में ऐसी प्रयोगशालाएं हैं. इस के लिए अपने निकटतम कृषि विकास अधिकारी अथवा विकास खंड अधिकारी से संपर्क करें.
पूसा, नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मृदा एवं पादप परीक्षण प्रयोगशाला में इस के लिए किसान और उद्यमी देश के किसी भी भाग से कभी भी संपर्क कर के मिट्टी परीक्षण और वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही जानकारी का पूरा लाभ उठा सकते हैं.
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की कुछ विशेषताएं
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मृदा एवं पादप परीक्षण प्रयोगशाला विश्वसनीय परीक्षण सेवा के लिए काफी प्रसिद्ध है. यहां मिट्टी व सिंचाई जल के अतिरिक्त कार्बनिक खाद तथा पौधों के विश्लेषण की सुविधा भी उपलब्ध है.
इस प्रयोगशाला में विभिन्नविभिन्न संस्थाओं में सेवारत अधिकारियों के लिए हर साल मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है.
परीक्षण संबंधी जानकारी और आवश्यक कदम उठाने के लिए यहां मृदा वैज्ञानिकों से सीधा संपर्क हो जाता है और वैज्ञानिक खेती या नई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए सुझाव मिल जाते हैं.
 विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में परिसर में परीक्षा केंद्र बनाया था. इस प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया गया था. परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षार्थी की फोटोग्राफी भी की गई.
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में परिसर में परीक्षा केंद्र बनाया था. इस प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया गया था. परीक्षा के दौरान प्रत्येक परीक्षार्थी की फोटोग्राफी भी की गई.









 उन्होंने आगे कहा कि संस्थान में जो यहां सीखा, उस को अपने फार्म पर जा कर धीरेधीरे अपनाना है और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपनी खेती और पशुपालन को उद्यमिता की ओर ले जाए.
उन्होंने आगे कहा कि संस्थान में जो यहां सीखा, उस को अपने फार्म पर जा कर धीरेधीरे अपनाना है और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपनी खेती और पशुपालन को उद्यमिता की ओर ले जाए.

 अर्जुन मुंडा ने पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान परिसर में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और स्थानीय किसानों के साथ बातचीत की. इस अवसर पर उन्होंने किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया, जो देश की अर्थव्यवस्था में महान योगदान देते हैं.
अर्जुन मुंडा ने पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान परिसर में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और स्थानीय किसानों के साथ बातचीत की. इस अवसर पर उन्होंने किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया, जो देश की अर्थव्यवस्था में महान योगदान देते हैं. मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान समुदाय से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम फसल बीमा और पीएम किसान समृद्धि जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाएं.
मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान समुदाय से आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम फसल बीमा और पीएम किसान समृद्धि जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाएं.
 उन्होंने बताया कि इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यकम, जो केंद्र सरकार द्वारा पोषित है और राज्य सरकार द्वारा संचालित है, में समस्त पशुपालकों के द्वार पर उन के पशुओं में निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है. इस कार्यकम में टीकाकरण से पूर्व कान में छल्ला लगवाना (ईयर टैगिंग) अनिवार्य है.
उन्होंने बताया कि इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यकम, जो केंद्र सरकार द्वारा पोषित है और राज्य सरकार द्वारा संचालित है, में समस्त पशुपालकों के द्वार पर उन के पशुओं में निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है. इस कार्यकम में टीकाकरण से पूर्व कान में छल्ला लगवाना (ईयर टैगिंग) अनिवार्य है.

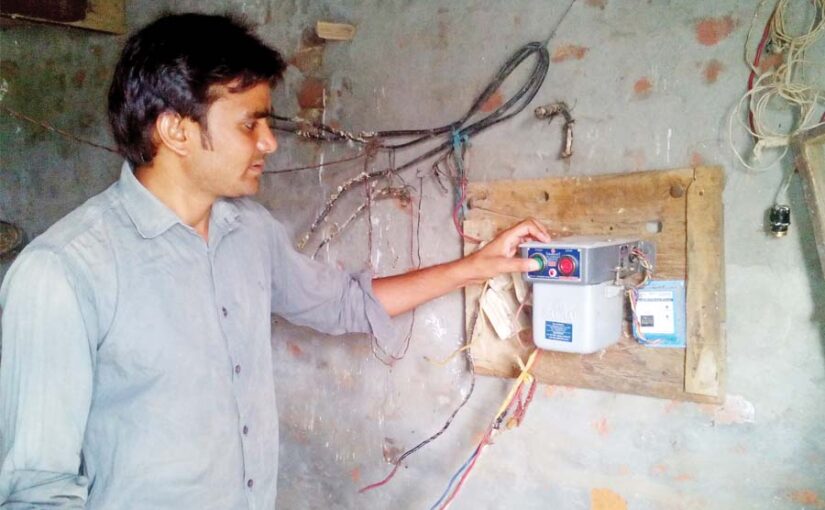
 इन दर्दनाक हादसों से सबक लेना चाहिए. लेकिन पेट की आग के मारे ज्यादातर किसान इतना सबकुछ देखनेसुनने और पढ़ने पर भी कुछ खास सावधानियां नहीं बरतते.
इन दर्दनाक हादसों से सबक लेना चाहिए. लेकिन पेट की आग के मारे ज्यादातर किसान इतना सबकुछ देखनेसुनने और पढ़ने पर भी कुछ खास सावधानियां नहीं बरतते.
 गौरतलब है कि इस कौशल विकास कार्यक्रम के प्रतिभागी ग्रामीण बकरी दुग्ध उत्पादक हैं और वो यहां कौशल विकास एवं ज्ञान उन्नयन के साथसाथ आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए विषय विशेषज्ञों से जानकारी लेने के उद्देश्य से आए थे. प्रतिभागियों को बकरी दुग्ध उत्पादन एवं संरक्षण की प्रचलित विधियों के साथ आधुनिक विधियों का दृश्य श्रृव्य माध्यम से विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया गया और दोनों विधियों के फायदे एवं नुकसान बताए गए. बकरी दुग्ध ग्रामीण स्तर का प्रचलित एवं प्रसिद्ध उत्पाद है एवं पौष्टिकता से भरपूर बकरी दुग्ध में अपार व्यावसायिक संभावनाएं हैं.
गौरतलब है कि इस कौशल विकास कार्यक्रम के प्रतिभागी ग्रामीण बकरी दुग्ध उत्पादक हैं और वो यहां कौशल विकास एवं ज्ञान उन्नयन के साथसाथ आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए विषय विशेषज्ञों से जानकारी लेने के उद्देश्य से आए थे. प्रतिभागियों को बकरी दुग्ध उत्पादन एवं संरक्षण की प्रचलित विधियों के साथ आधुनिक विधियों का दृश्य श्रृव्य माध्यम से विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया गया और दोनों विधियों के फायदे एवं नुकसान बताए गए. बकरी दुग्ध ग्रामीण स्तर का प्रचलित एवं प्रसिद्ध उत्पाद है एवं पौष्टिकता से भरपूर बकरी दुग्ध में अपार व्यावसायिक संभावनाएं हैं.