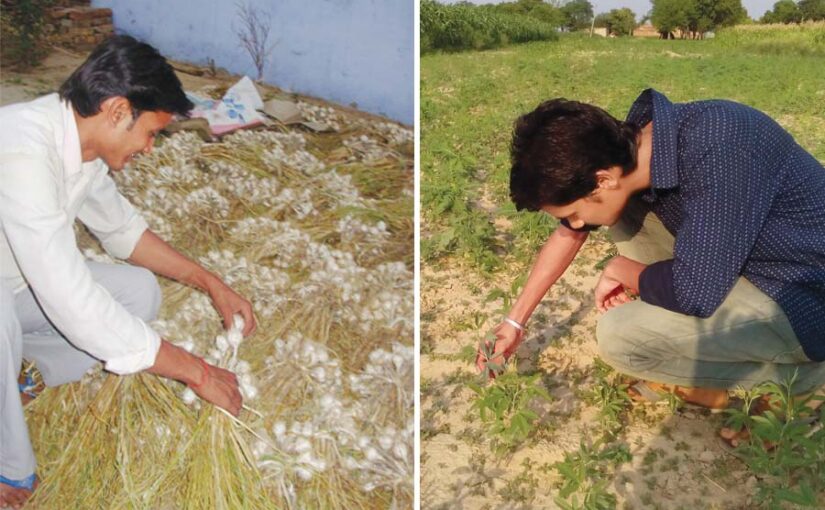घरआंगन हो या खेतखलिहान, हर जगह चूहों (Rats) का आतंक है. हर कोई इन के तांडव से परेशान जरूर होता है. ऐसे में चूहों (Rats) का प्रभावी नियंत्रण हम सभी को जरूर करना चाहिए.
घरआंगन के अलावा चूहे (Rats) खेतखलिहानों में सब से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इस के अलावा भारी मात्रा में मल त्याग करने व काटने, कुतरने की आदत के चलते बहुत सी बीमारियों के वाहक भी बनते हैं.
एक अनुमान के मुताबिक, देश में पैदा होने वाले कुल खाद्यान्न का तकरीबन 10 फीसदी सिर्फ चूहे ही हजम कर जाते हैं. इन की आबादी भी काफी तेजी से बढ़ती है. चूहे मात्र 5 हफ्ते में ही मैथुन के योग्य हो जाते हैं. एक मादा चूहा सालभर में 6-10 बार बच्चा देती है व एक बार में 6-12 बच्चे दे सकती है.
एक जोड़ी चूहे को अगर नियंत्रित न किया जा सके तो सालभर में ये 1,000-1,200 तक तादाद बढ़ा सकते हैं.
चूहे प्रमुखत: 4 प्रकार के पाए जाते हैं. पहला, घरेलू चूहा, जो सिर्फ घरों में ही पाया जाता है. दूसरा, खेत में चूहे, जो खेत और खलिहान दोनों में पाए जाते हैं. तीसरा, खेत और घर दोनों जगह के चूहे और चौथा, जंगली चूहे, जो जंगलों व रेगिस्तानों में रह कर घासफूल, फलफूल वगैरह खा कर अपना पेट भरते हैं.
चूहे भले ही अलगअलग प्रकार के हैं, मगर इन सब का नियंत्रण इन तरीकों से होता है:
गैररसायनिक तरीका
प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा : गैररसायनिक तरीके में चूहों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे बिल्ली, सियार, कुत्ता, उल्लू, चमगादड़, लोमड़ी, चील जैसे जीवों को रख कर नियंत्रित कर सकते हैं. ये सभी जीव चूहों को खा जाते हैं.
चूहेदानी द्वारा : चूहेदानी में चूहों की पसंद की चीजें जैसे रोटी, डबलरोटी, बिसकुट, अमरूद वगैरह रख कर फंसा लिया जाता है. बाद में उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है.
चूहा अवरोधी भंडारण द्वारा : भंडारण पक्के कंक्रीट के फर्श पर या धातुओं जैसे जस्ता, लोहा, तांबा, वगैरह से बने पात्र में करना चाहिए.
साफसफाई द्वारा : चूहों का स्थायी घर झाडि़यों, कूंड़ों, मेंड़ों वगैरह में होता है, जिस की बेहतर ढंग से साफसफाई कर के चूहों की आबादी घटाई जा सकती है.
रासायनिक तरीका
5 दिवसीय योजना बना कर : चूहे बड़े चालाक होते हैं. मुमकिन है कि अचानक से कोई दवा रखने पर उसे न खाएं और चूहों का खात्मा रासायनिक दवा देने पर भी न हो सके, इसलिए एक 5 दिवसीय योजना बनानी चाहिए.
पहले दिन बिलों का निरीक्षण कर उन्हें मिट्टी से बंद कर देना चाहिए. दूसरे दिन खुले हुए बिल के पास सादा चारा रखना चाहिए. तीसरे दिन दोबारा बिलों के पास सादा चारा रखना चाहिए और चौथे दिन जहरीला चारा बना कर रखना चाहिए. इस के लिए 48 भाग चारा जैसे गुड़, चना, चावल, डबलरोटी वगैरह में 1 भाग जिंक फास्फाइड नामक दवा और एक भाग सरसों का तेल मिला कर देना चाहिए. 5वें दिन बिलों में धूम्रण के लिए 1-2 टैबलेट सल्फास एल्यूमिनियम फास्फाइड 15 फीसदी की गोली रख कर बिल को बंद कर दें.
बांझ करने वाले रसायनों द्वारा : चूहों के नियंत्रण का एक बेहतर उपाय यह भी है कि उन की आबादी बढ़ने ही न पाए, इस के लिए बाजार में अनेक तरह के रसायन आते हैं. चूहे इन्हें खा कर नपुंसक बन जाते हैं.
प्रमुख रसायनों में फुराडेंटीन नाम की दवा की एक गोली (0.2 ग्राम प्रति चूहा) व कोल्चीसीन की एक टैबलेट का 5वां हिस्सा खाने की चीजों में मिला कर चूहों को खिलाने से नपुंसक हो जाते हैं.
धूम्रण के द्वारा : साइमेग या साइनो गैस पाउडर, एल्यूमिनियम फास्फाइड वगैरह दवाओं की 3-4 ग्राम मात्रा हर एक बिल में डाल कर बिल बंद कर देने से चूहे मर जाते हैं.
जिंक फास्फाइड द्वारा : चूहों को खत्म करने के लिए यह सब से असरकारक रसायन है. इस के लिए जहरीला आहार बनाना पड़ता है.
आहार बनाने के लिए 48 भाग चारा जैसे गुड़, चना, चावल, डबलरोटी वगैरह में एक भाग जिंक फास्फाइड नाम की दवा व एक भाग सरसों का तेल लकड़ी के टुकड़े की मदद से मिला कर 10-15 ग्राम हरेक बिल में रखने से चूहे इन को खा कर मर जाते हैं.
वारफेरिन द्वारा : यह रसायन स्टारफेरिन या रेटाफेरिन नाम से आता है. इस की 25 ग्राम मात्रा और 450 ग्राम टूटा हुआ अनाज व 15 ग्राम चीनी और 10 ग्राम खाने वाला तेल इन सब को अच्छी तरह लकड़ी से मिला कर मिट्टी के बरतन में चूहों के बिल के पास रखने से चूहे खा कर बाद में मर जाते हैं.
घरेलू उपाय : गुड़ की चाशनी बना लीजिए. कौटन यानी रुई के छोटेछोटे टुकड़ों को चाशनी में इस तरह डुबोएं कि पूरी तरह से रुई में गुड़ सोख जाए. हवा के सहारे चाशनी में डूबी हुई रुई को सुखा लीजिए. सूखने के बाद जहांजहां चूहों से प्रभावित जगह हों, वहांवहां इन टुकड़ों को रख दीजिए. चूहे इसे खाएंगे, गुड़ तो पच जाएगा, मगर रुई नहीं पचा पाएगा. इस से चूहों को बारबार प्यास लगेगी और पानी न मिलने पर चूहे दम तोड़ देंगे.
हालांकि इस का असर बहुत धीरेधीरे होता है, मगर लंबे समय तक सब्र रख कर इस को किया जाए तो फायदा जरूर मिलता है.












 हरिद्वार के प्रगतिशील किसान और मशरूमपालक मनमोहन ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के दौरान बताया कि साल 2017 में उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ ले कर मशरूम उत्पादन शुरू किया था और लोगों को रोजगार भी दिया था. साथ ही, उन की खुद की आमदनी भी कई गुना बढ़ गई थी. बीते 4-5 सालों में उन्होंने मशरूम उत्पादन में 12 से 15 करोड़ रुपए का कारोबार किया. आज पूरे उत्तराखंड में वे मशरूम सप्लाई करते हैं और डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड्स भी उन से व्यापार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन के फार्म का नाम भी ‘मामाभांजा फार्म’ है.
हरिद्वार के प्रगतिशील किसान और मशरूमपालक मनमोहन ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के दौरान बताया कि साल 2017 में उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ ले कर मशरूम उत्पादन शुरू किया था और लोगों को रोजगार भी दिया था. साथ ही, उन की खुद की आमदनी भी कई गुना बढ़ गई थी. बीते 4-5 सालों में उन्होंने मशरूम उत्पादन में 12 से 15 करोड़ रुपए का कारोबार किया. आज पूरे उत्तराखंड में वे मशरूम सप्लाई करते हैं और डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड्स भी उन से व्यापार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन के फार्म का नाम भी ‘मामाभांजा फार्म’ है.