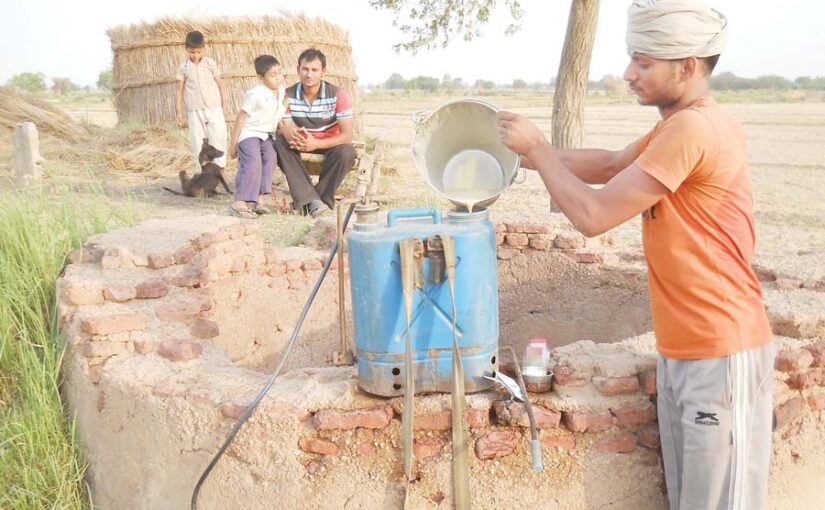हरी खाद की ये फसलें दलहनी व अदलहनी दोनों तरह की होती हैं पर ज्यादातर दलहनी फसलों को शामिल करते हैं क्योंकि इन फसलों में नाइट्रोजन बनाए रखने की कूवत होती है. खेती में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिस की खेती मुख्यत: जमीन में पोषक तत्त्वों को बढ़ाने और जैविक पदार्थों की भरपाई करने के मकसद से की जाती है.
अकसर इस तरह की फसल में ही हल चला कर मिट्टी में मिला दिया जाता है जो सड़गल कर जमीन की उपजाऊ कूवत को बढ़ाती है और लाभदायक जीवों की तादाद में इजाफा कर जमीन के उपजाऊपन को बनाए रखती है.
मुख्य खरीफ और रबी में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों की बोआई या रोपाई के पहले विभिन्न हरी खाद की फसलों को बो कर इन को हरी अवस्था में ही मिट्टी पलटने वाले हल से चला कर मिट्टी में मिला कर हरी खाद दी जाती है.
कुछ इलाकों में अदलहनीय फसलों का इस्तेमाल स्थानीय उपलब्धता, सूखा सहन करने की कूवत, तेजी से बढ़ोतरी व प्रतिकूल हालात में भी अनुकूलन के चलते किया जाता है. इन फसलों का ब्योरा इस तरह है:
हरी खाद में इस्तेमाल होने वाली फसलों के गुण
* दलहनी फसल हो, जो कम समय में ज्यादा नाइट्रोजन जमीन को दे सके.
* फसल में पानी की मांग कम हो ताकि कम सिंचाई की सुविधा वाले इलाकों में आसानी से उगाई जा सके.
* गहरी जड़ वाली फसल हो जो गहराई से पोषक तत्त्वों को हासिल कर सके और निचली सतहों को मुलायम बना सके.
* जल्दी उगने व तेजी से बढ़ने वाली फसलें सही होती हैं.
* काष्ठवत पौधे न हों, जिस से जल्दी सड़ाव हो सके.
* कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो.
* परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये बाद वाली फसल को किसी तरह से खराब न करे.
* इन फसलों को ज्यादा क्रियाओं की जरूरत न हो जैसे खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्त्व प्रबंधन, खेत की तैयारी, सिंचाई वगैरह.
हरी खाद के फायदे
* इस से जमीन को जीवांश पदार्थ भरपूर मिलता है, जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ा कर जमीन की भौतिक व रासायनिक दशा को सुधारता है.
* हरी खाद डालने से जमीन की निचली सतहों से अवशोषित हो कर पोषक तत्त्व जमीन की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं. इस से उथली जड़ वाली फसलें भी ली जा सकती हैं.
* यह खादपानी के बहाव को रोक कर जमीन में पानी सोखती है. साथ ही, जमीन के कटाव को भी रोकती है. इस तरह यह पानी व मिट्टी संरक्षण में सहायक है. साथ ही, जमीन की संरचना को भी यह सुधारती है और क्षारीय और लवणीय जमीन का सुधार करती है.
* हरी खाद पोषक तत्त्वों को अपने अंदर रोकती है और धीरेधीरे पौधों को देती है व पोषक तत्त्वों का नुकसान भी नहीं होने पाता है.
* दलहनी पौधों की जड़ों में वातावरण की स्वतंत्रता नाइट्रोजन को बनाए रखने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो आबोहवा से नाइट्रोजन को बनाए रख कर इस की उपलब्धता बढ़ाते हैं.
* यह फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैगनीशियम, आयरन वगैरह की उपलब्धता को बढ़ाती है.
* यह खरपतवार नियंत्रण में भी मददगार है.
* यह रासायनिक उर्वरकों की घुलनशीलता बढ़ाती है जिस से उर्वरक पौधों को आसानी से मुहैया हो जाते हैं.
हरी खाद वाली फसलों की सस्य क्रियाएं : वैसे तो इन फसलों को ज्यादा सस्य क्रियाओं की जरूरत नहीं होती है, पर ज्यादा जीवांश पदार्थ हासिल करने के लिए सस्य क्रियाएं जरूर करनी चाहिए.
बोआई का समय : इन की बोआई पानी की उपलब्धता व मुख्य फसल की बोआई पर निर्भर करती है. बारिश पर आधारित इलाकों में खरीफ में मानसून शुरू होते ही बोआई कर देनी चाहिए जबकि सिंचाई वाले इलाकों में इस की बोआई अप्रैलमई माह तक कर देनी चाहिए.
जमीन की तैयारी : जमीन की 1 व 2 जुताई कर बोआई करनी चाहिए.
फास्फोरस का इस्तेमाल : अगर जमीन में फास्फोरस कम हो तो फास्फोरस उर्वरक देना चाहिए ताकि ज्यादा जड़ ग्रंथियां बनें और नाइट्रोजन बना रह सके.
बोआई की विधि : छिड़काव विधि से बीज को बराबर बिखेर कर ढकना चाहिए.
बीज दर : मुख्य फसल की तुलना में बीज दर अधिक रखनी चाहिए. जैसे सनई 30 किलोग्राम, ग्वार 25 किलोग्राम, ढैंचा 35 किलोग्राम, लोबिया 125 किलोग्राम, उड़द व मूंग 30-35 किलोग्राम वगैरह.
सिंचाई : गरमी व सर्दी के दिनों में क्रमश: 10 और 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए.
जमीन में मिलाने की सही अवस्था : फसल की एक विशेष अवस्था पर पलटाई करने से जमीन को सब से ज्यादा नाइट्रोजन व जीवांश पदार्थ हासिल होते हैं.
इस अवस्था के पहले या बाद में पलटाई करना फायदेमंद नहीं होता है. जब फसल में 50 फीसदी फूल आ गए हों तो मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में दबा देना चाहिए. दबाने से पहले पाटा चला कर पौधों को गिरा देना चाहिए.
सनई की फसल में तकरीबन 50 दिन बाद व ढैंचा में 40 दिन बाद यह अवस्था आती है. बरसीम वगैरह की फसलों में 2-3 कटाई लेने के बाद फसल को खेत में दबा सकते हैं.
आगामी फसल की बोआई का अंतराल : खरीफ में धान की रोपाई तो दबाने के तुरंत बाद की जा सकती है, पर रबी फसलों जैसे गेहूं, गन्ना, आलू, सब्जियां वगैरह को हरी खाद देने के 30-35 दिन बाद बोना चाहिए.
पलटने की विधि और गहराई : खड़ी फसल को पहले पाटा चला कर खेत में गिरा देते हैं यानी मिट्टी पलटने वाले हल से इसे खेत में दबा देते हैं. फसल को खेत में दबाने की गहराई कई वजहों से प्रभावित होती है.
जमीन का प्रकार : बलुई जमीनों में गहराई और चिकनी जमीनों में ऊपरी सतह पर फसल का फुटाव जल्दी होता है, क्योंकि इन सतहों में नमी और हवा का बहना विच्छेदन की क्रियाओं के लिए सही होता है.
फसल की अवस्था : अपरिपक्व यानी अधपकी फसल किसी भी गहराई पर सड़ सकती है, पर परिपक्व यानी पकी हुई फसल कम गहराई पर ही दबानी चाहिए. जिन फसलों की शाखाएं व पत्तियां सख्त हों, उन्हें ऊपर की सतह में ही दबाना चाहिए.
मौसम : शुष्क मौसम में निचली सतह पर और नम मौसम में फसल को ऊपरी सतह पर ही दबाना चाहिए. फसल को खेत में दबा कर पाटा चलाना जरूरी है जिस से मिट्टी में अच्छी तरह से फसल दब जाए और फसल का सड़ना ठीक तरह से हो.
पूर्व सड़ाव के लिए अगर मिट्टी में नमी की कमी है तो खेत की सिंचाई करना जरूरी है. हरी खाद की पलटाई और आगामी फसल बोने के बीच के समय का अंतर भी खेत में करना चाहिए. मिट्टी में दबाने के 30-40 दिन के अंदर ही पूरी तरह सड़ाव हो पाता है.
हरी खाद देने की विधि : यह जरूरी है कि हरी खाद डालने की तकनीक की सही जानकारी हो क्योंकि इस के ऊपर ही हरी खाद की सफलता निर्भर करती है.
हरी खाद वाली फसलों की बोआई का समय इस तरह निश्चित करना चाहिए कि मिट्टी में उन पौधों को उस समय दबाया जा सके, जब ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्त्व खेत में मौजूद हों.
पौधों के दबाने और अगली फसल के बोने के बीच इतना अंतर होना चाहिए कि हरी खाद
द्वारा मिले पोषक तत्त्व अगली फसल के लिए मिट्टी किस प्रकार की अवस्था में सब से
ज्यादा सही रहती है, इस का भी सही अंदाजा रहना चाहिए.
हरी खाद की सीमाएं : हमारे देश में हरी खाद के चलन में कुछ बाधाएं हैं. इस की वजह से हरी खाद की फसलें उगाना किसानों के लिए आसान नहीं है जैसे: कम बारिश वाले इलाकों में हरी खाद की फसल इस वजह से नहीं उगाते क्योंकि मिट्टी में नमी के चलते हरी खाद खेत में दबाने से वे अच्छी तरह सड़ती नहीं है. साथ ही, दगली बोई जाने वाली फसल के बीजों का अंकुरण यानी फुटाव भी नमी की कमी में नहीं हो पाता.
जिन इलाकों में मिट्टी में नमी की कमी नहीं हो पाती है यानी सिंचित या ज्यादा बारिश वाले इलाकों में, जिस मौसम में हरी खाद की फसल उगाते हैं, उस मौसम में किसान की दूसरी जरूरत की कोई फसल नहीं ली जा सकती. इसलिए हरी खाद की फसल की अपेक्षा किसान दूसरी फसल लेना ज्यादा पसंद करता है.
किसान को हरी खाद को खेत में दबाने के यंत्र भी मुहैया नहीं हैं और ज्यादातर किसान हरी खाद को मिट्टी में दबाने की तकनीक से वाकिफ नहीं हैं.
विशेष रूप से खरीफ मौसम में फसल की सही बढ़वार के लिए बारिश न होने पर सिंचाई का भी सही इंतजाम नहीं हो पाता.
तमाम तरह की मिट्टियों, खासतौर से विकारग्रस्त यानी लवणीय, क्षारीय, जलमगन यानी पानी में डूबी हुई, पथरीली वगैरह के लिए सही हरी खाद की फसल का मिलना मुश्किल होता है.














 कार्यशाला के चीफ पैटर्न व हकृवि के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि क्षेत्र की अह्म भूमिका रहेगी. कृषि हमेशा से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है. यह लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है और हमारी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है. हाल ही के वर्षों में, इस क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो इस क्षेत्र को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे संकल्प को मजबूत करने में मदद करेगी.
कार्यशाला के चीफ पैटर्न व हकृवि के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि क्षेत्र की अह्म भूमिका रहेगी. कृषि हमेशा से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है. यह लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है और हमारी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है. हाल ही के वर्षों में, इस क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो इस क्षेत्र को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे संकल्प को मजबूत करने में मदद करेगी.