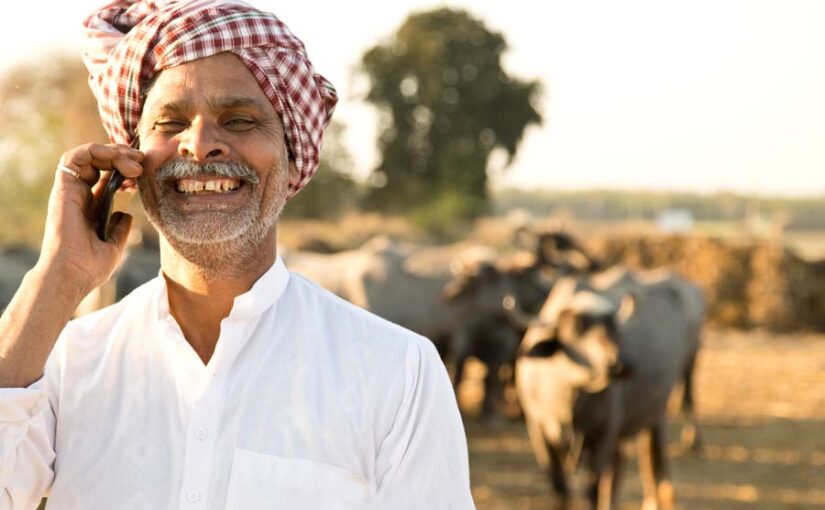दमोह: ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग किसान ही हैं, हम पशुपालन इसलिए करते हैं कि घर में दूध हो जाएगा, घी बन जाएगा. यदि हम पशुपालन को व्यापारिक दृष्टि से करने लगें, तो निश्चित रूप से यह आय बढ़ाने का काम तो करेगा.
इस विभाग के माध्यम से प्रदेश का नक्शा बदला जा सकता है. यहां काम की काफी संभावनाएं हैं. मार्गों पर गौवंश बड़ी समस्या है, सरकार इस दिशा में काम कर रही है, जल्द ही इस के परिणाम दिखेंगे.
यह विचार मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने पथरिया विकासखंड के ग्राम बोतराई में आयोजित पशु जागृति अभियान के तहत पशु बांझपन शिविर एवं जागरूकता गोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यक्त किया.
इस अवसर पर नानाजी देशमुख वेटनरी विज्ञान यूनिवर्सिटी, जबलपुर के कुलपति प्रो. डा. सीता प्रसाद तिवारी, अधिष्ठाता डा. राजेश कुमार शर्मा, निदेशक विस्तार शिक्षा डा. सुनील नायक, जनपद अध्यक्ष खिलान अहिरवार खासतौर पर मौजूद थे.
पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटेल ने कहा कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिस में गौवंश आदि की हेल्थ, उन को दिए जाने वाली दवाई और सरकार की जोजो भी योजना है, के बारे में किसानों और पशुपालकों को अवगत कराया है.
राज्यमंत्री लखन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय की सभी टीम ने आ कर मेरे क्षेत्र के गांव को चुना, उस के लिए उन का धन्यवाद करता हूं. इस कैंप से लोगों में जागरूकता तो आएगी, साथ ही यहां का प्रचारप्रसार होगा, तो दूसरे गांव के लोग भी यहां पर शामिल होंगे.
उन्होंने कहा कि मैं ने बड़े स्तर पर कोई एक ऐसे मेले का आयोजन करने को कहा था, जिस में पूरे जिले के लोग तो शामिल होंगे ही, साथ में संभाग और प्रदेश के लोग भी यहां आएं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री का सपना है, उस को पूरा कर सकें और उन को भी आयोजन में बुला सकें.
पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटेल ने कहा कि गौवंश-पशुपालन से किसानों की आमदनी दोगुनी करने का काम किया जा सकता है. हमारे पास दूध तो है, लेकिन उस की खपत नहीं है तो दूध का बहुत ज्यादा स्टाक हो जाता है, अमूल के साथ टाईअप कर के इस काम को आगे बढ़ने का काम करेंगे.
उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैं ने दिल्ली में पशुपालन और डेयरी के मंत्री परशोत्तम रूपाला से मिल कर अपनी समस्या के बारे में आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि आप बड़ेबड़े गौ अभ्यारण बनाइए, बाउंड्री बनाने के लिए, शेड बनाने के लिए, पानी के लिए जिस का पूरा पैसा हम देंगे.
उन्होंने बताया कि एक हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति ने कहा कि हम आप के साथ काम करना चाहते हैं, हम सांची डेयरी है, उस के साथ टाईअप करना चाहते हैं, इस में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है. हम इनवेस्ट करेंगे और सांची के साथ कोलैबोरेट कर के ईको वर्ल्ड वाईज बनाएं. वे कुछ दिन बाद यहां आ कर एग्रीमेंट करने वाले हैं.
पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटेल ने कहा कि हमारी सब से बड़ी समस्या है सड़कों पर जो गौवंश घूम रही है, इस संबंध में मंत्री परशोत्तम रूपाला से चर्चा हुई, जिस की योजना बना कर 5 से 10 गांव में एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगा कर उन्हें गैस दी जा सके. इस के लिए योजना तैयार की गई है, इस में समय लगेगा, क्योंकि यह बड़ा काम है, जब गाय का गोबर आप के घर से बिकने लगेगा, तो आप गौवंश को कहीं बेसहारा नहीं छोड़ेंगे.
मैं उसी दिन से यह सपना देख रहा हूं कि जिस दिन से यह तीनों चीजें हो गई, तो आप यह मान कर चलिए कि मध्य प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सब से ऊपर हो जाएगा.
नानाजी देशमुख वेटनरी विज्ञान यूनीर्वसिटी, जबलपुर के कुलपति डा. सीता प्रसाद तिवारी ने कहा कि कृषि से संबंधित जो बृहद नालेज आप सभी के पास है. हम पशुपालन के क्षेत्र को गांवगांव तक ले जाएं, पशुपालन के माध्यम से जो किसान आत्मनिर्भर हो और अपनी आमदनी को बढ़ाने के सुझाव दिए.
उन्होंने कहा कि गौशाला में हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, और हम गौशाला में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं और जो पैसा हमारे पास आएगा, उस पैसे को हम गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगाएंगे. इस की विविध जानकारी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जबलपुर देता है.
उन्होंने कहा कि क्लिनिकल कैंप के माध्यम से यहां के बीमार पशुओं का इलाज भी कराया जाएगा. हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय से जो डाक्टर है, वह एक या दो महीने में कम से कम एक बार यहां पर सेवाएं दें. बोतराई गांव में आगे चल कर जो भी पशुपालन एवं पशु चिकित्सा से संबंधित जो भी एक्टिविटी है, इस का एक केंद्र बने. हमें रोजगार भी निर्मित करना है और हमारे यहां के जो लोग हैं, काफी दूर तक पढ़ाई करने जाते हैं, 12वीं के बाद एक डिप्लोमा का कार्यक्रम, पशु चिकित्सा महाविद्यालय चलाता है.
वेटनरी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डा. राजेश शर्मा ने कहा कि दवाएं वितरण कर रहे हैं, जिस में कैल्शियम मिनरल मिक्सचर और फिर संगोष्ठी भी साथ में, जो हमारे युवा वर्ग है जो हमेशा रोजगार के लिए परेशान रहते हैं, पशुपालन से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि आय को दोगुना करना है.
कृषि और पशुपालन जब साथसाथ दोनों व्यवसाय किए जाएंगे, तब आय निश्चित रूप से दोगुनी हो सकती है. तो हम पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सभी हमारे शिक्षक, जो आए हैं पीजी, पीएचडी के स्टूडेंट भी साथ में आए हुए हैं, वे दिनभर गांव के जो भी पशुओं की समस्या है, उन का निराकरण करेंगे और जितना संभव हो सकेगा, इतना उपचार देंगे.
इस के पूर्व उन्होंने गौपालकों को दवाई की किट भी वितरित की. नानाजी देशमुख वेटनरी विज्ञान यूनिर्वसिटी, जबलपुर से आए पीजी, पीएचडी के स्टूडेंट से पशुओं का इलाज किया.
कार्यक्रम में खरगराम पटेल, लाखन प्रजापति, बद्री पटेल, बलराम पटेल, राजेश कुर्मी, रणवीर, अन्य जनप्रतिनिधि, उपसंचालक पशु चिकित्सा डा. एडब्ल्यू खान सहित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे.