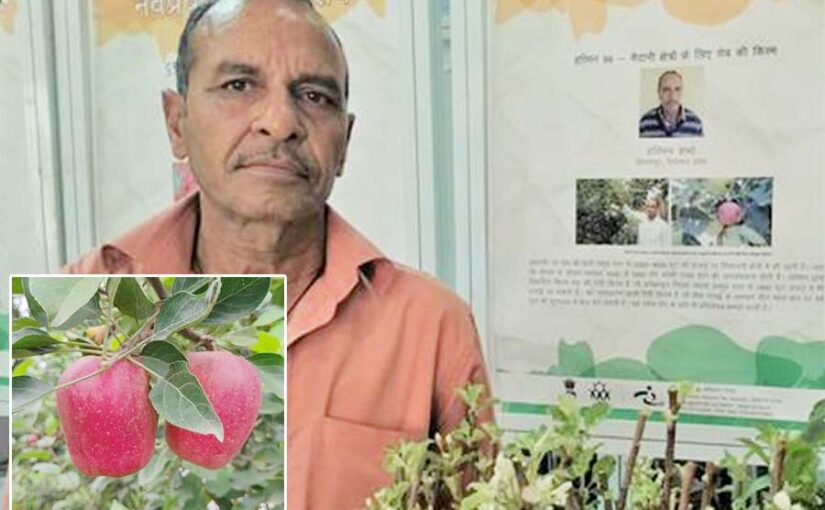मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के स्थायी और जिम्मेदार विकास और मछुआरों के कल्याण के माध्यम से नीली क्रांति (ब्लू रेवोल्यूशन) लाने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से एक प्रमुख योजना ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है.
इस योजना में मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियों की परिकल्पना की गई है, जिस में विभाग ने पीएमएमएसवाई योजना के तहत वेस्सल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नैशनल रोलआउट प्लान को मंजूरी दी है, जिस में 364 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,00,000 फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडर की स्थापना शामिल है.
नाव मालिकों को ट्रांसपोंडर के लिए मुफ्त में सहायता प्रदान की जाती है, जिस में टू वे कम्यूनिकेशन की सुविधा उपलब्ध है और संपूर्ण एक्सक्लूसिव इकोनोमिक जोन को कवर करते हुए किसी भी आपात स्थिति के दौरान छोटे टेक्स्ट मैसेज भेजे जा सकते हैं. यह मछुआरों को समुद्री सीमा के पास आने या उसे पार करने पर अलर्ट भी करता है.
इस के अलावा अन्य गतिविधियों जैसे समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड कोस्टल फिशिंग, गांवों का विकास, जिस का उद्देश्य स्थायी मत्स्य प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय नुकसान को कम करते हुए तटीय मछुआरों को आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करना है.
18 से 70 साल की आयु समूह में आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता पर 5 लाख रुपए, आकस्मिक स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता पर 2.50 लाख रुपए और दुर्घटनावश अस्पताल में भरती होने पर 25,000 रुपए का बीमा लाभ प्रदान करना, 18 से 60 साल की आयु समूह के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता देना, जिस में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान 3 महीनों के लिए प्रति मछुआरे को 3,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिस में लाभार्थी का योगदान 1,500 रुपए होता है और इस के लिए सामान्य राज्य के लिए अनुपात 50:50, उत्तरपूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:20, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सौ फीसदी है.
वर्तमान में चल रही पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों और मत्स्य किसानों को माली रूप से सशक्त बनाने और उन की बारगैनिंग पावर बढ़ाने के लिए मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों/फिश फार्मर प्रोड्यूसर और्गेनाइजेशन (एफएफपीओ) की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जो मछुआरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है.
मत्स्यपालन विभाग ने अब तक 544.85 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागतपर कुल 2,195 एफएफपीओ की स्थापना के लिए मंजूरी दी है, जिस में 2,000 मत्स्य सहकारिताओं को एफएफपीओ का रूप देने और 195 नए एफएफपीओ गठित करना शामिल है.
इस के अलावा, मछुआरों और मत्स्यपालकों द्वारा संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए साल 2018-19 से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को मात्स्यिकी क्षेत्र तक विस्तारित किया गया है और आज तक मछुआरों और मत्स्यपालकों को 4,50,799 केसीसी कार्ड दिए गए हैं.