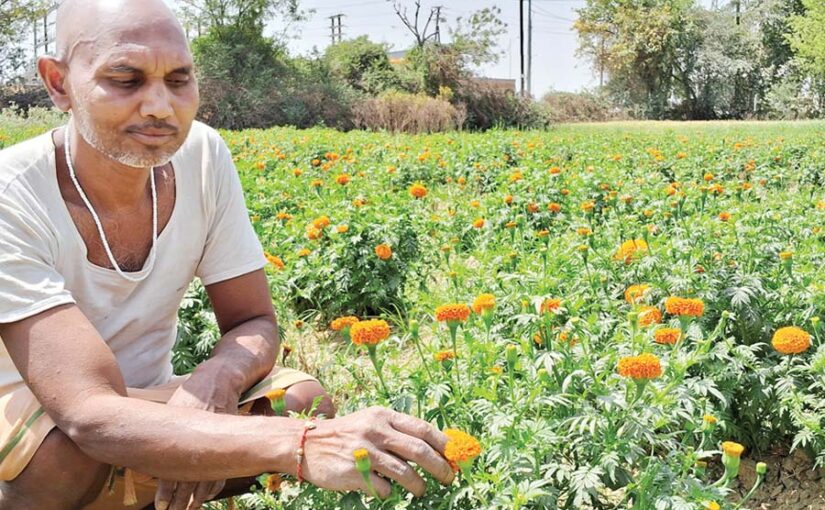Vermi Compost : खेती में अंगरेजी खाद के साथ ही जहरीली दवाओं, रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से पैदावार तो बढ़ी, लेकिन इन का असर हवा, पानी, मिट्टी समेत पूरे माहौल पर पड़ा है. इन्हें जल्दीजल्दी और ज्यादा मात्रा में डालने से उपज का स्वाद, गुण, इनसानी सेहत व समूची खाद्य श्रंखला गड़बड़ा गई है. धरती थकहार कर जहरीली व बंजर बन गई है. अंगरेजी खाद व दवाएं अब अपना असर खोने लगी हैं, इसलिए दुनियाभर के वैज्ञानिक अब नए रास्ते निकालने में लगे हुए हैं.
अंगरेजी खाद व कैमिकल्स से तोबा कर के अब देशी कंपोस्ट खाद को तरजीह दी जा रही है. कंपोस्ट से उगाए गए और्गैनिक फल, सब्जी, दालों व अनाज आदि की मांग, जागरूकता व बाजार कीमत लगातार बढ़ रही है.
जाहिर है कि यह सिलसिला आगे और तेजी से बढ़ेगा. ऐसे में वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) बना कर बेचना कमाई का चोखा धंधा है.
कंपोस्ट खाद की मांग गांव के खेतों में ही नहीं, बल्कि कसबों और शहरों की नर्सरियों व कालोनियों में भी तेजी से बढ़ रही है. दरअसल, बहुत से लोग अंगरेजी खाद के असर से बचने के लिए अपने गमलों, किचन गार्डन आदि में अब कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं. सेहत के लिए जागरूक हो रहे लोग अब घर की छतों पर भी जैविक खाद से फल, फूल व सब्जियां आदि उगाने लगे हैं.
उत्तर भारत के मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव व दिल्ली में भी आंगन, दीवारों व छतों पर हरियाली रखने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन इस मामले में बैंगलुरु पूरे देश में पहले स्थान पर है. वहां के बहुत से लोग कंपोस्ट की मदद से छतों पर और्गैनिक सब्जियां उगा कर दूसरे देशों को निर्यात कर के अच्छीखासी कमाई कर रहे हैं. वे अपनी उपज की क्वालिटी सुधारने के लिए वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) का इस्तेमाल करते हैं.

क्या है वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost)
घास, पत्ती, मिट्टी व गोबर के ढेर में कुछ केंचुए छोड़े जाते हैं. वे उसे खा कर अपना जो मल निकालते हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) कहते हैं. इस में नाइट्रोजन, सल्फर व पोटाश आदि पोषक तत्त्व होने के कारण यह खाद जमीन की सेहत व खेतीबागबानी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है. साथ ही, इसे तैयार करने में बदबू भी नहीं आती. कचरे का निबटारा भी आसानी से हो जाता है.
कचरे से कंपोस्ट बनाने का चलन सदियों पुराना है, लेकिन पहले गंवई इलाकों में लोग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कूड़ेकचरे को गड्ढे में दबा कर छोड़ देते थे. बहुत से लोग अब भी यही करते हैं. इस तरह से कंपोस्ट तैयार होने में तकरीबन 2 साल का वक्त लगता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) 2-3 महीने में तैयार हो जाती है. 100 वर्गफुट जगह में 1 टन वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) बन जाती है, जो आधा हेक्टेयर जमीन में डालने के लिए काफी है.
इस काम की खासीयत यह है कि इसे घर के पिछवाड़े में छोटे पैमाने से ले कर बहुत बड़े पैमाने तक किया जा सकता है. वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) में बतौर कच्चे माल के तौर पर काम आने वाला कचरा खेती, बागबानी, होटलों, कालोनियों, पार्कों, केंचुए वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) बनाने वालों से व गोबर डेयरी व गौशालाओं आदि से मिल जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार आइसेनियाफेटिडा किस्म के लाल केंचुए कंपोस्ट के लिए सब से बढि़या हैं, क्योंकि ये हर मौसम को आराम से सह लेते हैं.
1-2 किलोग्राम के पैकेट पौलीथिन की पन्नी में व बड़े 5,10 व 20 किलोग्राम को बैग या बोरे में पैक करें. अपने नाम, पते, ब्रांड और वजन आदि का लेबल लगा कर सप्लाई करें. बिक्री से पहले नियमकायदों की जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि अधिकारी से सलाह ले सकते हैं.

वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) ऐसे बनाएं
वर्तमान में कूड़ाकचरा जलाने से अच्छा है उसे वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) बनाना व उस से पैसे कमाना. इस के लिए समतल जगह पर रेत, मिट्टी की 6 इंची तह लगाएं. कचरे से कांच, धातु व पत्थर आदि निकाल कर अलग कर दें. घास, पत्ती, फल, सब्जियों आदि के गीले कचरे पर गोबर की तह लगा कर केंचुए छोड़ें. उन के ऊपर फिर गोबर व हरा कचरा डाल कर ढेर को पुआल, टाट या गन्ने की सूखी पत्तियों से ढक दें, ताकि सीधी व तेज धूप से नुकसान न हो.
इस के बाद रोज हजारे या स्प्रेयर से हलका पानी डालते रहें, ताकि थोड़ी नमी बनी रहे. हफ्ते में एक बार सावधानी से ढेर को पलट कर ऊपरनीचे कर दें. एक माह बाद केंचुए बढ़ने पर कचरे की और भी तह लगा सकते हैं. गोबर व हरे कचरे की मात्रा तकरीबन आधी आधी रख सकते हैं. साथ ही नमी भी 50 फीसदी से ज्यादा न हो.
वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) खाद को उलटतेपलटते रहें और अंत में छानते वक्त सावधानी बरतें ताकि केंचुओं का नुकसान न हो. डेढ़ माह बाद पानी छिड़कना बंद कर दें. अब आप देखेंगे कि धीरेधीरे कचरा बदल कर हलकी, भुरभुरी व कत्थई रंग की वर्मी कंपोस्ट (Vermi Compost) में बदलने लगी है.