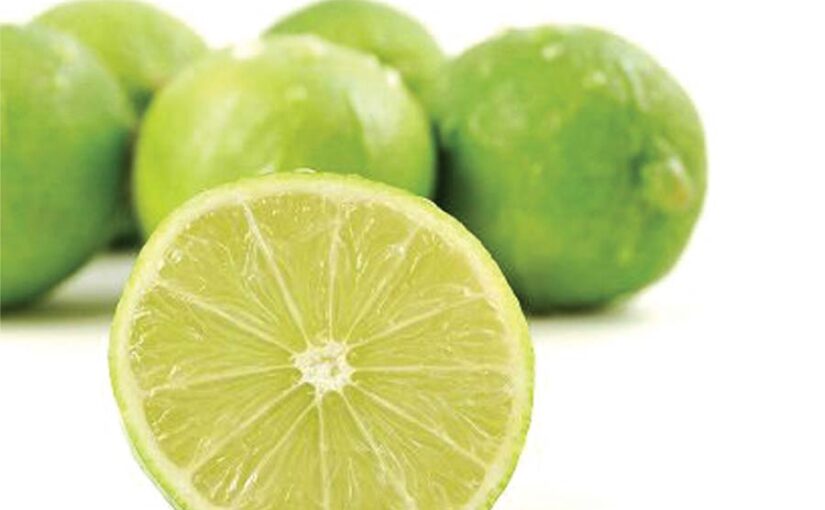हाल ही में देखा गया है कि पिछले एक दशक में देश में फलों व सब्जियां की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो कि कृषि क्षेत्र में आई प्रगति को तो दर्शाता ही है, साथ ही यह खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिहाज से भी एक बड़ी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है.
पिछले 10 सालों में समूचे देश में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमश: 7 और 12 किलोग्राम बढ़ी है. प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ने का श्रेय मुख्य रूप से तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मूकश्मीर को मिलना चाहिए, जिन के योगदान से ही आज देश प्रति व्यक्ति हर साल 227 किलोग्राम फल व सब्जियों का उत्पादन कर रहा है, जो प्रति व्यक्ति 146 किलोग्राम की अनुशंसित खपत से कहीं ज्यादा है.
दरअसल, आज का भारत परंपरागत खेती से आगे बढ़ कर नवाचार और तकनीकी उपायों को अपनाने में सफल हो रहा है. किसानों द्वारा ड्रिप सिंचाई उच्च उपज वाली फसलों को प्राथमिकता देना और स्मार्ट खेती जैसे वीडियो को अपनाना इस के मुख्य कारण हैं.
इस के अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि अवसरंचना कोष और किसान उत्पादक संगठन जैसी पहलों ने किसानों को बेहतर संसाधन तो दिए ही हैं, साथ ही, उन की बाजारों तक पहुंच भी सुनिश्चित की है.
लोगों में स्वास्थ्य एवं पोषण को ले कर बढ़ती जागरूकता ने भी फलों एवं सब्जियों की मांग को प्रोत्साहित किया है. लोगों के आहार पैटर्न में यह जो बदलाव दिखाई दे रहा है, वह कोरोना महामारी के दौर से ही दिखना शुरू हो गया था.
हालांकि, आसमान में होती मौसम की स्थितियों में होने वाले नुकसानों पर भी भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाश डाला है कि आजकल बाजार में हरी सब्जियों के साथसाथ बैंगनी रंग की सब्जियों का चलन काफी बढ़ गया है. लोग इन सब्जियों को स्वास्थ्य के लिए काफी महत्त्वपूर्ण मानते हुए अधिक खरीद रहे हैं, साथ ही, किसानों को उस की कीमत भी अच्छी मिल रही है.
कई सब्जियों और फलों की प्रजातियां ऐसे विज्ञान द्वारा विकसित कर दी गई हैं, जिन का कलर बैंगनी हो गया है. चाहे टमाटर हो या पत्तागोभी, मूली, शलजम, गाजर, आलू, फूलगोभी, ब्रोकोली, केला, अंगूर आदि फल और सब्जियां हैं, जिन की लगातार बाजार में मांग बढ़ रही है.

रंगीन सब्जियों की पोषण सुरक्षा में भूमिका
रंगीन सब्जियां पोषण सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऔक्सिडैंट से भरपूर होती हैं. इन में मौजूद प्राकृतिक पिगमेंट जैसे कैरोटीनौइड, एंथोसायनिन और फ्लेवोनौइड़स न केवल सब्जियों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, बल्कि ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं.
गाजर, पालक, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियां कुपोषण से बचाने में मददगार हैं, क्योंकि ये विटामिन ए, सी, ई और के, के साथसाथ आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम की कमी को भी पूरा करती हैं.
इन सब्जियों में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है, जबकि बीटाकैरोटीन आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है. इस के अलावा हृदय और हड्डियों को मजबूत करने में भी इन का महत्त्वपूर्ण योगदान है. कम कैलोरी और उच्च पोषण मूल्य के कारण रंगीन सब्जियां संतुलित आहार और टिकाऊ पोषण सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा हैं.
बैंगनी कलर लोगों को करता है आकर्षित
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, अनाज के उत्पादन में तापमान में 3 डिगरी सैल्सियस से एक डिगरी भी ज्यादा होने पर गेहूं की पैदावार में 3 से 4 फीसदी की कमी आ सकती है, जो बेहद चिंताजनक है. लेकिन इस से भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 30 से 35 फीसदी फसल कटाई भंडारण, परिवहन और पैकेजिंग के गलत तौरतरीकों के चलते खराब हो जाती है.
देश के 7 फीसदी कोल्ड स्टोरेज केवल 4 राज्यों गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में है. भारत फिलहाल फल व सब्जियों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है. लेकिन बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर अब आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने का समय है. फलसब्जियों की उपलब्धता बढ़ाना सकारात्मक संकेत है, लेकिन खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है.
आखिर क्यों होता है इन का रंग बैंगनी
सब्जियों का बैंगनी रंग मुख्य रूप से उन के अंदर मौजूद एंथोसायनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है, जो एक प्रकार का फ्लेवोनौइड है. यह पिगमेंट सब्जी के परिपक्वता स्तर और उस के अंदर की अम्लीयता पर निर्भर करता है. जैसेजैसे सब्जी अपने विकास के अंतिम चरण में पहुंचती है, एंथोसायनिन पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जिस से उस का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है.
इस के अलावा बाहरी कारण जैसे प्रकाश, तापमान और पर्यावरणीय दबाव भी इस रंग को और गहरा बनाने में भूमिका निभाते हैं. बैंगनी रंग का विकास अकसर सब्जी के पकने और पोषक तत्त्वों के पूरे विकास का संकेत देता है. यह रंग न केवल सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि यह एंटीऔक्सिडैंट गुणों से भरपूर होता है, जो सब्जी को पोषण और स्वास्थ्य के नजरिए से और भी उपयोगी बनाता है.
रंगीन सब्जियों की खूबियां
रंगीन सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, पालक, ब्रोकोली, शिमला मिर्च, चुकंदर, बैंगन और अन्य अपने विशिष्ट रंगों के कारण विशेष पोषक तत्त्वों से भरपूर होती हैं. इन रंगों के पीछे मौजूद पिगमेंट्स जैसे कैरोटीनौइड, फ्लेवोनौइड्स और एंथोसायनिंस स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं.
लाल सब्जियां : टमाटर और चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थ लाइकोपीन और एंथोसायनिन से भरपूर होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक हैं.
हरी सब्जियां : पालक, ब्रोकोली और पत्तेदार सब्जियां आयरन, कैल्शियम और फाइबर का सब से बेहतर स्रोत हैं. ये हड्डियों को मजबूत करती हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखती हैं.
पीली और नारंगी सब्जियां : गाजर और कद्दू जैसे खाद्य पदार्थ विटामिन ए और बीटाकैरोटीन प्रदान करते हैं, जो आंखों की रोशनी और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं.
बैंगनी और नीली सब्जियां : बैंगन और अन्य गहरे रंग की सब्जियां एंटीऔक्सिडैंट से भरपूर होती हैं, जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करती हैं.