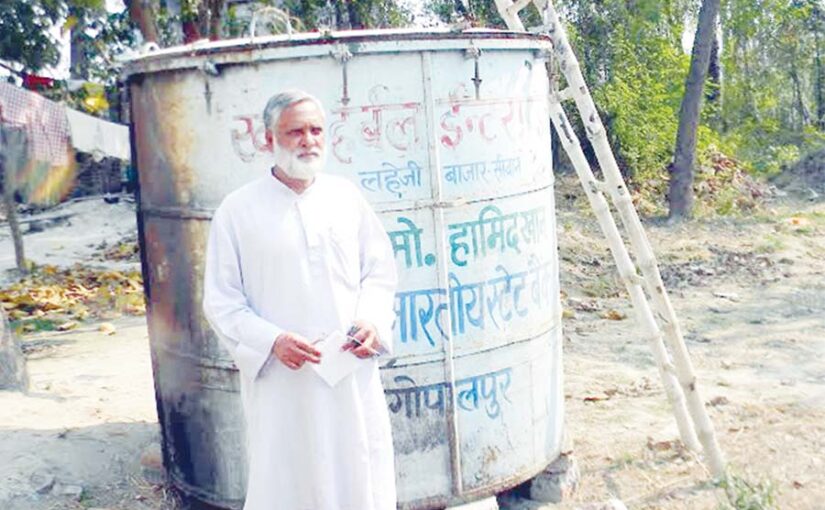Chilli Nursery| हर दिन इस्तेमाल की जाने वाली मिर्च की खेती बरसात में जुलाई से अक्तूबर तक, सर्दी में सितंबर से जनवरी तक और जायद मौसम में फरवरी से जून तक की जाती है. मिर्च को सुखा कर बेचने के लिए सर्दी के मौसम की मिर्च का इस्तेमाल होता है.
मिर्च की खासीयत यह है कि यदि पौध अवस्था में ही इस की देखभाल ठीक से कर ली जाए तो अच्छा उत्पादन मिलने में कोई शंका नहीं होती है. भरपूर सिंचाई समयानुसार करने से ज्यादा फायदा लिया जा सकता है. टपक सिंचाई अपनाने से मिर्च की फसल से दोगुनी उपज हासिल की जा सकती है. टपक सिंचाई से 50-60 फीसदी जल की बचत होती है और खरपतवार से नजात मिल जाती है.
मिर्च की नर्सरी ऐसे लगाएं
पौधशाला, रोपणी या नर्सरी एक ऐसी जगह है, जहां पर बीज या पौधे के अन्य भागों से नए पौधों को तैयार करने के लिए सही इंतजाम किया जाता है. पौधशाला का क्षेत्र सीमित होने के कारण देखभाल करना आसान व सस्ता होता है.
पौधशाला के लिए जगह का चुनाव
* पौधशाला के पास बहुत बड़े पेड़ न हों.
* जमीन उपजाऊ, दोमट, खरपतवार रहित व अच्छे जल निकास वाली हो, अम्लीय क्षारीय जमीन का चयन न करें.
* पौधशाला में लंबे समय तक धूप रहती हो.
* पौधशाला के पास सिंचाई की सुविधा मौजूद हो.
* चुना हुआ क्षेत्र ऊंचा हो ताकि पानी न ठहरे.
* एक फसल के पौध लगाने के बाद दूसरी बार पौध उगाने की जगह बदल दें यानी फसलचक्र अपनाएं.

क्यारियों की तैयारी व उपचार
पौधशाला की मिट्टी की एक बार गहरी जुताई करें या फिर फावड़े की मदद से खुदाई करें. खुदाई करने के बाद ढेले फोड़ कर गुड़ाई कर के मिट्टी को भुरभुरी बना लें और उगे हुए सभी खरपतवार निकाल दें. फिर सही आकार की क्यारियां बनाएं. इन क्यारियों में प्रति वर्गमीटर की दर से 2 किलोग्राम गोबर या कंपोस्ट की सड़ी खाद या फिर 500 ग्राम केंचुए की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाएं. यदि मिट्टी कुछ भारी हो तो प्रति वर्गमीटर 2 से 5 किलोग्राम रेत मिलाएं.
मिट्टी का उपचार
जमीन में विभिन्न प्रकार के कीडे़ और रोगों के फफूंद जीवाणु वगैरह पहले से रहते हैं, जो मुनासिब वातावरण पा कर क्रियाशील हो जाते हैं व आगे चल कर फसल को विभिन्न अवस्थाओं में नुकसान पहुंचाते हैं. लिहाजा नर्सरी की मिट्टी का उपचार करना जरूरी है.
सूर्यताप से उपचार
इस विधि में पौधशाला में क्यारी बना कर उस की जुताईगुड़ाई कर के हलकी सिंचाई कर दी जाती है, जिस से मिट्टी गीली हो जाए. अब इस मिट्टी को पारदर्शी 200-300 गेज मोटाई की पौलीथीन की चादर से ढक कर किनारों को मिट्टी या ईंट से दबा दें ताकि पौलीथीन के अंदर बाहरी हवा न पहुंचे और अंदर की हवा बाहर न निकल सके. ऐसा उपचार तकरीबन 4-5 हफ्ते तक करें. यह काम 15 अप्रैल से 15 जून तक किया जा सकता है. उपचार के बाद पौलीथीन शीट हटा कर खेत तैयार कर के बीज बोएं. सूर्यताप उपचार से भूमि जनित रोग कारक जैसे फफूंदी, निमेटोड, कीट व खरपतवार वगैरह की संख्या में भारी कमी हो जाती है.
रसायनों द्वारा जमीन उपचार
बोआई के 4-5 दिनों पहले क्यारी को फोरेट 10 जी 1 ग्राम या क्लोरोपायरीफास 5 मिलीलीटर पानी के हिसाब से या कार्बोफ्यूरान 5 ग्राम प्रति वर्गमीटर के हिसाब से जमीन में मिला कर उपचार करते हैं. कभीकभी फफूंदीनाशक दवा कैप्टान 2 ग्राम प्रति वर्गमीटर के हिसाब से मिला कर भी जमीन को सही किया जा सकता है.
जैविक विधि द्वारा उपचार
क्यारी की जमीन का जैविक विधि से उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरडी की 8 से 10 ग्राम मात्रा को 10 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला कर क्यारी में बिखेर देते हैं. इस के बाद सिंचाई कर देते हैं. जब खेत का जैविक विधि से उपचार करें, तब अन्य किसी रसायन का इस्तेमाल न करें.

बीज खरीदने में सावधानियां
* बीज अच्छी किस्म का शुद्ध व साफ हो, अंकुरण कूवत 80-85 फीसदी हो.
* बीज किसी प्रमाणित संस्था, शासकीय बीज विक्रय केंद्र, अनुसंधान केंद्र या विश्वसनीय विक्रेता से ही लेना चाहिए. बीज प्रमाणिकता का टैग लगा पैकेट खरीदें.
* बीज खरीदते समय पैकेट पर लिखी किस्म, उत्पादन वर्ष, अंकुरण फीसदी, बीज उपचार वगैरह जरूर देख लें ताकि पुराने बीजों से बचा जा सके. बीज बोते समय ही पैकेट खोलें.
बीज उपचार : बीज हमेशा उपचारित कर के ही बोने चाहिए ताकि बीज जनित फफूंद से फैलने वाले रोगों को काबू किया जा सके. बीज उपचार के लिए 1.5 ग्राम थाइरम, 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2.5 ग्राम डाइथेन एम 45 या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरडी का प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए. यदि क्यारी की जमीन का उपचार जैविक विधि (ट्राइकोडर्मा) से किया गया है, तो बीजोपचार भी ट्राइकोडर्मा विरडी से करें.
बीज बोने की विधि : क्यारियों में उस की चौड़ाई के समानांतर 7-10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर गहरी लाइनें बना लें और उन्हीं लाइनों पर करीब 1 सेंटीमीटर के अंतर से बीज बोएं. बीज बोने के बाद उसे कंपोस्ट, मिट्टी व रेत के 1:1:1 के 5-6 ग्राम थाइरम या केपटान से उपचारित मिश्रण से 0.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ढक देते हैं.
क्यारियों को पलवार से ढकना : बीज बोने के बाद क्यारी को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पुआल, सरकंडों, गन्ने के सूखे पत्तों या ज्वारमक्का के बने टटीयों से ढक देते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और सिंचाई करने पर पानी सीधे ढके हुए बीजों पर न पड़े, वरना मिश्रण बीज से हट जाएगा और बीज का अंकुरण प्रभावित होगा.
सिंचाई : क्यारियों में बीज बोने के बाद 5-6 दिनों तक हलकी सिंचाई करें ताकि बीज ज्यादा पानी से बैठ न जाएं. बरसात में क्यारी की नालियों में मौजूद ज्यादा पानी को पौधशाला से बाहर निकालना चाहिए. क्यारियों से पलवार घासफूल तब हटाएं जब तकरीबन 50 फीसदी बीजों का अंकुरण हो चुका हो. बोआई के बाद यह अवस्था मिर्च में 7-8 दिनों बाद, टमाटर में 6-7 दिनों बाद व बैगन में 5-6 दिनों बाद आती है.
खरपतवार नियंत्रण : क्यारियों में उपचार के बाद भी यदि खरपतवार उगते हैं, तो समयसमय पर उन्हें हाथ से निकालते रहना चाहिए. इस के लिए पतलीलंबी डंडियों की भी मदद ली जा सकती है. बेहतर रहेगा अगर यदि पेंडीमिथालिन की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल कर बोआई के 48 घंटे के भीतर क्यारियों में छिड़क दें.
पौध विरलन : यदि क्यारियों में पौधे अधिक घने उग आएं तो उन को 1-2 सेंटीमीटर की दूरी पर छोड़ते हुए अन्य पौधों को छोटी उम्र में ही उखाड़ देना चाहिए, वरना पौधों के तने पतले व कमजोर बने रहते हैं. घने पौधे पदगलन रोग लगने की संभावना बढ़ाते हैं. उखाड़े गए पौधे खाली जगह पर रोपे जा सकते हैं.
पौध सुरक्षा : पौधशाला में रस चूसने वाले कीट जैसे माहू, जैसिड, सफेद मक्खी व थ्रिप्स से काफी नुकसान पहुंचता है. विषाणु अन्य बीमारियों को फैलाते हैं, लिहाजा इन के नियंत्रण के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या डायमिथियेट (रोगोर) 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर बोआई के 8-10 दिनों और 25-27 दिनों बाद छिड़कना चाहिए. क्यारी और बीज उपचार करने के बाद भी यदि पदगलन बीमारी लगती है (जिस में पौधे जमीन की सतह से गल कर जमीन पर गिरने लगते हैं और सूख जाते हैं), तो फसल पर मैंकोजेब या कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें.
पौधे उखाड़ना : क्यारी में तैयार पौधे जब 25-30 दिनों के हो जाएं और उन की ऊंचाई 10-12 सेंटीमीटर की हो जाए और उन में 5-6 पत्तियां आ जाएं, तब उन्हें पौधशाला से खेत में रोपने के लिए निकालना चाहिए. पौध निकालने से पहले उन की हलकी सिंचाई कर देनी चाहिए. सावधानी से पौधे निकालने के बाद 50 या 100 पौधों के बंडल बना लें.
पौधों का रोपाई से पहले उपचार : पौधशाला से निकाले गए पौध समूह या रोपा की जड़ों को कार्बेंडाजिम बाविस्टीन 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में बने घोल में 10 मिनट तक डुबोना चाहिए, रोपाई के बाद सिंचाई जरूर करें.
गरमी के मौसम में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर और बरसात में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें.
मिर्च से अधिकतम उत्पादन हासिल करने के लिए उस की नर्सरी लगा कर पौधशाला में स्वस्थ पौधे तैयार करने का अपना अलग महत्त्व है. जितनी स्वस्थ नर्सरी रहेगी, उतनी ही अच्छी रोप मिलेगी.