वर्ष 2022 की विदाई और 2023 का आगमन. नए वर्ष के स्वागत की औपचारिकताओं के बीच यह कलैंडर वर्ष भी हर साल की तरह एक बार फिर अपनी केंचुली बदल लेगा. लेकिन इस कलैंडर वर्ष में देश की आबादी के सब से बड़े हिस्से के किसानों ने क्या खोया और पाया क्या, इस पर निष्पक्ष चिंतन जरूरी है.
कह सकते हैं कि वर्ष 2022 की शुरुआत किसानों के मोरचे पर अस्थाई युद्ध विराम से हुई. दरअसल, तीनों कृषि कानूनों को वापस करवा कर किसानों ने कुछ हद तक देश की खेतीकिसानी का भविष्य तो बचाया, पर उन के वर्तमान के दोनों हाथ आज भी बिलकुल खाली हैं.
देश के किसानों की आय में वृद्धि अथवा देश में अरबपतियों की बढ़ती संख्या दोनों में से देश की आर्थिक समृद्धि का वास्तविक सूचकांक आखिर आप किसे मानेंगे?
सिक्के का दूसरा पहलू भी जरा देखिए. भारत सरकार की ‘द सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे औफ फार्मर’ का कहना है कि पिछले सालों में भारत के किसान औसतन केवल 27 रुपए की रोज की कमाई कर पाए हैं.
कृषि मंत्रालय ने अन्नदाताओं की आय से संबंधित जो सब से ताजा आंकड़े जारी किए थे, उस के मुताबिक, भारत का किसान परिवार प्रतिदिन औसतन 264.94 रुपए यानी 265 रुपए कमाता है. यह एक व्यक्ति की आय नहीं है, बल्कि 5 सदस्यों के परिवार की औसत आय है.
हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में यहां यह बताना भी लाजिमी है कि प्राय: गरीबी, भुखमरी, बाढ़, अकाल और न्यूनतम आय के लिए जाना जाने वाला पड़ोसी बंगलादेश इस साल प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम से आगे निकल गया है, जबकि 15 साल पहले इसी बंगलादेश की प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय की महज आधी थी.
एक ओर देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर खेती और किसानों की जिंदगी दिनोंदिन कठिन होती जा रही है. हर कलैंडर वर्ष के साथ अमीरों और गरीबों के बीच की खाई चौड़ी हाती जा रही है.
दिनरात कुरसी हासिल करने और उसे बचाने के खेल में लगी सरकारें धीरेधीरे यह भूलती जा रही हैं कि देश का सब से महत्त्वपूर्ण तबका रहा है यह किसान, जिस के पसीने के दम पर यह देश पूरी दुनिया में सोने की चिडि़या कहलाता था. कुछेक साल पहले तक किसान और खेती के महत्त्व व उपादेयता को रेखांकित करती हुई अकबर के समकालीन कृषि पंडित महाकवि घाघ की एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ‘उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद चाकरी भीख निदान…’
मतलब साफ था कि समाज में अव्वल दर्जे पर अन्नदाता किसान और उस की खेती, फिर व्यापार और नौकरी आदि सामाजिक उपादेयता के क्रम में क्रमश: उस के बाद आते हैं. वैश्विक बाजारवाद की ताकतों ने खेतीकिसानी की इस 500 साल पुरानी कहावत के अर्थ और निहितार्थों को सीधेसीधे 180 डिगरी पर पलट दिया है.
आज 10 एकड़ के किसान का बेटा भी अपनी जमीन बेच कर मिले पैसे को रिश्वत में दे कर भी चपरासी की नौकरी करना चाहता है. जाहिर है कि अपने पिता की दुरावस्था को लगातार देखते हुए बड़ा हुआ बेटा किसी भी हालत में घाटे की खेती नहीं करना चाहता है.
भारत सरकार की ‘द सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे औफ फार्मर’ का कहना है कि वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के हर किसान ने हर दिन केवल 27 रुपए की कमाई की. वर्ष 2022 के अंतिम हफ्ते में भी हालात इस से कुछ बेहतर नहीं दिखते.
इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों का जीवन कितना कठिन हो गया है, और क्यों पिछले 2 दशकों में 4 लाख से ज्यादा किसान पूरी तरह से पस्त हो कर निराशा और मजबूरी में आत्महत्या का रास्ता चुन चुके हैं. इसे आत्महत्या कहना उचित नहीं है, बल्कि यह सरकार और बाजार की पक्षपाती नीतियों द्वारा की गई किसानों की हत्या है.
एक किसान आत्महत्या करने के पहले ही हजारों बार मर चुका होता है. इस निर्मम आखेट में फंस कर किसानों का इस तरह से जान देना इस सदी की सब से बड़ी त्रासदी है. ऐसा नहीं है कि इन वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां और योजनाएं नहीं बनाई गईं. ये योजनाएं देखने, पढ़ने, सुनने में भले ही आकर्षक लगती हैं, किंतु इन नीतियों की मूल डिजाइन ऐसी रही है कि किसानों की कमाई को जानबूझ कर कम रखा जाए. कमाई कम होगी, तो ये गांव छोड़ कर शहरों की तरफ प्रवास करेंगे. शहरों को, कारखानों को सस्ती कीमत पर मजदूर मिलेंगे. कारपोरेट्स दिनोंदिन मालमाल और किसान मजदूर बदहाल होंगे. अगर कमाई कम है, तो कर्ज के बोझ का बढ़ना भी स्वाभाविक है और बिलकुल ऐसा ही हुआ भी.
वर्ष 2012-13 में देश के हर किसान पर औसतन 47,000 रुपए के कर्ज का बोझ था. यह बढ़ कर वर्ष 2018-19 में तकरीबन 74,000 रुपए हो चुका है.
नए सरकारी आंकड़े आने अभी बाकी हैं. जिस तरह से हमारे देश के हर नागरिक पर कर्जा बढ़ रहा है. जाहिर है, अगर यही हाल रहा, तो हम देश के प्रति व्यक्ति के सिर पर एक लाख रुपए कर्ज के लक्ष्य तक वर्ष 2023 में अवश्य पहुंच जाएंगे.
बता दें कि सब से बुरा हाल किसानों का है. देश के 50 फीसदी किसान कर्ज के बोझ तले इतना दब चुके हैं कि उन के उबरने की अब कोई आशा नहीं दिखती. कर्ज में डूबे किसान की दयनीय दशा पर आज से 100 साल पहले वर्ष 1921 में मुंशी प्रेमचंद ने दिल को छू लेने वाली एक कालजयी कहानी लिखी थी, ‘पूस की रात’.
इस कहानी के नायक किसान हल्कू और उस की पत्नी मुन्नी के बीच का वार्त्तालाप है. मुन्नी अपने पति हल्कू से कहती है, ‘मैं कहती हूं, तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मरमर कर काम करो. पैदावार हो तो उस से कर्जा अदा करो. कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं. ऐसी खेती से बाज आए.’
देश का सच यही है कि आजादी के 75 साल बाद भी देश के बहुसंख्यक किसानों की दशा अभागे हल्कू, होरी से बेहतर नहीं है.
वर्ष 2023 में देश के किसान के लिए आशा की किरण आखिर कहां छिपी है? सब से पहले हम अपनी सरकार की ओर देख लेते हैं. इस जिद्दी सरकार ने किसान आंदोलन के दबाव में तीनों कृषि कानूनों को वापस तो ले लिया, पर इस से उस के अहं को बड़ी चोट पहुंची है, ऐसा दिखता है.
मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी किसान राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे तथाकथित कुछेक मौकापरस्त किसान नेताओं को साथ ले कर किसानों की समस्या को बूझने और उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, ऐसे में इन से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती.
भाजपा के अनुषंगी किसान संगठन, जो कि अपने दांत और नाखून पहले ही गिरवी रख चुके हैं, किसानों के नाम पर यदाकदा निरर्थक गर्जना करते घूम रहे हैं. इस नूराकुश्ती से भी कुछ खास हासिल नहीं है. उत्तर भारत और महाराष्ट्र के गन्ने की राजनीति से पैदा हुए किसान नेताओं के पास गन्ना किसानों का कुछ ठोस जनाधार तो है, पर आज भी वे गन्ने की राजनीति में ही उलझे हुए हैं. गन्ने से इतर समस्याओं की न तो इन्हें विशेष समझ है, न विशेष रुचि है और न ही इन के पास इन का कोई ठोस निदान है.
इधर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जैविक खेती, जीरो बजट खेती आदि कई लपूझन्ने जोड़ कर अपने जेबी तनखैया मेंबरान मनोनीत कर जैसेतैसे एक एमएसपी कमेटी का एक बेडौल बिजूका बना कर खड़ा कर दिया है, जिस से किसान का कोई भला होने की उम्मीद नहीं है.
एमएसपी पिछले कई दशकों से किसानों की सब से जरूरी मांग रही है. दरअसल, किसानों की कड़ी मेहनत से तैयार किए गए उत्पादों को केवल 4 से 6 फीसदी को ही घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाता है, बाकी 94 से 96 फीसदी किसानों का उत्पाद लागत से भी कम कीमत पर बिकता है अथवा लूटा जाता है. किसानों की बदहाली का यह एक प्रमुख कारण है.
इसी एकसूत्रीय मांग को ले कर वर्ष 2022 के अंतिम महीनों में देश के किसान संगठनों ने मिल कर सर्वसम्मति से देश के प्रत्येक किसान के लिए और प्रत्येक फसल के लिए ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी किसान मोरचा’ बनाया है. वरिष्ठ किसान नेता बीएम सिंह को इस का अध्यक्ष चुना गया है.
वर्ष 2023 में किसानों के लिए आशा की पहली किरण यहां दिखाई दे रही है. किंतु केवल मोरचा बनने से ही सबकुछ नहीं हो जाता. अब अपनी इस जरूरी मांग को हासिल करने के लिए सभी किसानों और किसान संगठनों को अपने सारे अंतर्विरोधों को दरकिनार कर के आगे आना होगा, एकजुट होना होगा. अभी नहीं तो कभी नहीं. हमें स्पष्ट रूप से यह तय करना होगा कि एमएसपी नहीं तो वोट नहीं. नारा भी दिया गया है, ‘गांवगांव एमएसपी, घरघर एमएसपी’ और ‘फसल हमारी, भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा’.
अब नारों और और जुमलों से आगे जा कर यह साबित करना होगा कि अगर सत्ता चाहिए तो आप को सब से पहले देश के किसान संगठनों के साथ बैठ कर किसानों के लिए लाभकारी ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून’ बनाना होगा.
– डा. राजाराम त्रिपाठी, राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा) और राष्ट्रीय प्रवक्ता, एमएसपी गारंटी किसान मोरचा.
 तुलसी को ठंड से बचाने के वैज्ञानिक उपाय
तुलसी को ठंड से बचाने के वैज्ञानिक उपाय









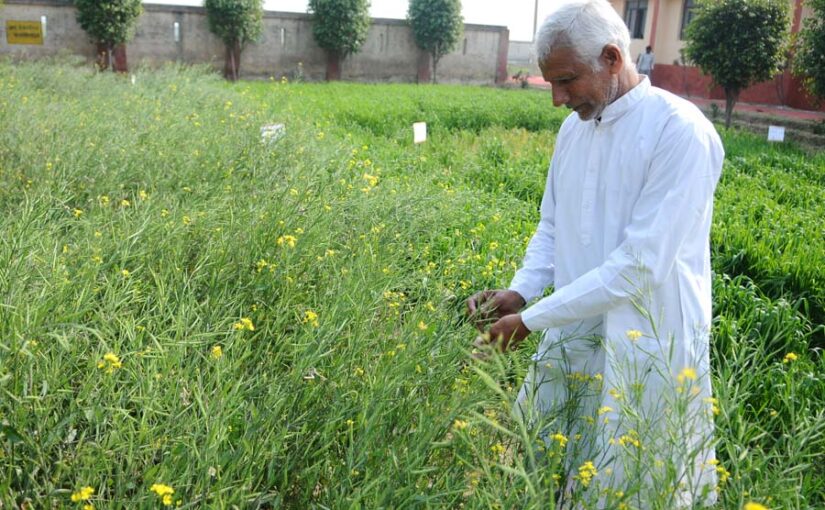

 उन्होंने यह भी कहा कि कई बार दलहन उत्पादक किसानों को सटोरियों या किसी अन्य स्थिति के कारण उचित दाम नहीं मिलते थे, जिस से उन्हें बड़ा नुकसान होता था. इस वजह से वे किसान दलहन की खेती करना पसंद नहीं करते थे. हम ने तय कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पूर्व ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, उस की दलहन को एमएसपी पर खरीद लिया जाएगा. इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद किसानों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे. फसल आने पर अगर दाम एमएसपी से ज्यादा होगा, तो उस की एवरेज निकाल कर भी किसान से ज्यादा मूल्य पर दलहन खरीदने का एक वैज्ञानिक फार्मूला बनाया गया है और इस से किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी.
उन्होंने यह भी कहा कि कई बार दलहन उत्पादक किसानों को सटोरियों या किसी अन्य स्थिति के कारण उचित दाम नहीं मिलते थे, जिस से उन्हें बड़ा नुकसान होता था. इस वजह से वे किसान दलहन की खेती करना पसंद नहीं करते थे. हम ने तय कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पूर्व ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, उस की दलहन को एमएसपी पर खरीद लिया जाएगा. इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद किसानों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे. फसल आने पर अगर दाम एमएसपी से ज्यादा होगा, तो उस की एवरेज निकाल कर भी किसान से ज्यादा मूल्य पर दलहन खरीदने का एक वैज्ञानिक फार्मूला बनाया गया है और इस से किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी. केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, किसान हित में अनेक ठोस कदम उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा कृषि क्षेत्र को सतत बढ़ावा दे रही है, जिन में दलहन में देश के आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य अहम है, जिस पर कृषि मंत्रालय भी तेजी से काम कर रहा है.
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, किसान हित में अनेक ठोस कदम उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा कृषि क्षेत्र को सतत बढ़ावा दे रही है, जिन में दलहन में देश के आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य अहम है, जिस पर कृषि मंत्रालय भी तेजी से काम कर रहा है. उन्होंने प्रसन्नता जताई कि 2 शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसा पोर्टल बनाया गया है, जहां किसान पंजीयन के पश्चात स्टाक ऐंट्री कर पाएंगे, स्टाक के वेयरहाउस पहुंचते ई-रसीद जारी होने पर किसानों को सीधा पेमेंट पोर्टल से बैंक खाते में होगा. पोर्टल को वेयरहाउसिंग एजेंसियों के साथ एकीकृत किया है, जो वास्तविक समय आधार पर स्टाक जमा निगरानी करने में सहायक होगा, जिस से समय पर पेमेंट होगा. इस प्रकार खरीदे स्टाक का उपयोग उपभोक्ताओं को भविष्य में अचानक मूल्य वृद्धि से राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा. स्टाक राज्य सरकारों को उन की पोषण व कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपयोग के लिए भी उपलब्ध होगा.
उन्होंने प्रसन्नता जताई कि 2 शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसा पोर्टल बनाया गया है, जहां किसान पंजीयन के पश्चात स्टाक ऐंट्री कर पाएंगे, स्टाक के वेयरहाउस पहुंचते ई-रसीद जारी होने पर किसानों को सीधा पेमेंट पोर्टल से बैंक खाते में होगा. पोर्टल को वेयरहाउसिंग एजेंसियों के साथ एकीकृत किया है, जो वास्तविक समय आधार पर स्टाक जमा निगरानी करने में सहायक होगा, जिस से समय पर पेमेंट होगा. इस प्रकार खरीदे स्टाक का उपयोग उपभोक्ताओं को भविष्य में अचानक मूल्य वृद्धि से राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा. स्टाक राज्य सरकारों को उन की पोषण व कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपयोग के लिए भी उपलब्ध होगा.



 पलवार लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए :
पलवार लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए :


 निगरानी:
निगरानी: 
 कौन हैं अपूर्वा त्रिपाठी
कौन हैं अपूर्वा त्रिपाठी