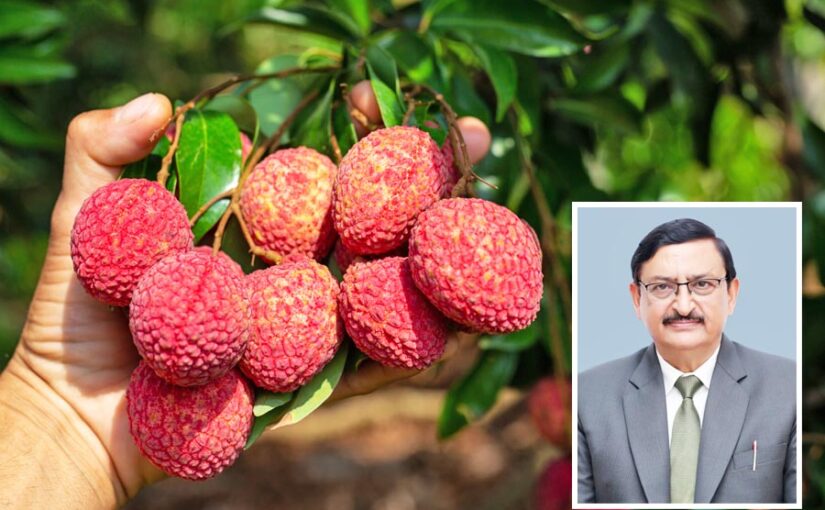उदयपुर : 30 अप्रैल, 2024. एमपीयूएटी के गोद लिए बड़गांव पंचायत समिति के गांव मदार और ब्राह्मणों की हुंदर ने एक बार फिर स्मार्ट विलेज का खिताब अपने नाम कर प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है. प्रदेश के सभी 27 राजकीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी (यूएसआर) के तहत गांव गोद ले कर उसे स्मार्ट विलेज में रूपांतरित करने की राज्यपाल की पहल को एमपीयूएटी ने पूरी गंभीरता से लिया.
एमपीयूएटी की ओर से उक्त दोनों स्मार्ट विलेज को जनवरी से मार्च, 2024 की त्रैमासिक अवधि में किए गए नवाचार और अन्य गतिविधियों की समीक्षा के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने एमपीयूएटी के कुलपति डा. अजीत कुमार कर्नाटक के साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी इसे अनुकरणीय पहल के रूप में रेखांकित किया है. इस से पूर्व भी मदार और ब्राह्मणों की हुंदर गांव 2 बार यह खिताब मिल चुका है.
कुलपति डा. अजीत कुमार कर्नाटक ने एमपीयूएटी की विभिन्न टीमों ने इन गांवों में जा कर जो गतिविधियां की हैं, उस से न केवल कृषि, बल्कि सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है. यहीं नहीं, कोरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत 1.5 रुपए करोड़ से ज्यादा के काम संपादित होने की खुशी गांव वालों के चेहरों पर साफ झलकती है.
कुलपति डा. अजीत कुमार कर्नाटक ने बताया कि सीएसआर योजना के अंतर्गत नाबार्ड के सहयोग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मदार में 5 केवी क्षमता वाले सोलर ट्री की स्थापना की गई. इस की अनुमानित लागत 9.08 लाख रुपए है. इस से प्रतिदिन 15-20 यूनिट बिजली बन रही है, जिस से स्कूल, पनघट व स्ट्रीट लाइट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. आईआईएफएल, मुंबई और ब्लूइनफिनिटी लेब्स प्रा. लि. के सहयोग से कीटनाशक/पेस्टीसाइड/उर्वरक छिड़काव के लिए 25 किलोग्राम क्षमता का ड्रोन विश्वविद्यालय को दिया गया. इस की अनुमानित लागत 30 लाख रुपए है. इस का उपयोग स्मार्ट गांव में किया गया है. राजस्थान माइंस एवं मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदार में 150 बच्चों को टेबल, स्टूल और 4 अलमारी 3.94 लाख रुपए का फर्नीचर उपलब्ध कराया गया.
उन्होंने बताया कि आईआईएफएल, मुंबई के सहयोग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मदार को 50 कंप्यूटर टेबलेट, औक्सीजन कंसन्ट्रेटर और कोविड किट उपलब्ध कराए गए.
इस के अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मदार में कन्वेशन हाल को बनाने में तकरीबन 42 लाख रुपए की लागत आई है. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए विधायक मद से 10 लाख रुपए की लागत से खेल मैदान की चारदिवारी का काम किया गया.
स्मार्ट गांव मदार एवं ब्राहम्णों की हुंदर में 8 स्वयं सहायता समूह की 120 किसान महिलाएं सदस्य हैं, जो कि सब्जी उत्पादन, सिलाई केंद्र, अनाज भंडारण, दूध उत्पादन, सोलर लाइट, सोलर कुकर, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इत्यादि गतिविधियों से लाभान्वित हो रही हैं.
डा. अजीत कुमार कर्नाटक ने बताया कि इस विश्वविद्यालय द्वारा मदार एवं ब्राहम्णों की हुंदर गांव पंचायत समिति, बड़गांव (उदयपुर) को सितंबर, 2020 में गोद लिए गए थे. इन गांवों के विकास की कार्ययोजना स्मार्ट गांव क्रियान्वयन कमेटी द्वारा आजीविका अवसर एवं आर्थिक सृदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न स्किल ट्रेनिंग एवं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तरीकों से की जा रही है. विश्वविद्यालय के 130 वैज्ञानिकों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा 42 बार भ्रमण कर कार्ययोजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया. विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 36 एकदिवसीय प्रशिक्षणों के माध्यम से 2311 किसान एवं किसान महिलाएं लाभान्वित हुए.
निदेशक प्रसार डा. आरए कौशिक ने बताया कि विश्वविद्यालय के चयनित स्मार्ट गांव मदार एवं ब्राम्हणों की हुंदर में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 किसानों के खेतों पर गेहूं की उन्नत किस्म एचआई 1034 के प्रदर्शन लगाए गए थे. इसी प्रकार सब्जी व फूल प्रदर्शन में प्याज, पालक, गाजर, पूसा साग एवं मैरी गोल्ड आदि के 16 किसानों के खेतों पर प्रदर्शन लगाए गये थे.
उन्होंने बताया कि बंजर भूमि विकास हेतु ग्राम पंचायत एवं वन विभाग के सहयोग से 175 पेड़ नीम, करंज, जामुन, सुबबूल एवं मोरिंगा आदि लगाए गए. पशुपालन विभाग के सहयोग से शिविर आयोजित कर 360 पशुओं और 590 भेड़बकरियों का टीकाकरण व उपचार किया गया. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शिविर आयोजित कर 93 रोगियों का उपचार कर निःशुल्क दवाएं दी गईं. इसी क्रम में इफको के सहयोग से गेहूं की फसल पर ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया.












 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलसचिव प्रो. रामजी सिंह ने बताया कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश प्रदेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (यूपी कैटेट) के माध्यम से होता है. इस वर्ष यूपी कैटेट 2024 प्रवेश परीक्षा का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा ही कराया जा रहा है, जिस में आवेदन 17 मार्च, 2024 से ही प्राप्त किए जा रहे हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई, 2024 है.
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलसचिव प्रो. रामजी सिंह ने बताया कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश प्रदेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (यूपी कैटेट) के माध्यम से होता है. इस वर्ष यूपी कैटेट 2024 प्रवेश परीक्षा का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा ही कराया जा रहा है, जिस में आवेदन 17 मार्च, 2024 से ही प्राप्त किए जा रहे हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई, 2024 है. कृषि विज्ञान केंद्र, कोटवा, आजमगढ़ में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डा. रुद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने के लिए वर्तमान में कुल 5 राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित हैं. इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान का स्तर अन्य महाविद्यालयों से बेहतर होता है. साथ ही, छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी और अच्छा शैक्षणिक माहौल भी मिलता है. यदि कृषि के क्षेत्र में नौकरी की बात करें, तो आज भी कृषि के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपार संभावनाएं हैं. लेकिन इस के लिए शिक्षा संस्थान जहां से शिक्षा ली गई है, बेहद मायने रखता है. श्री दुर्गाजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदेश्वर, आजमगढ़ के सहायक प्राध्यापक डा. सर्वेश कुमार ने बताया कि स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रछात्राएं भी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.
कृषि विज्ञान केंद्र, कोटवा, आजमगढ़ में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डा. रुद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने के लिए वर्तमान में कुल 5 राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित हैं. इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान का स्तर अन्य महाविद्यालयों से बेहतर होता है. साथ ही, छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी और अच्छा शैक्षणिक माहौल भी मिलता है. यदि कृषि के क्षेत्र में नौकरी की बात करें, तो आज भी कृषि के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपार संभावनाएं हैं. लेकिन इस के लिए शिक्षा संस्थान जहां से शिक्षा ली गई है, बेहद मायने रखता है. श्री दुर्गाजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदेश्वर, आजमगढ़ के सहायक प्राध्यापक डा. सर्वेश कुमार ने बताया कि स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रछात्राएं भी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. कृषि विभाग, आजमगढ़ में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक के पद पर काम कर रहे डा. मुलायम यादव ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालयों में बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि) व पीएचडी कर के प्रशासनिक पदों के साथ ही कृषि व अन्य संबंधित विभागों में अधिकारी व कर्मचारी के रूप में चयनित हो सकते हैं. साथ ही, ऊंची तालीम ले कर विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में वैज्ञानिक, महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों मे सहायक प्राध्यापक आदि पदों पर भी चयनित हो सकते हैं. इस के अलावा बैंकों व अर्धसरकारी कंपनी व निजी कंपनियों में भी कृषि के छात्रों को अच्छी नौकरी मिलती है.
कृषि विभाग, आजमगढ़ में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक के पद पर काम कर रहे डा. मुलायम यादव ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालयों में बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि) व पीएचडी कर के प्रशासनिक पदों के साथ ही कृषि व अन्य संबंधित विभागों में अधिकारी व कर्मचारी के रूप में चयनित हो सकते हैं. साथ ही, ऊंची तालीम ले कर विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में वैज्ञानिक, महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों मे सहायक प्राध्यापक आदि पदों पर भी चयनित हो सकते हैं. इस के अलावा बैंकों व अर्धसरकारी कंपनी व निजी कंपनियों में भी कृषि के छात्रों को अच्छी नौकरी मिलती है. आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की शोध छात्रा रूपाली सिंह ने बताया कि ग्रामीण छात्राओं के लिए भी कृषि विश्वविद्यालयों से शिक्षा लेना एक बेहतर विकल्प है. यहां से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्रामीण युवा कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर के न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार के साधन मुहैया करा सकते हैं.
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या की शोध छात्रा रूपाली सिंह ने बताया कि ग्रामीण छात्राओं के लिए भी कृषि विश्वविद्यालयों से शिक्षा लेना एक बेहतर विकल्प है. यहां से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्रामीण युवा कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर के न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार के साधन मुहैया करा सकते हैं.
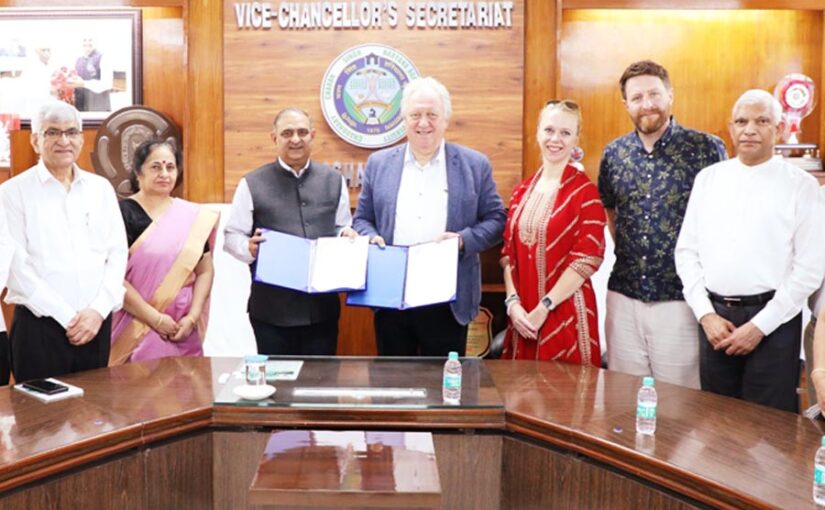

 कार्यशाला के चीफ पैटर्न व हकृवि के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि क्षेत्र की अह्म भूमिका रहेगी. कृषि हमेशा से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है. यह लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है और हमारी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है. हाल ही के वर्षों में, इस क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो इस क्षेत्र को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे संकल्प को मजबूत करने में मदद करेगी.
कार्यशाला के चीफ पैटर्न व हकृवि के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि क्षेत्र की अह्म भूमिका रहेगी. कृषि हमेशा से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है. यह लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है और हमारी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है. हाल ही के वर्षों में, इस क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो इस क्षेत्र को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे संकल्प को मजबूत करने में मदद करेगी.