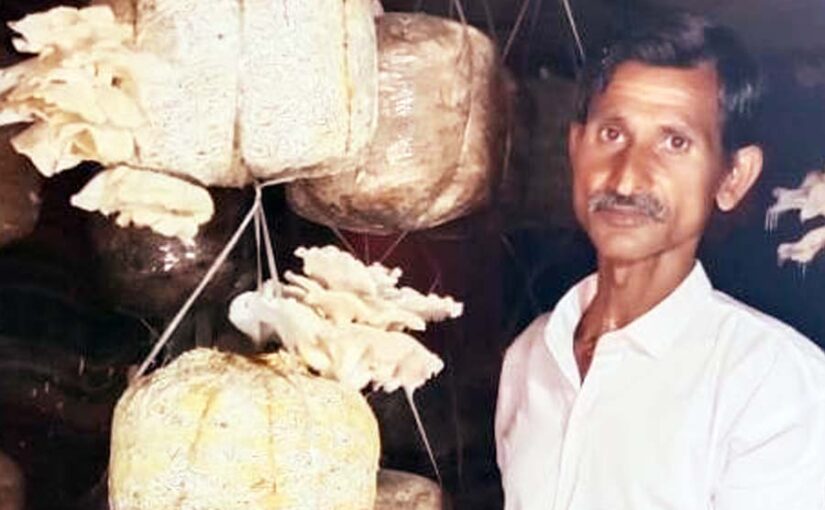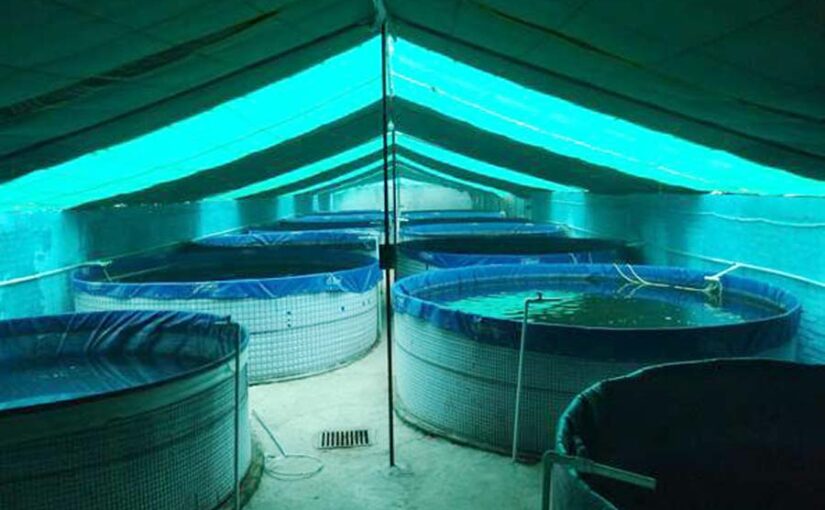हिसार : बदलते समय के साथसाथ अगर हमें कृषि क्षेत्र में कृषि क्रियाओं को समयानुसार क्रियान्वित करने से जुड़ी चुनौतियों व श्रमिकों की कमी को देखते हुए ड्रोन तकनीक को अपनाना होगा. इस तकनीक को अपनाने से कृषि लागत को कम करने के साथसाथ संसाधनों की भी बचत की जा सकती है.
यह विचार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर कंबोज ने व्यक्त किया. वे विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कृषि मेला (खरीफ) के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे.
मेले में विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल के कुलपति डा. सुरेश कुमार मल्होत्रा और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई मौजूद रहे.
इस बार मेले का मुख्य विषय खेती में ड्रोन का महत्व है. मुख्यातिथि प्रो. बीआर कंबोज ने आह्वान किया कि किसान समुदाय को नईनई तकनीकों व प्रौद्योगिकियों के बारे में समयानुसार अपडेट करते रहना समय की मांग है. उन्होंने आगे यह भी कहा कि खेती में ड्रोन तकनीक का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण को संरक्षित रखना मुख्य चुनौतियां हैं. साथ ही, किसानों द्वारा फसलों में कीटनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग करने से इनसान अनेक बीमारियों की चपेट में भी आ रहा है. हमें उपरोक्त चुनौतियों से निबटना है तो किसानों को ड्रोन तकनीक को अपनाना होगा, क्योंकि ड्रोन के द्वारा कम समय में जल विलय उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का छिडक़ाव समान तरीके से व सिफारिश के अनुसार आसानी से किया जा सकता है, जिस से कम लागत होने के साथसाथ संसाधनों की भी बचत होगी.
मुख्यातिथि प्रो. बीआर कंबोज ने कृषि मेला खरीफ में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर खुशी जताई. साथ ही कहा कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र के अंदर महिलाओं की भूमिका दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है.
प्रो. बीआर कंबोज ने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वे विभिन्न फसलों की उन्नत 44 किस्में अनुमोदित व विकसित कर किसान समुदाय को माली मजबूती देने का काम कर रहे हैं, जिस की बदौलत हमारा विश्वविद्यालय कृषि क्षेत्र में अनूठी पहचान बना रहा है.
उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा ईजाद की गई अधिक पैदावार देने वाली किस्म, जिन में सरसों की रोग प्रतिरोधी व पाले के प्रति सहनशील किस्म आरएच 725, गेहूं की अधिक उत्पादकता देने वाली किस्म डब्ल्यूएच 1270 का जिक्र करते हुए खरीफ फसलों में चारे वाली ज्वार की अधिक पैदावार देने वाली सीएसवी 53 एफ व एचजे 1514, बाजरे की जिंक व लौह तत्व से भरपूर बायोफोर्टीफाइड किस्म एचएचबी 299 व एचएचबी 311 एवं मूंग की एमएच 421 किस्म के बारे में भी बताया.
महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल के कुलपति डा. सुरेश कुमार मल्होत्रा ने बताया कि हरियाणा का किसान प्रगतिशील किसान है. अपने प्रयासों की बदौलत वह अन्य राज्यों के किसानों, प्रौद्योगिकियों व नवाचारों के मुकाबले में सब से आगे हैं. इसलिए किसान खाद्य सुरक्षा, खाद्य भंडारण, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण जैसी अनेक चुनौतियों का हल निकालने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है. तिलहनी व दलहनी फसलों की मांग के मुकाबले उत्पादन कम है, जिस के कारण आयात करना पड़ता है. इस मांग को पूरा करने के लिए हमें खरीफ एवं रबी सीजन के अलावा रबी सीजन के तुरंत बाद आने वाली गरमी के मौसम में एक कम अवधि वाली फसल ले कर खेती को लाभदायक बनाने के बारे में भी प्रेरित किया. हकृवि कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षा, विस्तार के क्षेत्र सराहनीय काम कर रहा है.
गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि फसलों की अधिक पैदावार लेने के लिए पर्यावरण का अनुकूल होना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि हमें फसलों के अवशेष जैसे धान की पराली को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने से एक ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है, वहीं दूसरी ओर मित्र कीट एवं लाभदायक जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं. यदि फसल के अवशेष जलाने के बजाय किसान उन्हें खेत में ही समायोजित करें, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी व पर्यावरण संरक्षण होगा.
मुख्यातिथि सहित अन्य अधिकारियों ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी को सराहा
कृषि मेला खरीफ में विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों की ओर से विभिन्न विषयों पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिस में विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में सहित आधुनिक तकनीकों व कृषि यंत्र शामिल रहे. मुख्यातिथि सहित अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया. साथ ही, वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों के प्रयासों को सराहा.
इस प्रदर्शनी में कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए किसानवैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया, जिस में किसानों ने फसलों से संबंधित समस्याओं के हल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से जाने.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यातिथि प्रो. बीआर कंबोज ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया. इस के अलावा उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन करते हुए संबंधित विभागों के वैज्ञानिकों को बधाई दी.
कृषि मेला खरीफ में पहले दिन हरियाणा व अन्य राज्यों से तकरीबन 40 हजार किसानों ने भाग लिया. मंच का संचालन हरियाणा कला परिषद, हिसार मंडल के अतिरिक्त निदेशक रामनिवास शर्मा ने किया. मेले में उपस्थित किसानों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया.