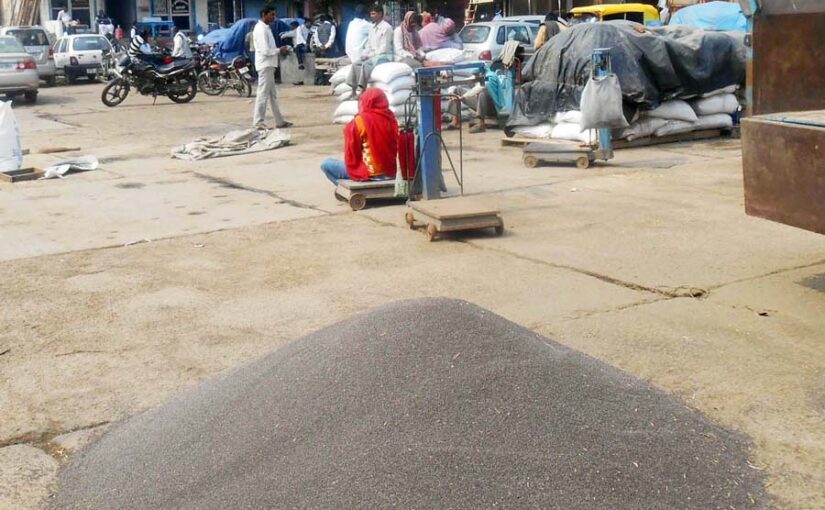नई दिल्लीः केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), नेशनल कोआपरेटिव आर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया.
इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा और डा. आशीष कुमार भूटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय के साथसाथ एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरैक्टर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहां तीन कोऑपरेटिव्स के नए कार्यालय के उद्घाटन के रूप में एक बहुत बड़े काम का बीज बोया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ की कल्पना के साथ हम आगे बढ़े हैं.
उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय में शुरू में ही गैप्स, उन्हें भरने, कोआपरेटिव्स का दायरा बढ़ाने और टर्नओवर और मुनाफा बढ़ा कर किसानों तक उसे पहुंचाने की गतिविधियों की पहचान कर ली गई थी और इन तीनों समितियों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी.
मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आज 31,000 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले और स्टेट औफ द आर्ट तकनीक के साथ बने इस कार्यालय में इन समितियों का मुख्यालय शुरू होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम इस कार्यालय में कारपोरेट क्षेत्र के सारे नवाचार का अनुभव करेंगे और उन्हें प्राप्त भी करेंगे. उन्होंने कहा कि ये तीनों समितियां किसानों की अलगअलग प्रकार की जरूरतों को पूरा करने वाली हैं.
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुत कम समय में हम ने तीनों समितियों को बनाने के लिए देश की प्रमुख सहकारी समितियों, अमूल, नेफेड, एनसीसीएफ, इफको, कृभको, एनडीडीबी और एनसीडीसी को इन के मूल प्रमोटर के रूप में एकत्रित किया और इन सभी संस्थाओं ने मिल कर इन तीनों समितियों को स्थापित करने का काम किया.
उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को कोआपरेटिव समितियों से लगभग 7,000, आर्गेनिक लिमिटेड को 5,000 और बीज सहकारी समिति को 16,000 सदस्यता आवेदन मिल चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह बताता है कि काम का दायरा कितना बढ़ा है और इतने कम समय में हम इसे इतना नीचे तक उतारने में सफल रहे हैं.
मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन तीनों समितियों की स्थापना एक बहुमुखी उद्देश्य के साथ की गई थी और जब ये पूरी तरह से काम करने लग जाएंगी, तब हमारे किसानों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कैमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी जमीन खराब होती जा रही है, हमें इसे बचाना है और आर्गेनिक खेती की ओर किसानों को ले जाना आज के समय की मांग है.
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की समृद्धि, भूमि, जल संरक्षण, बाढ़ से बचाव के साथसाथ 130 करोड़ भारतीयों और विश्वभर के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी आर्गेनिक उत्पादों की वृद्धि, मार्केटिंग और पहुंच बढ़ाना बहुत जरूरी है. साथ ही, उन्होंने कहा कि इस के लिए बनाई गई समिति आर्गेनिक उत्पादों के कलैक्शन, सर्टिफिकेशन, टैस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, खरीद, स्टोरेज, प्रोसैसिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और निर्यात तक की पूरी चेन का सब काम खुद भी करेगी और कई कोआपेरेटिव्स के लिए गाइड का काम भी करेगी.
अमित शाह ने कहा कि बीज के लिए बनाई गई सहकारी समिति हमारे प्राकृतिक, मीठे और पारंपरिक बीजों के स्वाद, गुणवत्ता और बीज को संरक्षित और संवर्धित करने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि हम पीएसीएस के माध्यम से ढाई एकड़ जमीन वाले किसानों को भी बीज का प्लाट देने और उन की आय में बढ़ोतरी का काम करेंगे.
मंत्री अमित शाह ने कहा कि जैविक उत्पादों के लिए बनी समिति इन उत्पादों के मिलने वाले अच्छे दाम में से बहुत छोटा हिस्सा अपने संचालन के लिए रख कर ज्यादातर हिस्सा कोआपरेटिव डेयरी के स्तर पर किसानों को वापस देगी. इसी प्रकार निर्यात के लिए बनी समिति कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात में हमारे देश के हिस्से को बढ़ाएगी और इस से होने वाला मुनाफा सीधा किसानों के बैंक खातों में जमा होगा.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम ने तय किया है कि अगले 5 साल में निर्यात कोआपरेटिव सोसाइटी के टर्नओवर को सालाना एक लाख करोड़ रूपए तक पहुचाएंगे और निर्यात में फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर दलहन के आयात की कमी को भी इसी माध्यम से पूरा किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि दलहन का उत्पादन तभी बढ़ सकता है, जब इस के निर्यात की सुचारु व्यवस्था हो और तभी किसान दलहन बोएगा. अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि कम से कम 50 फीसदी मुनाफा पीएसीएस के माध्यम से सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाए.
अमित शाह ने कहा कि आज हमारे देश में गुजरात सहित कई राज्यों में लाखों किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है. प्राकृतिक खेती के मौडल में एक देशी गाय से 21 एकड़ भूमि की खेती होती है, उत्पादन कम नहीं होता है और भूमि की उर्वरता बढ़ती जाती है. पिछले 3 सालों में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या में 7 गुना वृद्धि हुई है, जो बताता है कि ये प्रयोग सफल रहा है.
मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने देशभर में आर्गेनिक खेती में भूमि परीक्षण और अनाज के प्रोडक्शन की टेस्टिंग के लिए लैबोरेट्रीज का जाल बुनने का काम हाथ में लिया है. अगले 5 साल में देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा, जहां आर्गेनिक भूमि और प्रोडक्ट का परीक्षण नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि जहां आर्गेनिक उपज ज्यादा है, वहां तक इस प्रक्रिया को ले जा कर और इसे किसानों को उपलब्ध करा कर उत्पाद को सर्टिफाइड कर बाजार का मुनाफा उस तक पहुंचने का काम करेंगे.
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम ने बीज सहकारी लिमिटेड के लिए 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रूपए से ज्यादा टर्नओवर का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि साल 2030 तक आर्गेनिक्स भारत के घरेलू बाजार में 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी रखेगा.
उन्होंने कहा कि आज वैश्विक आर्गेनिक बाजार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है और इस में भारत का निर्यात 7,000 करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ा कर हम 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहते हैं. वहीं वैश्विक कृषि उपज बाजार 2,155 अरब डालर है और इस में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 45 अरब डालर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम ने तय किया है कि साल 2030 तक एक बड़ी छलांग लगा कर इसे 115 अरब डालर तक पहुंचाएंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि इन तीन समितियों के माध्यम से आने वाले दिनों में आर्गेनिक प्रोडक्ट, बीज संरक्षण और संवर्धन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में सभी गैप्स को भरने में सफलता मिलेगी.