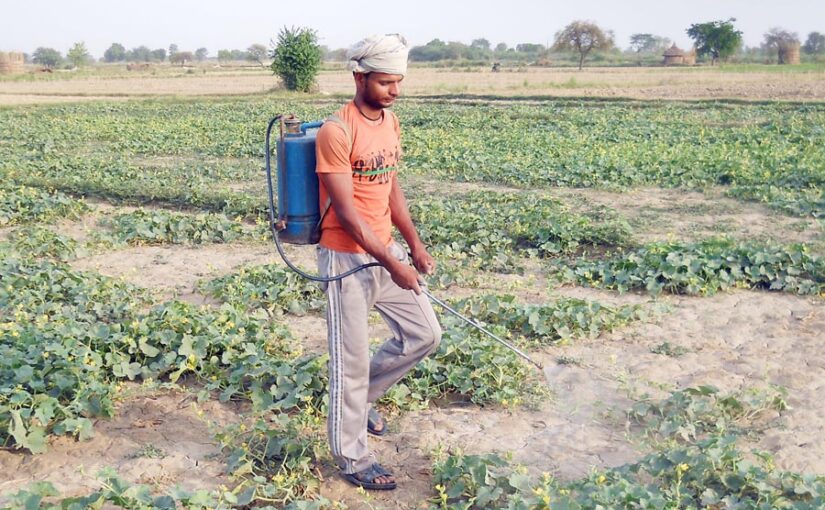हिसार: चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत चल रहे फार्मर फस्र्ट प्रोग्राम के तहत किसानों के लिए ‘‘पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण की उपयोगिता’’ विषय पर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में हिसार जिले के गांव पायल व चिड़ोद के किसानों ने भाग लिया.
फार्मर फस्र्ट प्रोग्राम के प्रमुख अन्वेषक डा. अशोक गोदारा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने व दूध उत्पादन बढ़ाने की जानकारी देना है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकें. फार्मर फस्र्ट प्रोग्राम (एफएफपी) के तहत उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के अलावा किसानवैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ा कर छोटे किसानों की कृषि और अधिकांश किसानों की जटिल, विविध और जोखिम वाली वास्तविकताओं को महत्त्व देने के लिए आईसीएआर की एक पहल है.
उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत कृषि में संसाधन प्रबंधन, जलवायु लचीली कृषि, भंडारण, बाजार, आपूर्ति श्रंखला, मूल्य श्रंखला, नवाचार, सूचना प्रणाली आदि सहित उत्पादन प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाता है.
कार्यक्रम में पशु पोषण वैज्ञानिक डा. सज्जन सिहाग ने पशुओं को उन की अवस्था के अनुसार संतुलित आहार, जिस में हरा चारा, सूखा चारा, चोकर व मिनरल मिक्सचर खिलाने की सलाह दी.
उन्होंने कहा कि पशु के अंदर खनिज मिश्रण की कमी के कारण पशु जकड़न व नया दूध नहीं होता, पशु मूत्र पीते हैं, दीवार चाटते हैं, कपड़ा, गाभा व मिट्टी खाते हैं. इसलिए पशुओं को खनिज मिश्रण पूरे साल रोज देते रहें. इस से पशु को बहुत ही फायदा होगा.
चारा अनुभाग के सस्य वैज्ञानिक डा. सतपाल ने हरा चारा उत्पादन व पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सालभर हरा चारा उपलब्ध करवाने के लिए फसल चक्रों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कम खर्च पर अधिक दूध उत्पादन के लिए जरूरी है कि पशुओं को पौष्टिक व संतुलित मात्रा में हरा चारा पूरे साल मिलता रहे. साल के कुछ माह में जैसे अक्तूबरनवंबर व मईजून में हरे चारे की कमी आ जाने के कारण हम पशुओं को हरा चारा पूरी मात्रा में नहीे दे पाते हैं, जिस के फलस्वरूप पशुओं की सेहत खराब हो जाती है और दूध उत्पादन में कमी आ जाती है.
उन्होंने बताया कि मईजून माह में हरे चारे की कमी न हो, इस के लिए पशुपालक मार्च माह में ही ज्वार, मक्का, लोबिया आदि फसलों की बिजाई कर सकते हैं. मार्च माह में अनेक कटाई देने वाली ज्वार की किस्म जैसे एसएसजी 59-3 व सीएसवी 33 एमएफ (अनंत) व सीएसएच 24 एमएफ की बिजाई कर सकते हैं, जिस से 4 से 5 कटाई में नवंबर माह तक हरा चारा मिलता रहेगा.
कार्यक्रम के अंत में पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य सुधार के लिए मिनरल मिक्सचर के 5-5 किलोग्राम के पैकेट महत्त्वपूर्ण इनपुट के तौर पर निःशुल्क वितरित किए गए. इस अवसर पर पौध रोग विशेषज्ञ डा. एचएस सहारण व एसआरएफ डा. बिट्टू राम भी मौजूद रहे.