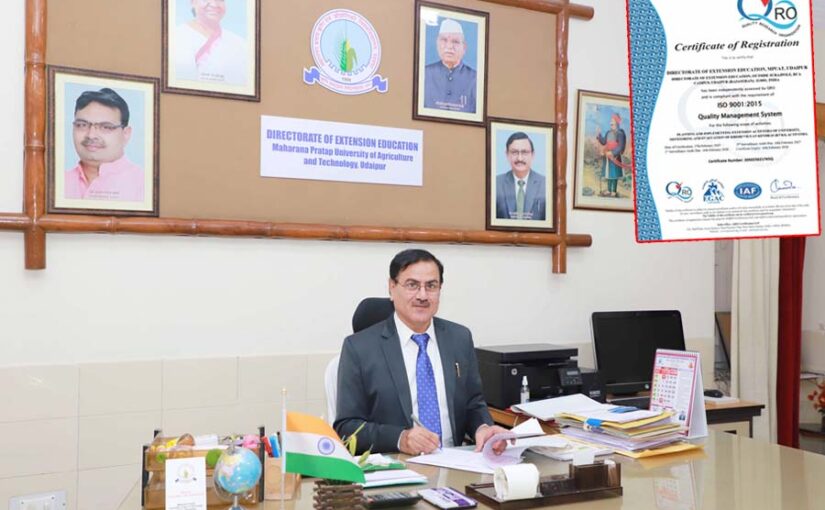नई दिल्ली : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 22 फरवरी से 24 फरवरी में आयोजित होने जा रहा है. मेले का विषय “उन्नत कृषि विकसित भारत” है.
इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे. रामनाथ ठाकुर, राज्य मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे. भागीरथ चौधरी, राज्य मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 24 फरवरी, 2025 को आयोजित समापन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे. डा. हिमांशु पाठक, सचिव डेयर और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उद्घाटन और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे.
इस साल के पूसा कृषि विज्ञान मेले के मुख्य आकर्षण होंगे :
– भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नई किस्मों और तकनीकों का लाइव प्रदर्शन.
– भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, एफपीओ, उद्यमियों, स्टार्टअप्स, सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा नवीन तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी.
– तकनीकी सत्र और किसानों वैज्ञानिकों के साथ संवाद, जो जलवायु अनुकूल कृषि, फसल विविधीकरण, डिजिटल कृषि, युवाओं और महिलाओं का उद्यमिता विकास, कृषि विपणन, किसान संगठन और स्टार्टअप्स, और किसानों के नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित होंगे.
– पूसा द्वारा विकसित फसलों की किस्मों की बिक्री.
– मेले के दौरान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि सलाह.
जलवायु जोखिम और पोषण के बढ़ते महत्व को समझते हुए पूसा संस्थान में अनुसंधान जलवायु अनुकूल किस्मों और बायोफोर्टिफाइड किस्मों के विकास पर केंद्रित है, जो उच्च उत्पादकता के साथ बेहतर पोषण सुरक्षा प्रदान करता है.
साल 2024 के दौरान 10 विभिन्न फसलों में कुल 27 नई किस्में विकसित की गई हैं, जिन में 7 गेहूं की किस्में, 3 चावल, 8 संकर मक्का, 1 संकर बाजरा, 2 चने की किस्में, 1 अरहर संकर, 3 मूंग दाल की किस्में, 1 मसूर की किस्म, 2 डबल जीरो सरसों की किस्में और 1 सोयाबीन की किस्म शामिल हैं. इन में 16 किस्में और 11 संकर किस्में हैं.
बदलते जलवायु परिदृश्य के तहत पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 जलवायु अनुकूल और बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया गया है, जिस में 7 अनाज और मिलेट्स, 2 दालें और 1 चारा किस्म शामिल है.
संस्थान ने बासमती धान उत्पादन और व्यापार में श्रेष्ठ किस्मों के विकास के माध्यम से विशाल योगदान दिया है. पूसा बासमती धान की किस्मों में पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1509 और उन्नत बासमती धान की किस्में, जिन में बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे पीबी-1847, पीबी-1885 और पीबी-1886.
साल 2023-2024 में भारत से 5.2 मिलियन टन बासमती धान के निर्यात से 48,389 करोड़ रुपए की आय में लगभग 90 फीसदी योगदान करती है. अप्रैल, 2024 से नवंबर, 2024 तक पूसा के बासमती धान से निर्यात आय 31,488 करोड़ रुपए तक पहुंची है. 2 छोटी अवधि वाली धान की किस्में पूसा 1824 और पूसा 2090 विकसित की गई हैं, जो बाद में रबी फसल के खेतों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय प्रदान कर सकती हैं.
पूसा आरएच 60 एक उच्च उपज वाली, छोटी अवधि वाली सुगंधित धान की संकर किस्म है, जिस में लंबे, पतले दाने होते हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए सब से मुफीद है. पूसा नरेंद्र केएन-1 और पूसा सीआरडी केएन-2 उन्नत काला नमक धान की किस्में हैं, जिन में बेहतर प्रतिरोधक क्षमता और उच्च उपज है, जो उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित हैं.
पूसा के अनुसंधान कार्यक्रम ने पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया और 8 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया. एक गेहूं की किस्म (एचआई-1665) और एक ड्यूरम गेहूं की किस्म (एचआई-60 पीपीएम), प्रोविटामिन ए (6.22पीपीएम), उच्च लाइसीन (4.93 फीसदी) और ट्रिप्टोफैन (1.01 फीसदी) से समृद्ध किया गया है.
पूसा बायोफोर्टिफाइड मक्का संकर-4 को उच्च प्रोविटामिन A, लाइसीन, ट्रिप्टोफैन से बायोफोर्टिफाइड किया गया है. पूसा पौपकौर्न संकर-1 और संकर-2 उच्च पौपिंग फीसदी और बटरफ्लाई प्रकार के पौप किए गए फ्लैक्स प्रदान करते हैं, जो एनडब्ल्यूपीजेड और पीजेड क्षेत्रों के लिए अनुशंसित हैं. पूसा एचएम-4 मेल स्टीराइल बेबीकौर्न-2 एक मेल स्टीराइल आधारित संकर है, जिसे एनईपीजेडपीजेड और सीडब्ल्यूजेड क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है.
2 डबल जीरो सरसों की किस्में (पूसा सरसों-35 और पूसा सरसों-36), जिन में एरूसिक अम्ल और ग्लूकोसिनोलेट्स कम होते हैं. समय पर बोई गई सिंचित परिस्थितियों में यह उच्च उपज प्रदान करती हैं, जो क्षेत्र-III (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान) के लिए उपयुक्त हैं. पूसा-1801 (एमएच 2417) बाजरा की एक द्विउद्देश्यीय किस्म (अनाज और चारा) है, जो उच्च लोहा (70 पीपीएम) और जिंक (57 पीपीएम) से युक्त बायोफोर्टिफाइड किस्म हैं. यह कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक है और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सब से उपयुक्त है.
चने की किस्म पूसा चना विजय 10217 उच्च उपज वाली किस्म है, जो फ्यूजेरियम विल्ट के प्रति प्रतिरोधक है. उत्तर प्रदेश में यह सिंचित परिस्थितियों के लिए अनुशंसित है. चने की किस्म पूसा-3057 में उच्च प्रोटीन (24.3 फीसदी) है और कई रोगों, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट (उकठा), कौलर रोट (तना गलन) और ड्राई रूट रोट (जड़ गलन) के प्रति प्रतिरोधक है.
यह पोड बोरर (फली बेधक सूँडी) के प्रति भी मध्यम प्रतिरोधक है और इस के बीज आकर्षक रंग और बड़े आकार के होते हैं.
अरहर की किस्म पूसा अरहर हाइब्रिड-5 उच्च उपज वाली किस्म है (औसतन 23.35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक, और संभावित उपज 25.46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो एसएमडी, फाइटोफोथोरा स्टेम ब्लाइट, मैक्रोफोमिना ब्लाइट (अंगमारी) और अल्टरनेरिया लीफ स्पौट (पत्ती धब्बा रोग) के प्रति प्रतिरोधक है और यह दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है.
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा छोटे किसानों के लिए 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कृषि प्रणाली मौडल विकसित किया गया है, जिस में फसलें, डेयरी, मछलीपालन, बतखपालन, बायोगैस संयंत्र, फलदार पेड़ और कृषि वनस्पति शामिल हैं. इस मौडल में प्रति हेक्टेयर हर साल 3 लाख, 79 हजार रुपए तक की शुद्ध आय प्राप्त करने की क्षमता है. इसी तरह, पूसा संस्थान द्वारा 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली मौडल विकसित किया गया है, जिस में पौलीहाउस, मशरूम की खेती के साथसाथ फसल और बागबानी आदि गतिविधियां भी शामिल हैं. इस मौडल से प्रति एकड़ हर साल एक लाख, 75 हजार 650 रुपए की शुद्ध आय पैदा करने की क्षमता है.
बागबानी आधारित फसल विविधीकरण किसानों के बीच लोकप्रिय रहा है. सब्जियों, फलों और फूलों की खेती लाभदायक रही है, जबकि फलों और सब्जियों की खेती पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी उपयोगी है.
सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने 48 सब्जी फसलों में 268 सुधारित सब्जी किस्में विकसित की हैं, जिन में 41 संकर और 227 किस्में शामिल हैं. आईएआरआई ने गाजर (पूसा प्रतीक, पूसा रुधिरा, पूसा असिता), भिंडी (पूसा लाल भिंडी-1), भारतीय सेम (पूसा लाल सेम), ब्रोकोली (पूसा पर्पल ब्रोकोली-1) और विटामिन सी से भरपूर पालक की किस्म (पूसा विलायती पालक) जैसे पोषणयुक्त किस्में विकसित की हैं, ताकि कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सके.
यलो वेन मोजेक वायरस (वेयूएमवी) प्रतिरोधी और ए नैशन लीफ कर्ल वायरस (ईएलसीवी) सहिष्णु भिंडी की किस्में (पूसा भिंडी-5 और डीओएच-1) पैस्टिसाइड्स के उपयोग को कम करने और खेती की लागत में कमी लाने के लिए विकसित की गई हैं.
हाल के सालों में बैंगन की 6 किस्में और एक संकर, प्याज की 3 किस्में, खीरे की 2 किस्में और 1 संकर, भारतीय सेम की 3 किस्में, करेला की 3 संकर किस्में और खरबूजे की 2 किस्में और 1 संकर विकसित की गई हैं. 2 सौफ्टसीडेड अमरूद की किस्में, पूसा आरुषि (लाल गूदा) और पूसा प्रतीक्षा (सफेद गूदा), साथ ही, एक उभयलिंगी, सैमीड्वार्फ पपीता किस्म, पूसा पीत भी विकसित की गई है.
एक गेंदा किस्म, पूसा बहार को केंद्रीय किस्म विमोचन समिति द्वारा जोन IV, V, VI और VII में विमोचन के लिए अनुशंसा की गई है. साल 2018-19 में (239.861 टन) से ले कर साल 2023-24 में (975.478 टन) तक गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन चौगुना से अधिक बढ़ा है.
जैव रसायन संभाग द्वारा विकसित पोषणयुक्त खाद्य उत्पादों में डिवाइन डो (बाजरे का आटा, जिस में गुणवत्ता वाली प्रोटीन, प्रतिरोधी स्टार्च, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे Fe और Zn होते हैं) शामिल हैं. पर्लीलोफ एक ग्लूटनमुक्त ब्रेड प्री-मिक्स है, जो पूरी तरह से बाजरा से बनाया गया है, जो गेहूं आधारित ब्रेड का पोषणयुक्त विकल्प प्रदान करता है. इस का ग्लाइसैमिक इंडेक्स (पीजीई 68-69 फीसदी) कम है, जो रक्तशर्करा के प्रबंधन में मदद करता है, जबकि यह फाइबर, आवश्यक खनिजों और बायोएक्टिव यौगिकों से भरपूर होता है.
पूसा संस्थान द्वारा एक त्वरित रंगमापी परीक्षण किट ‘स्पीडीसीड व्यायबिलिटी किट’ विकसित की गई है, जो 1–4 घंटे के भीतर बीज के प्रकार के आधार पर जीवित और अव्यायी बीजों के बीच अंतर करने में सक्षम है. इस किट में एक सूचक घोल शामिल है, जो जीवित बीजों द्वारा छोड़े गए CO₂ को पकड़ने पर रंग बदलता है. पूसा एसटीएफआर मीटर, जिसे पूसा संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, एक कम लागत, यूजर फ्रेंडली, डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामेबल उपकरण है, जो 14 महत्वपूर्ण मृदा मापदंडों का विश्लेषण करने के लिए है, जिस में गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि मृदा pH, EC, जैविक कार्बन, उपलब्ध N (जैविक कार्बन से व्युत्पन्न), P, K, S, B, Zn, Fe, Cu, Mn, साथ ही, चूना और जिप्सम की आवश्यकता का परीक्षण किया जा सकता है.
पूसा डीकंपोजर, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, एक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और आर्थिक रूप से प्रभावी सूक्ष्मजीव समाधान है, जो स्थल पर और स्थल के बाहर अवशेष प्रबंधन के लिए है.
पूसा डीकंपोजर को तैयार व उपयोग पाउडर रूप में भी किया गया है. यह पाउडर पूरी तरह से पानी में घुलने योग्य है और इसे आसानी से यांत्रिक स्प्रेयर के साथ उपयोग किया जा सकता है. खेत में धान के पुआल के विघटन के लिए प्रति एकड़ 500 ग्राम की सिफारिश की जाती है.
पूसा फार्म सन फ्रिज, जिसे संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, एक औफ-ग्रिड, बैटरीरहित सौर संवर्धित और वाष्पन शीतलक संरचना है. इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य खेतों में एक सौर शीतलक भंडारण केंद्र स्थापित करना है. इस ठंडे भंडारण का उपयोग नाशवान वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है.
“पूसा मीफ्लाई किट” और “पूसा क्यूफ्लाई किट” तैयार व उपयोग किट हैं, जो क्रमशः फलमक्खी की समस्या को विभिन्न प्रकार के फल और ककड़ी सब्जियों में प्रबंधित करने के लिए हैं. यह एक विशिष्ट और प्रभावी तरीका अपनाती है, जो बैक्ट्रोसेरा प्रजाति के नर फलमक्खियों को आकर्षित करने और नष्ट करने के लिए पैराफेरोमोन इन्प्रेग्नेशन का उपयोग करती है. यह पूरे मौसम के लिए पर्याप्त होती है. विभिन्न किटों को रोग प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है.
चिली लीफ कर्ल वायरस और मूंगफली पीले मोजेक वायरस का त्वरित निदान करने के लिए प्वाइंट औफ केयर डायग्नोस्टिक किट और ईजी पीसीआर डिटेक्शन किट विकसित की गई हैं. पूसा धान बकानी परीक्षण किट को बीज और मृदा में बकानी रोग का कारण बनने वाले पैथोजन (रोग कारक) की पहचान करने के लिए विकसित किया गया है.











 डा. उमाशंकर शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को 21 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सभी वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि अपनेअपने क्षेत्र में जा कर ब्रांड अंबेसडर की भूमिका निभाएं. इस प्रशिक्षण में 5 राज्यों के 26 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया. डा. एसके शर्मा, सहायक महानिदेशक, मानव संसाधन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने बताया कि प्राकृतिक कृषि (Natural farming) एक तकनीक ही नहीं, अपितु पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, जिस के द्वारा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया जाता है.
डा. उमाशंकर शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को 21 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान सभी वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि अपनेअपने क्षेत्र में जा कर ब्रांड अंबेसडर की भूमिका निभाएं. इस प्रशिक्षण में 5 राज्यों के 26 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया. डा. एसके शर्मा, सहायक महानिदेशक, मानव संसाधन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने बताया कि प्राकृतिक कृषि (Natural farming) एक तकनीक ही नहीं, अपितु पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, जिस के द्वारा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाया जाता है.