उस वाटिका को ‘पोषण वाटिका’ या ‘रसोईघर बाग’ या ‘गृहवाटिका’ कहा जाता है जो घर के अगलबगल में या घर के आंगन में ऐसी खुली जगह, जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल के लिए विभिन्न मौसम में मौसमी फल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं.
पोषण वाटिका का मुख्य मकसद ही रसोईघर का पानी व कूड़ाकरकट को पारिवारिक श्रम से उपयोग कर, घर की फल व सागसब्जियों की दैनिक जरूरतों की पूरा करने या आंशिक रूप से भरपाई करने की कोशिश करना व दैनिक आहार में उपयोग होने वाली सब्जी व फल शुद्ध, ताजा और जैविक उत्पाद रोजाना हासिल करना होता है.
आजकल बाजार में बिकने वाली ज्यादातर चमकदार फल और सागसब्जियों को रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर उगाया जाता है. इन फसल सुरक्षा पर तरहतरह के रसायनों का इस्तेमाल खरपतवार पर नियंत्रण, कीड़े और बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है, परंतु इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल और सागसब्जी में बाद तक भी बना रहता है.
इस के चलते इन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है और आम आदमी तरहतरह की बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है.
इस के अलावा फल और सागसब्जियों के स्वाद में भी काफी अंतर देखने को मिल जाता है, इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली खुली जगह में छोटीछोटी क्यारियां बना कर जैविक खादों का इस्तेमाल कर के रसायनरहित फल और सागसब्जियों का उत्पादन करना चाहिए.
जगह का चुनाव
इस के लिए जगह चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर यह जगह घर के पीछे या आसपास ही होती है. घर से मिले होने के कारण थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है.
गृहवाटिका के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए, जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, जैसे नलकूप या कुएं का पानी, स्नान का पानी, रसोईघर का पानी आदि पोषण वाटिका तक पहुंच सके.
जगह खुली हो, जिस में सूरज की रोशनी मिल सके. ऐसी जगह, जो जानवरों से सुरक्षित हो और उस जगह की मिट्टी उपजाऊ हो, ऐसी जगह का चुनाव पोषण वाटिका के लिए करना चाहिए.
पोषण वाटिका का आकार
जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है, वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की तादाद और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है.
लगातार फसल चक्र अपनाने, सघन बागबानी और अंत:फसल खेती को अपनाते हुए एक औसत परिवार, जिस में एक औरत, एक मर्द व 3 बच्चे यानी कुल 5 सदस्य हैं, ऐसे परिवार के लिए औसतन 25×10 वर्गमीटर जमीन काफी है. इसी से ज्यादा पैदावार ले कर पूरे साल अपने परिवार के लिए फल व सब्जियां हासिल की जा सकती हैं.
लेआउट करें तैयार
एक आदर्श पोषण वाटिका के लिए उत्तरी भारत खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध तकरीबन 250 वर्गमीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका के किसी एक तरफ लगाना चाहिए, जिस से कि इन पौधों की दूसरे पौधों पर छाया न पड़ सके और साथ ही, एकवर्षीय सब्जियों के फसल चक्र व उन के पोषक तत्त्वों की मात्रा में बाधा न डाल सके. पूरे क्षेत्र को 8-10 वर्गमीटर की 15 क्यारियों में बांट लें.
* वाटिका के चारों तरफ बाड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस में 3 तरफ गरमी और बरसात के समय कद्दूवर्गीय पौधों को चढ़ाना चाहिए और बची हुई चौथी तरफ सेम लगानी चाहिए.
* फसल चक्र, सघन फसल पद्धति और अंत:सस्य फसलों के उगाने के सिद्धांत को अपनाना चाहिए.
* 2 क्यारियों के बीच की मेंड़ों पर जड़ों वाली सब्जियों को उगाना चाहिए.
* रास्ते के एक तरफ टमाटर व दूसरी तरफ चौलाई या दूसरी पत्ती वाली सब्जी उगानी चाहिए.
* वाटिका के 2 कोनों पर खाद के गड्ढे होने चाहिए, जिन में से एक तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट व दूसरी ओर कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो, जिस में घर का कूड़ाकरकट और फसल अवशेष डाल कर खाद तैयार कर सकें.
* इन गड्ढ़ों के ऊपर छाया के लिए सेम आदि की बेल चढ़ा कर छाया बनाए रखें. इस से पोषक तत्त्वों का नुकसान भी कम होगा व गड्ढा भी छिपा रहेगा.
पोषण वाटिका के फायदे
* जैविक उत्पाद (रसायनरहित) होने के कारण फल और सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पौषक तत्व मौजूद रहते हैं.
* बाजार में फल और सब्जियों की कीमत ज्यादा होती है, जिसे न खरीदने से लगाई गई पूंजी में कमी होती है.
* परिवार के लिए ताजा फलसब्जियां मिलती रहती हैं.
* उपलब्ध सब्जियां बाजार के बजाय अच्छे गुणों वाली होती हैं.
* गृहवाटिका लगा कर औरतें परिवार की माली हालत को मजबूत बना सकती हैं.
* पोषण वाटिका से मिलने वाले मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित कर सालभर तक उपयोग किया जा सकता है.
* यह मनोरंजन व कसरत का भी एक अच्छा साधन है.
* बच्चों के लिए ट्रेनिंग का यह एक अच्छा साधन भी है.
* मनोवैज्ञानिक नजरिए से खुद के द्वारा उगाई गई फलसब्जियां, बाजार के मुकाबले ज्यादा स्वादिष्ठ लगती हैं.
 फसल की व्यवस्था
फसल की व्यवस्था
पोषण वाटिका में बोआई करने से पहले योजना बना लेनी चाहिए, ताकि पूरे साल फल व सब्जियां मिलती रहें. इस में निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिए :
* क्यारियों की स्थिति.
* उगाई जाने वाली फसल का नाम और प्रजाति.
* बोआई का समय.
* अंत:फसल का नाम और प्रजाति.
* बोनसाई तकनीक का इस्तेमाल.
* इन के अलावा दूसरी सब्जियों को भी जरूरत के मुताबिक उगा सकते हैं.
* मेंड़ों पर मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पोदीना, प्याज, हरा साग जैसी सब्जियां लगानी चाहिए.
* बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, छप्पनकद्दू, परवल, करेला, सीताफल आदि को बाड़ के रूप में किनारों पर ही लगानी चाहिए.
* वाटिका में फल वाले पौधों जैसे पपीता, अनार, नीबू, करौंदा, केला, अंगूर, अमरूद आदि के पौधों को सघन विधि से इस तरह किनारे की तरफ लगाएं, जिस से कि सब्जियों पर छाया या पोषक तत्त्वों के लिए होड़ न हो.
* इस फसल चक्र में कुछ यूरोपियन सब्जियां भी रखी गई हैं, जो अधिक पोषणयुक्त और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं.
* पोषण वाटिका को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उस में कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं.
पोषण वाटिका में फसल चक्र अपनाने से ज्यादा फलसब्जियां
प्लाट नं. : सब्जियों व फल का नाम
प्लाट नं. 1 : आलू, लोबिया, अगेती फूलगोभी
प्लाट नं. 2 : पछेती फूलगोभी, लोबिया, लोबिया (वर्षा)
प्लाट नं. 3 : पत्तागोभी, ग्वार फ्रैंच बीन
प्लाट नं. 4 : मटर, भिंडी, टिंडा
प्लाट नं. 5 : फूलगोभी, गोठगोभी (मध्यवर्ती) मूली, प्याज
प्लाट नं. 6 : बैगन के साथ पालक, अंत: फसल के रूप में खीरा
प्लाट नं. 7 : गाजर, भिंडी, खीरा
प्लाट नं. 8 : मटर, टमाटर, अरवी
प्लाट नं. 9 : ब्रोकली, चौलाई, मूंगफली
प्लाट नं. 10 : स्प्राउट ब्रसेल्स बैंगन (लंबे वाले
प्लाट नं. 11 : लीक खीरा, प्याज
प्लाट नं. 12 : लहसुन, मिर्च, शिमला मिर्च
प्लाट नं. 13 : चाइनीज कैवेजलैट्रस-प्याज (खरीफ)
प्लाट नं. 14 : अश्वगंधा (सालभर) (शक्तिवर्धक व दर्द निवारक) अंत: फसल लहसुन
प्लाट नं. 15 : पौधशाला के लिए (सालभर)











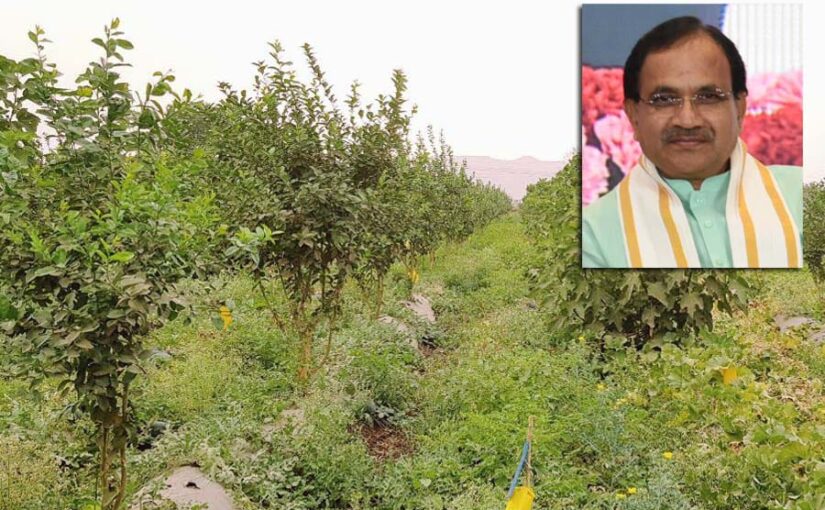

 इन बातों को अपनाने से खेती फायदेमंद, टिकाऊ होगी, मिट्टी और खेत का स्वास्थ्य ठीक होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व समुचित उपयोग होगा और खेत की मिट्टी की पानी सोखने की कूवत बढ़ेगी. फसल में कीट व बीमारियां कम लगेगीं. साथ ही, फसल पैदावार में बढ़ोतरी होगी.
इन बातों को अपनाने से खेती फायदेमंद, टिकाऊ होगी, मिट्टी और खेत का स्वास्थ्य ठीक होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व समुचित उपयोग होगा और खेत की मिट्टी की पानी सोखने की कूवत बढ़ेगी. फसल में कीट व बीमारियां कम लगेगीं. साथ ही, फसल पैदावार में बढ़ोतरी होगी.
 जहां कुछ जगहों पर ऐसे हालात हैं, वहीं कुछ जागरूक किसान विकल्प तलाशने में लगे हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि खेती में आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा रास्ता है, जो उन्हें ऐसी समस्याओं से बाहर ला कर भरपेट भोजन मुहैया करा सकता है.
जहां कुछ जगहों पर ऐसे हालात हैं, वहीं कुछ जागरूक किसान विकल्प तलाशने में लगे हैं और यह महसूस कर रहे हैं कि खेती में आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा रास्ता है, जो उन्हें ऐसी समस्याओं से बाहर ला कर भरपेट भोजन मुहैया करा सकता है.
 इस नीम के तेल और खली का उपयोग हम फसलों में रोग प्रबंधन के लिए कर सकते हैं. हमारे देश में रासायनिक जीवनाशियों की हर साल खपत 55,000 टन के आसपास है और अकेले नीम के पेड़ में ही ऐसी क्षमता है, जिस से सभी फसलों में हम सफलतापूर्वक रोग और नाशीकीट प्रबंधन कर सकते हैं.
इस नीम के तेल और खली का उपयोग हम फसलों में रोग प्रबंधन के लिए कर सकते हैं. हमारे देश में रासायनिक जीवनाशियों की हर साल खपत 55,000 टन के आसपास है और अकेले नीम के पेड़ में ही ऐसी क्षमता है, जिस से सभी फसलों में हम सफलतापूर्वक रोग और नाशीकीट प्रबंधन कर सकते हैं.



