आज वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत सस्ती, सरल व खेतों के लिए काफी उपयोगी है. गोबर की खाद के लिए जहां भरपूर गोबर उपलब्ध नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर गड्ढे खोद कर खाद बनाने में भी 6 महीने का समय लगता है. कूड़ाकरकट से बनने वाली कंपोस्ट खाद भी 4 महीने से पहले नहीं बन पाती है, जबकि वर्मी कंपोस्ट खाद 40 से 45 दिन में बन कर तैयार हो जाती है.
खेती के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल काफी खास है. फसल पैदावार की नजर से मिट्टी एक सचेत और जीवंत माध्यम है. भूमि की उत्पादकता कूवत को ध्यान में रखते हुए उस का पालनपोषण अत्यंत जरूरी माना जाता है. अगर हमें रासायनिक खेती को छोड़ कर वर्मी खाद आधारित खेती में बदलना है तो मिट्टी के उपयोग को समझना जरूरी है. जमीन हमें अनेक तरह के खाद्यान्न मुहैया करा कर हमारी मुफ्त सेवा करती है.
अत: जमीन भी हम से कुछ सेवा की अपेक्षा रखती है. खेतों में प्रति बीघा 100 या 250 मिलीलीटर की शीशी खाली करना ही भूमि की सेवा नहीं है. प्रति बीघा 2 से 3 टन जैविक खाद बना कर खेतों में डालना भूमि की सच्ची सेवा है. ऐसी ही एक जैविक खाद केंचुओं द्वारा निर्मित खाद है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जाना जाता है.
सलाह
एक अच्छे खेत के लिए साल में कम कम 2 बार 8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट का समान मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए. 2 से 3 साल के बाद जमीन की उर्वरता व संरचना देख कर वर्मी कंपोस्ट की मात्रा धीरेधीरे कुछ कम की जा सकती है.
कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से खेतों को सब से ज्यादा लाभ जैविक कार्बन से होता है. इस जैविक कार्बन को किसी भी औद्योगिक उत्पाद के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता है. अत: गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद के अलावा मिट्टी में इतनी ज्यादा मात्रा में जैविक कार्बन पहुंचाने का दूसरा कोई माध्यम नहीं है. जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी में कार्बन से पौधों को ऊर्जा मिलती है.
पौधों की जड़ों व मिट्टी में उपस्थित अनेक प्रकार के जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और न घुलने वाले फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदल कर पौधों को मुहैया कराते हैं.
लेकिन कार्बन की कमी के कारण ये जीवाणु ठीक तरह से काम नहीं कर पाते. इसलिए जैविक कार्बन कृषि योग्य मिट्टी के लिए काफी खास तत्त्व माना जाता है. मिट्टी में कार्बन की कमी से सूक्ष्मजीवी सही तरह से सक्रिय नहीं हो पाते, जिस से मिट्टी में ह्मूमस का निर्माण नहीं हो पाता और उस की जलधारण कूवत कम हो जाती है.
मिट्टी में जैविक कार्बन का कितना महत्त्व है, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं. यदि घर में 100 वाट का बल्ब लगाया जाए, लेकिन करंट 40 वाट जितना भी न हो तो 100 वाट की रोशनी हमें मिल ही नहीं सकती.
ठीक इसी तरह यदि मिट्टी में कई तरह के सूक्ष्म व पोषक तत्त्व मौजूद रहते हैं, लेकिन कार्बन यदि सही मात्रा में न हो तो पौधे इन तत्त्वों को सही तरह हासिल नहीं कर पाते और उन्हें इन पोषक व सूक्ष्म तत्त्वों की पूर्ति रासायनिक उत्पादों से करनी पड़ती है.
नतीजतन, सब से पहले तो फसल की लागत बढ़ जाती है, इस के बाद मिट्टी में मौजूद रासायनिक उत्पादों का कुछ हिस्सा ही पौधे ले पाते हैं और ज्यादा रासायनिक उत्पादों से जमीन की संरचना व उर्वरता भी बिगड़ जाती है. मिट्टी में पौधों की संतुलित बढ़ोतरी के लिए 16 तरह के पोषक तत्त्व जरूरी बताए गए हैं, जिन में सब से पहला स्थान जैविक कार्बन का ही है. देश में मिट्टी को सोना बनाने की जो बात कही जाती है वह मुख्य रूप से मिट्टी में जैविक कार्बन की उपस्थिति पर ही निर्भर करती है.
जमीन को भी खुराक की जरूरत होती है. उसे भूखा रख कर हम कब तक अन्न हासिल कर सकेंगे. रासायनिक उर्वरक जमीन का भोजन नहीं है, कार्बनिक पदार्थों व 16 तरह के पोषक तत्त्वों से युक्त गोबर या कंपोस्ट खाद ही जमीन का भोजन है.
रासायनिक उर्वरक जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं. गोबर या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किए बिना जमीन में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना हानिकारक होता है. अलगअलग फसलों में विभिन्न तरह की बीमारियों व कीटों के लिए कई तरह के रासायनिक उत्पाद बाजार में बिकते हैं. खड़ी फसल बचाने के लिए रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल कोई बुराई नहीं है, लेकिन रासायनिक उत्पादों के साथसाथ जैविक उत्पादों को भी ज्यादा से ज्यादा अहमियत देनी चाहिए.
देश में इतने सालों तक केवल रासायनिक खेती करने के बाद भी यदि हम जमीन से अनाज हासिल करते हैं तो इस का श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है, जिन्होंने युगों तक इस जमीन में जैविक खेती की वरना अमेरिका जैसा राष्ट्र केवल कुछ समय तक रासायनिक खेती कर के अपनी 12 करोड़ एकड़ कृषि लायक जमीन गंवा चुका है और अब अपने कृषि कार्यक्रम में रासायनिक उत्पादों के साथसाथ जैविक उत्पादों को भी काफी महत्त्व दे रहा है. वहीं दूसरी ओर जैविक खेती का जनक भारत केवल रासायनिक खेती के कुचक्र में दिनोदिन फंसता जा रहा है. यदि यही हालात रहे तो आने वाली पीढि़यों को कृषि योग्य जमीन के नाम पर रासायनिक झील व दलदल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा.
वर्तमान हालात में किसानों का रासायनिक उत्पादों का उपयोग किए बिना अधिकतम उपज लेना आसान नहीं है, लेकिन किसानों को कंपोस्ट खाद व अन्य जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.
अपने कृषि कार्यक्रम में जैविक खेती अपनाने पर किसानों का आर्थिक पहलू किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्यप्रद जैविक खाद्य सामग्री हमेशा दोगुने दामों पर बिकती है और जमीन, जल व हवा भी प्रदूषणमुक्त रहते हैं.
देश में करोड़ों रुपए का शुद्ध पानी मिनरल वाटर की बोतलों में बिक सकता है, तो जैविक खेती से उत्पन्न स्वास्थ्यप्रद खाद्य सामग्री भी ऊंचे दामों पर आसानी से बाजार में बिक सकती है.
पौधों के पोषण के लिए किसानों ने खुद पहल की और गोबर व गौमूत्र आधारित खादें तैयार कर इस्तेमाल कीं, जैसे अमृपानी, मटा खाद, हरी पत्तियों की तरल खाद, बायोगैस संयंत्र की स्लेरी खाद, सींग खाद आदि तरल और त्वरित खाद ने भी कमाल का काम कर दिखाया. प्रयोगशील किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व कुछ कर्मठ देशप्रेमी वैज्ञानिकों ने इस जैविक खेती पद्धति को कृषि विज्ञान में बदलना शुरू किया और खुद इस्तेमाल कर अनुकूल परिणाम हासिल कर दिखाया कि यह एक चिरस्थायी पद्धति है.
गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, फल, सब्जी, चरीचारा, सभी फसलें जैविक पद्धति से उपजा कर दिखा दिया कि बिना बाजारू कृषि उत्पादों के भी अच्छी खेती की जा सकती है.
खेती में कीट और बीमारी भी कभीकभी आती है, लेकिन जैविक कृषि पद्धति अपनाएंगे तो यह भी कम हो जाती है. गोमूत्र, पुरानी छाछ, हींग, मिर्च, लहसुन का मिश्रण, नीम का तेल, नीम, करंज, शरीफा, आईपोमिया, गाजर घास आदि पानी में घोल कर 15-20 दिन के अंतर से छिड़काव करने से कीट और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है.













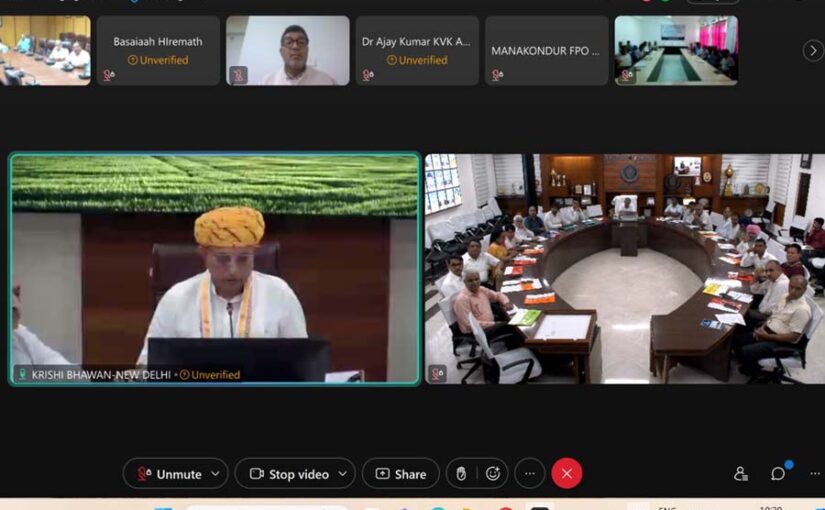





 कृषि में महिलाओं की खास भूमिका
कृषि में महिलाओं की खास भूमिका डा. आरसी अग्रवाल ने बताया कि पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है. पशु आनुवांशिक संसाधन राष्ट्र की पारंपरिक शक्ति है. आज 221 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ हम विश्व पटल पर प्रथम पायदान पर है. दुग्ध उत्पादन में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाले राज्य का गौरव पाया है.
डा. आरसी अग्रवाल ने बताया कि पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है. पशु आनुवांशिक संसाधन राष्ट्र की पारंपरिक शक्ति है. आज 221 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ हम विश्व पटल पर प्रथम पायदान पर है. दुग्ध उत्पादन में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाले राज्य का गौरव पाया है. कुलपति अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि विगत एक वर्ष में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं. विराट परिसर, श्रेष्ठ अकादमिक स्तर व शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण आज विश्वविद्यालय की भूमिका अद्वितीय है.
कुलपति अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि विगत एक वर्ष में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं. विराट परिसर, श्रेष्ठ अकादमिक स्तर व शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण आज विश्वविद्यालय की भूमिका अद्वितीय है. मिलेट्स वर्ष में भी पहचान बनाई
मिलेट्स वर्ष में भी पहचान बनाई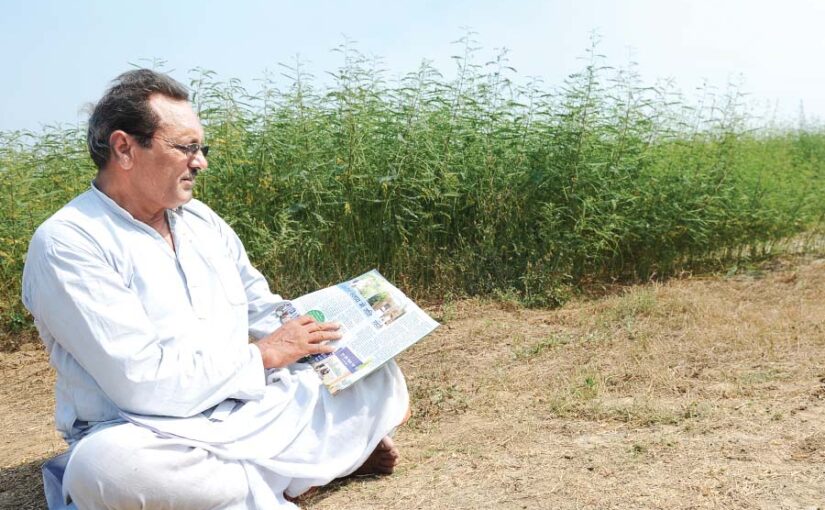
 देश में सब से पहले हिंदी का नाम आता है और कृषि से जुड़े साहित्य भी हिंदी में लगातार तैयार हो रहे हैं. भारतीय किसान संघ परिषद के ज्यादातर संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री और संबंधित फसल से जुड़ी अनुसंधान संबंधी उपलब्धियां हिंदी में ही मौजूद हैं. इसे और भी बढ़ावा देने की जरूरत है. हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रस्तुतीकरण और भी सुगम भाषा में हो.
देश में सब से पहले हिंदी का नाम आता है और कृषि से जुड़े साहित्य भी हिंदी में लगातार तैयार हो रहे हैं. भारतीय किसान संघ परिषद के ज्यादातर संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री और संबंधित फसल से जुड़ी अनुसंधान संबंधी उपलब्धियां हिंदी में ही मौजूद हैं. इसे और भी बढ़ावा देने की जरूरत है. हमेशा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रस्तुतीकरण और भी सुगम भाषा में हो.
 यदि आंकड़ों पर जाएं तो साल 2014 में जब राजग सरकार सत्ता में आई उस ने मांस निर्यात और बूचड़खानों के लिए अपने पहले ही बजट में 15 करोड़ की सब्सिडी दी और टैक्स में छूट का विधिवत प्रावधान किया. इस से समझा जा सकता है कि भाजपा की नीतियां मांस निर्यात के मामले में जैसी कांग्रेस की थीं, वैसी ही हैं.
यदि आंकड़ों पर जाएं तो साल 2014 में जब राजग सरकार सत्ता में आई उस ने मांस निर्यात और बूचड़खानों के लिए अपने पहले ही बजट में 15 करोड़ की सब्सिडी दी और टैक्स में छूट का विधिवत प्रावधान किया. इस से समझा जा सकता है कि भाजपा की नीतियां मांस निर्यात के मामले में जैसी कांग्रेस की थीं, वैसी ही हैं. गौर करने वाली बात यह है कि बिना किसी सरकारी मदद के देश में दूध का 70 फीसदी कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है. देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं. 14 राज्यों में अपनी दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं. लेकिन मांस निर्यात की वजह से पशुधन के खात्मे का असर घटते दूध उत्पादन पर साफ दिखाई पड़ रहा है. इस असंगठित क्षेत्र (दूध उत्पादन) में 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिस में अशिक्षित कारोबारी ज्यादा हैं.
गौर करने वाली बात यह है कि बिना किसी सरकारी मदद के देश में दूध का 70 फीसदी कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है. देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं. 14 राज्यों में अपनी दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं. लेकिन मांस निर्यात की वजह से पशुधन के खात्मे का असर घटते दूध उत्पादन पर साफ दिखाई पड़ रहा है. इस असंगठित क्षेत्र (दूध उत्पादन) में 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिस में अशिक्षित कारोबारी ज्यादा हैं. यदि महज भेड़ों को ही बूचड़खानों में भेजने की जगह उन का परंपरागत इस्तेमाल (जब तक वे जीवित रहें) किया जाए, तो 600 करोड़़ रुपए का दूध मिलेगा, 450 करोड़ रुपए की खाद, 50 करोड़ रुपए की ऊन प्राप्त होगी. इसी तरह गाय के वध को रोक देने से सालभर में जो लाभ होगा, वह हैरानी में डालने वाला है.
यदि महज भेड़ों को ही बूचड़खानों में भेजने की जगह उन का परंपरागत इस्तेमाल (जब तक वे जीवित रहें) किया जाए, तो 600 करोड़़ रुपए का दूध मिलेगा, 450 करोड़ रुपए की खाद, 50 करोड़ रुपए की ऊन प्राप्त होगी. इसी तरह गाय के वध को रोक देने से सालभर में जो लाभ होगा, वह हैरानी में डालने वाला है.