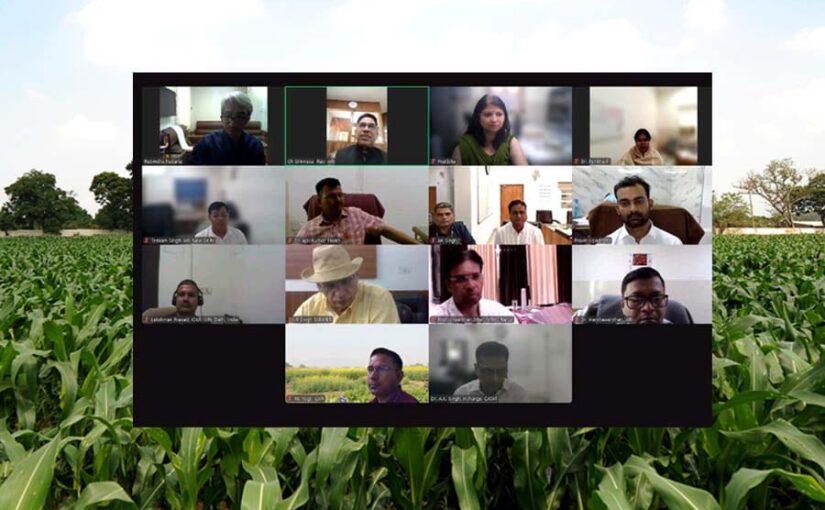Animal Health : भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अनु.प.)-केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा 05 जून, 2025 को टोंक जिले की मालपुरा तहसील के गरजेड़ा, पिपल्या एवं चांदसेन गांवों में किसान संगोष्ठी एवं पशु स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन किया गया.
जिन में कुल 364 किसानों में से 241 पुरूष एवं 123 महिला किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और वैज्ञानिकों से सीधी बातचीत की. इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डा. अरुण कुमार तोमर, अभियान के नोडल अधिकारी डा. एलआर गुर्जर सहित संस्थान के वैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों पर किसानों का मार्गदर्शन किया.
इन शिविरों में प्राकृतिक खेती के साथ जीवामृत बना कर भूमि को कैसे सुधार सकते हैं, जैविक कीटनाशक, मृदा स्वास्थ्य, बीजोपचार, जल प्रबंधन व सुक्ष्म सिंचाई, डिजिटल कृषि, पशुओं में होने वाली प्रजनन समस्याएं, पशु आहार और सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई. साथ ही, बीमार पशुओं की जांच व उपचार भी किया गया.
इस कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कई अहम समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया. जिन में प्रमुख रूप से शामिल हैं टोंक जिले में घटती दलहनी फसलें, ऊसर भूमि एवं खारे पानी की समस्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल की खरीद में देरी, नकली एवं महंगे उर्वरक, प्रमाणित बीजों की कमी, पशु चिकित्सा सेवाओं का अभाव, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजे की अनुचित कटौती, मुआवजा प्राप्ति की समय सीमा तय किए जाने की आवश्यकता समेत किसानों ने सरकार से इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की. इसी कड़ी में ग्राम गरजेड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिस में संस्थान के वैज्ञानिकों ने ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उन की समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए आगे की रणनीति पर विचारविमर्श किया.
इस अभियान के अंतर्गत नागौर जिले की मेड़ता सिटी तहसील के ग्राम मोकलपुर में 5 जून, 2025 को किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग राजस्थान सरकार, कन्हैया लाल चौधरी, किसान आयोग अध्यक्ष, सीआर चौधरी, समन्वयक विकसित कृषि संकल्प अभियान, राजस्थान, डा. अरुण कुमार तोमर, स्थानीय विधायक, जिला प्रमुख एवं उपजिला प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया. साथ ही, अभियान के अंतर्गत डूंगरपुर एवं दौसा जिलों में भी कृषि विज्ञान केंद्र की टीमों के साथ मिल कर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर द्वारा डूंगरपुर जिले के 6 गांव (आंतरी, पाड़ला मोरु, डोजा, गोड़ा फला, आरा व सूखा पादर) से कुल 949 प्रतिभागी शामिल हुए. दौसा जिले के 3 गांव (ठिकरिया, हापावास व थूमड़ी) से 694 प्रतिभागी उपस्थित रहे. दोनों जिलों से कुल 1,550 किसान (615 महिलाएं, 935 पुरुष) व 93 अन्य मिला कर कुल 1,643 प्रतिभागियों ने भाग लिया.