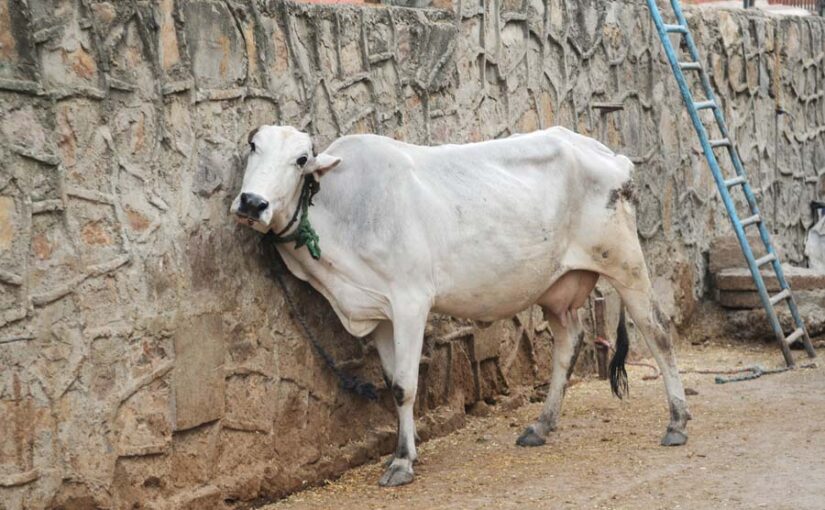भारत के जो किसान खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं, उन के लिए दुधारू पशुओं और पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या से दोचार होना पड़ता है. बारिश में तो हरा चारा खेतों की मेंड़ या खाली पड़े खेतों में आसानी से मिल जाता है, परंतु सर्दी या गरमी में पशुओं के लिए हरे चारे का इंतजाम करने में परेशानी होती है. ऐसे में किसानों को चाहिए कि खेत के कुछ हिस्से में हरे चारे की बोवनी करें, जिस से अपने पालतू पशुओं को हरा चारा सालभर मिलता रहे.
पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की बहुत कमी रहती है, जिस का दुधारू पशुओं की सेहत व दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है. इस समस्या के समाधान के लिए जायद में बहु कटाई वाली ज्वार, लोबिया, मक्का और बाजरा वगैरह फसलों को चारे के लिए बोया जाता है.
हालांकि मक्का, ज्वार जैसी फसलों से केवल 4-5 माह ही हरा चारा मिल पाता है, इसलिए किसान कम पानी में 10 से 12 महीने हरा चारा देने वाली फसलों को चुन सकते हैं.
जानकार किसान बरसीम, नेपियर घास, रिजका वगैरह लगा कर हरे चारे की व्यवस्था सालभर बनाए रख सकते हैं.
बरसीम
पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही लोकप्रिय चारा है, क्योंकि यह बहुत ही पौष्टिक व स्वादिष्ठ होता है. यह साल के पूरे शीतकालीन समय में और गरमी के शुरू तक हरा चारा मुहैया करवाती है.
पशुपालन व्यवसाय में पशुओं से बहुत ज्यादा दूध उत्पादन लेने के लिए हरे चारे का खास महत्त्व है. पशुओं के आहार पर तकरीबन 70 फीसदी खर्च होता है और हरा चारा उगा कर इस खर्च को कम कर के ज्यादा फायदा कमाया जा सकता है.
गाडरवारा तहसील के अनुविभागीय अधिकारी केएस रघुवंशी बताते हैं कि बरसीम सर्दी के मौसम में पौष्टिक चारे का एक उत्तम जरीया है. इस में रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22 फीसदी होती है. इस के चारे की पाचनशीलता 70 से 75 फीसदी होती है. इस के अलावा इस में कैल्शियम और फास्फोरस भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं. इस के चलते दुधारू पशुओं को अलग से खली, दाना वगैरह देने की जरूरत कम पड़ती है.
 नेपियर घास
नेपियर घास
किसानों के बीच नेपियर घास तेजी से लोकप्रिय हो रही है. गन्ने की तरह दिखने वाली नेपियर घास लगाने के महज 50 दिनों में विकसित हो कर अगले 4 से 5 साल तक लगातार दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत को पूरी कर सकती है.
पशुपालकों को एक बार नेपियर घास लगाने पर 4-5 साल तक हरा चारा मिल सकता है. इसे मेंड़ पर लगा कर खेत में दूसरी फसलें उगा सकते हैं. 50 दिनों में फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इस में सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है.
पशुपालन विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नेपियर घास पशुओं के लिए एक उत्तम आहार की जरूरत को पूरा करता है. दुधारू पशुओं को लगातार यह घास खिलाने से दूध उत्पादन में भी वृद्धि के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है. खेत की जुताई और समतलीकरण यानी एकसार करने के बाद नेपियर घास की जड़ों को 3-3 फुट की दूरी पर रोपा जाता है.
नेपियर घास का उत्पादन प्रति एकड़ तकरीबन 300 से 400 क्विंटल होता है. इस घास की खूबी यह है कि इसे कहीं भी लगाया जा सकता है. एक बार घास की कटाई करने के बाद उस की शाखाएं फिर से फैलने लगती हैं और 40 दिन में वह दोबारा पशुओं के खिलाने लायक हो जाता है. प्रत्येक कटाई के बाद घास की जड़ों के आसपास गोबर की सड़ी खाद या हलका यूरिया का छिड़काव करने से इस में तेजी से बढ़ोतरी होती है.
रिजका
यह किस्म चारे की एक अहम दलहनी फसल है, जो जून माह तक हरा चारा देती है. इसे बरसीम की अपेक्षा सिंचाई की जरूरत कम होती है. रिजका को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 30 सैंटीमीटर के अंतर से लाइनों में बोआई करनी चाहिए.
अक्तूबर से नवंबर माह के मध्य का समय बोआई के लिए सब से अच्छा माना जाता है.
रिजका अगर पहली बार बोया गया है, तो रिजका कल्चर का प्रयोग करना चाहिए. यदि कल्चर उपलब्ध न हो तो जिस खेत में पहले रिजका बोया गया है, उस में से
ऊपरी परत से 30 से 40 किलोग्राम मिट्टी निकाल कर जिस में रिजका बोना है, उस में मिला देना चाहिए.
कम पानी में भी होगी जवाहर विसिया 1
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने हरे चारे की एक नई किस्म खोजी है. कम पानी में उगने वाली हरे चारे की इस नई प्रजाति को जवाहर विसिया 1 नाम दिया गया है.
यह एक कटाई वाली दलहनी फसल है, जो 90 से 95 दिनों में चारे के लिए तैयार हो जाती है. एक हेक्टेयर जमीन में 240 से 260 क्विंटल हरे चारे के साथ 50 से 55 क्विंटल सूखे चारे का उत्पादन इस से होगा. इस चारे में 15 फीसदी तक प्रोटीन रहने के चलते यह पशुओं के लिए पौष्टिक है. दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने में यह चारा उपयोगी होगा.
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के वाइस चांसलर डाक्टर पीके विसेन ने बताया कि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों डाक्टर एके मेहता, डाक्टर एसबी दास, डाक्टर एसके बिलैया, डाक्टर पुष्पेंद्र यादव और डाक्टर अमित ?ा के सम्मिलित प्रयासों से एक लंबे अनुसंधान के बाद यह किस्म विकसित की गई है. कम पानी वाले या सूखाग्रस्त इलाकों के लिए चारे की यह किस्म वरदान साबित होगी.
अखिल भारतीय चारा अनुसंधान परियोजना की ओर से इंफाल, मणिपुर में आयोजित नैशनल सैमिनार में हरे चारे की इस किस्म को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के लिए अनुमोदित किया गया है.